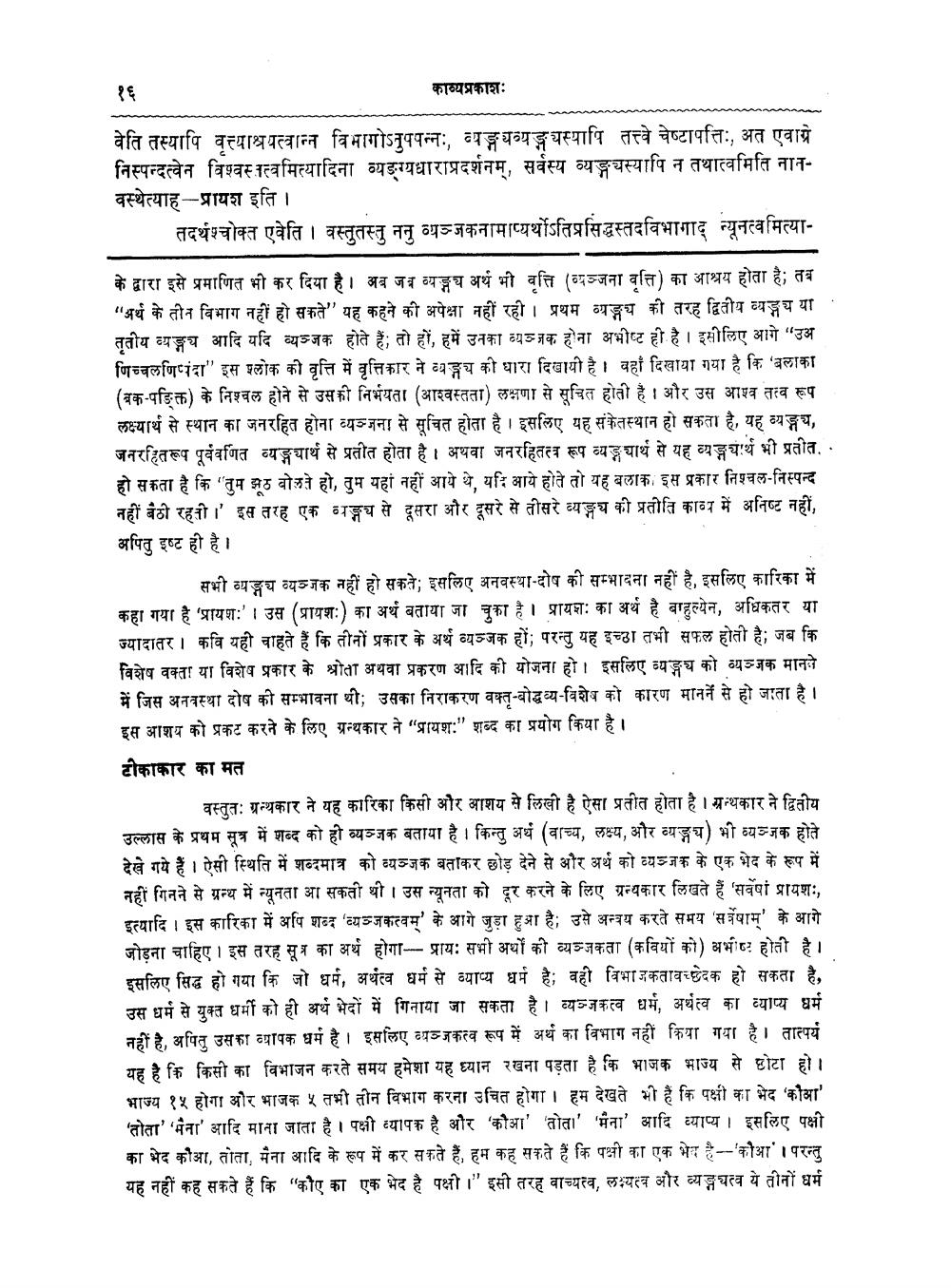________________
काव्यप्रकाशः
वेति तस्यापि वृत्त्याश्रयत्वान्न विभागोऽनुपपन्नः, व्यङ्गयव्यङ्गयस्यापि तत्त्वे चेष्टापत्तिः, अत एवाग्रे निस्पन्दत्वेन विश्वस्तत्त्वमित्यादिना व्यङ्ग्यधाराप्रदर्शनम्, सर्वस्य व्यङ्गयस्यापि न तथात्वमिति नानवस्थेत्याह–प्रायश इति ।
तदर्थश्चोक्त एवेति । वस्तुतस्तु ननु व्यञ्जकनामाप्यर्थोऽतिप्रसिद्धस्तदविभागाद् न्यूनत्वमित्या
के द्वारा इसे प्रमाणित भी कर दिया है। अब जब व्यङ्गय अर्थ भी वृत्ति (व्यञ्जना वत्ति) का आश्रय होता है; तब "अर्थ के तीन विभाग नहीं हो सकते" यह कहने की अपेक्षा नहीं रही। प्रथम व्यङ्गय की तरह द्वितीय व्यङ्गय या । तृतीय व्यङ्गय आदि यदि व्यञ्जक होते हैं, तो हों, हमें उनका व्यजक होना अभीष्ट ही है। इसीलिए आगे "उअ णिच्चलणिपंदा" इस श्लोक की वृत्ति में वृत्तिकार ने व्यङ्गय की धारा दिखायी है। वहाँ दिखाया गया है कि 'बलाका (बक-पङ्क्ति) के निश्चल होने से उसकी निर्भयता (आश्वस्तता) लक्षणा से सूचित होती है । और उस आश्व तत्व रूप लक्ष्यार्थ से स्थान का जनरहित होना व्यञ्जना से सुचित होता है। इसलिए यह संकेतस्थान हो सकता है, यह व्यङ्गय, जनरहितरूप पूर्ववणित व्यङ्गयार्थ से प्रतीत होता है। अथवा जनरहितत्व रूप व्यङ्ग चार्थ से यह व्यङ्गयार्थ भी प्रतीत, . हो सकता है कि "तुम झूठ बोलते हो, तुम यहां नहीं आये थे, यदि आये होते तो यह बलाक इस प्रकार निश्चल-निस्पन्द नहीं बैठी रहती।' इस तरह एक अङ्गय से दूसरा और दूसरे से तीसरे व्यङ्गय की प्रतीति काव्य में अनिष्ट नहीं, अपितु इष्ट ही है।
सभी व्यङ्गय व्यञ्जक नहीं हो सकते; इसलिए अनवस्था-दोष की सम्भावना नहीं है, इसलिए कारिका में कहा गया है 'प्रायशः' । उस (प्रायशः) का अर्थ बताया जा चुका है। प्रायशः का अर्थ है बाहुल्येन, अधिकतर या ज्यादातर । कवि यही चाहते हैं कि तीनों प्रकार के अर्थ व्यञ्जक हों; परन्तु यह इच्छा तभी सफल होती है; जब कि विशेष वक्ता या विशेष प्रकार के श्रोता अथवा प्रकरण आदि की योजना हो। इसलिए व्यङ्गय को व्यञ्जक मानने में जिस अनवस्था दोष की सम्भावना थी; उसका निराकरण वक्त-बोद्धव्य-विशेष को कारण मानने से हो जाता है। इस आशय को प्रकट करने के लिए ग्रन्थकार ने "प्रायशः" शब्द का प्रयोग किया है। टीकाकार का मत
वस्तुतः ग्रन्थकार ने यह कारिका किसी और आशय से लिखी है ऐसा प्रतीत होता है । ग्रन्थकार ने द्वितीय उल्लास के प्रथम सूत्र में शब्द को ही व्यञ्जक बताया है। किन्तु अर्थ (वाच्य, लक्ष्य, और व्यङ्गय) भी व्यजक होते देखे गये हैं। ऐसी स्थिति में शब्दमात्र को व्यञ्जक बताकर छोड़ देने से और अर्थ को व्यञ्जक के एक भेद के रूप में नहीं गिनने से ग्रन्थ में न्यूनता आ सकती थी। उस न्यूनता को दूर करने के लिए ग्रन्यकार लिखते हैं 'सर्वेषां प्रायशः, इत्यादि । इस कारिका में अपि शब्द 'व्यजकत्वम्' के आगे जुड़ा हुआ है; उसे अन्वय करते समय 'सर्वेषाम' के आगे जोड़ना चाहिए। इस तरह सूत्र का अर्थ होगा-प्रायः सभी अर्थों की व्यञ्जकता (कवियों को) अभीष्ट होती है। इसलिए सिद्ध हो गया कि जो धर्म, अर्थत्व धर्म से व्याप्य धर्म है; वही विभाजकतावच्छेदक हो सकता है, उस धर्म से युक्त धर्मी को ही अर्थ भेदों में गिनाया जा सकता है। व्यञ्जकत्व धर्म, अर्थत्व का व्याप्य धर्म नहीं है, अपितु उसका व्यापक धर्म है। इसलिए व्यजकत्व रूप में अर्थ का विभाग नहीं किया गया है। तात्पर्य यह है कि किसी का विभाजन करते समय हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि भाजक भाज्य से छोटा हो। भाज्य १५ होगा और भाजक ५ तभी तीन विभाग करना उचित होगा। हम देखते भी हैं कि पक्षी का भेद 'कौआ 'तोता' 'मैना' आदि माना जाता है। पक्षी व्यापक है और 'कौआ' 'तोता' 'मैना' आदि व्याप्य। इसलिए पक्षी का भेद कौआ, तोता, मैना आदि के रूप में कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पक्षी का एक भेद है-'कौआ। परन्तु यह नहीं कह सकते हैं कि "कौए का एक भेद है पक्षी।" इसी तरह वाच्यत्व, लक्ष्यत्व और व्यङ्गयत्व ये तीनों धर्म