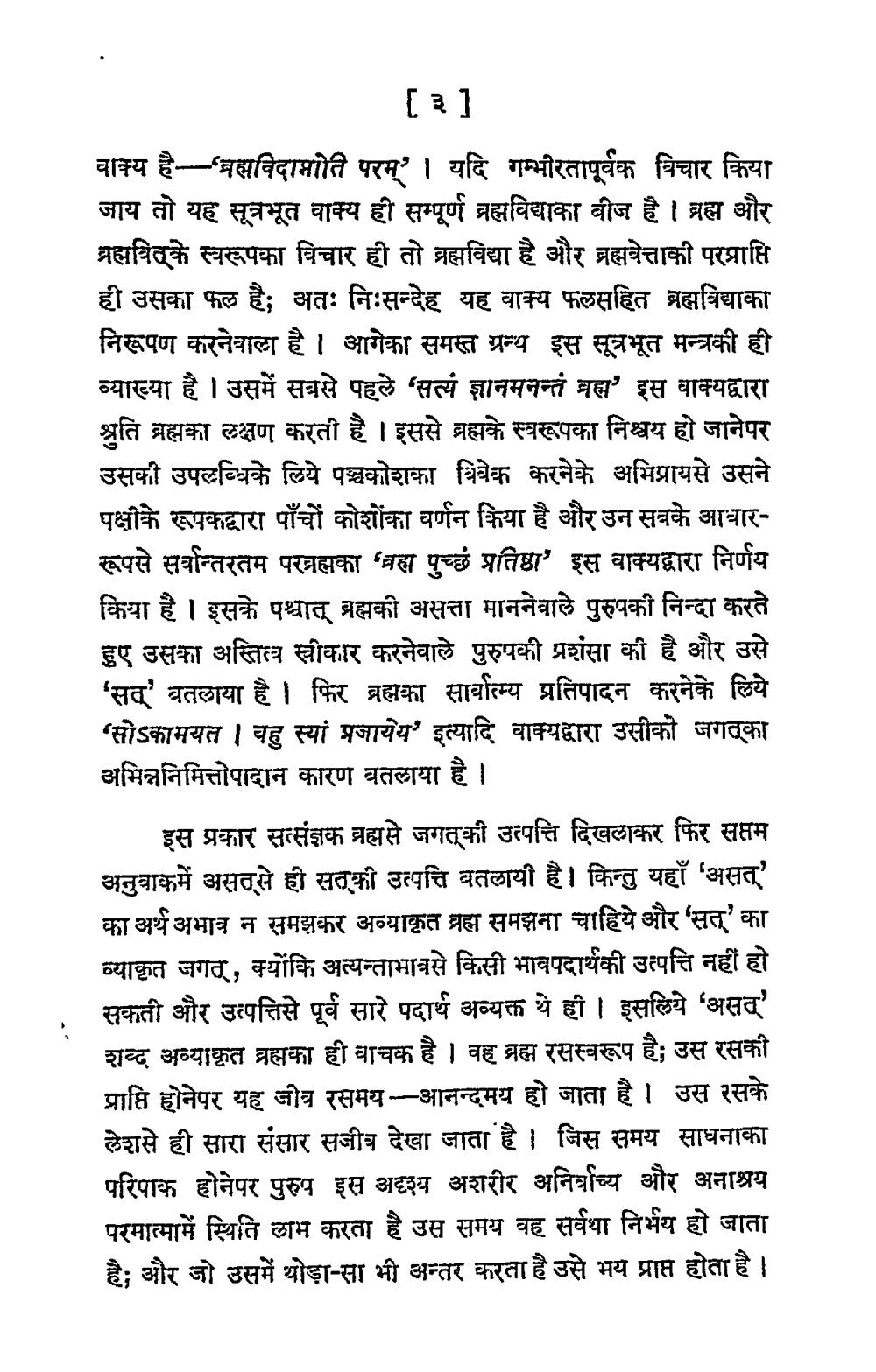________________
[३] वाक्य है-'ब्रह्मविदामाति परम्' । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका बीज है । ब्रह्म और ब्रह्मवित्के स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविद्या है और ब्रह्मवेत्ताकी परप्राप्ति ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फलसहित ब्रह्मविद्याका निरूपण करनेवाला है। आगेका समस्त ग्रन्य इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही व्याख्या है । उसमें सबसे पहले 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस वाक्यद्वारा श्रुति ब्रह्मका लक्षण करती है । इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर उसकी उपलब्धिके लिये पञ्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है और उन सबके आधाररूपसे सर्वान्तरतम परब्रह्मका 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वाक्यद्वारा निर्णय किया है । इसके पश्चात् ब्रह्मकी असत्ता माननेवाले पुरुषकी निन्दा करते हुए उसका अस्तित्व स्वीकार करनेवाले पुरुपकी प्रशंसा की है और उसे 'सत्' बतलाया है। फिर ब्रह्मका सात्म्यि प्रतिपादन करनेके लिये 'सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है ।
इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति दिखलाकर फिर सप्तम अनुवाकमें असत्से ही सत्की उत्पत्ति बतलायी है। किन्तु यहाँ 'असत्' का अर्थ अभाव न समझकर अव्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और 'सत्' का व्याकृत जगत् , क्योंकि अत्यन्ताभावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उत्पत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही । इसलिये 'असत्' शब्द अव्याकृत ब्रह्मका ही वाचक है । वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय-आनन्दमय हो जाता है । उस रसके लेशसे ही सारा संसार सजीव देखा जाता है। जिस समय साधनाका परिपाक होनेपर पुरुप इस अदृश्य अशरीर अनिर्वाच्य और अनाश्रय परमात्मामें स्थिति लाभ करता है उस समय वह सर्वथा निर्भय हो जाता है; और जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है।