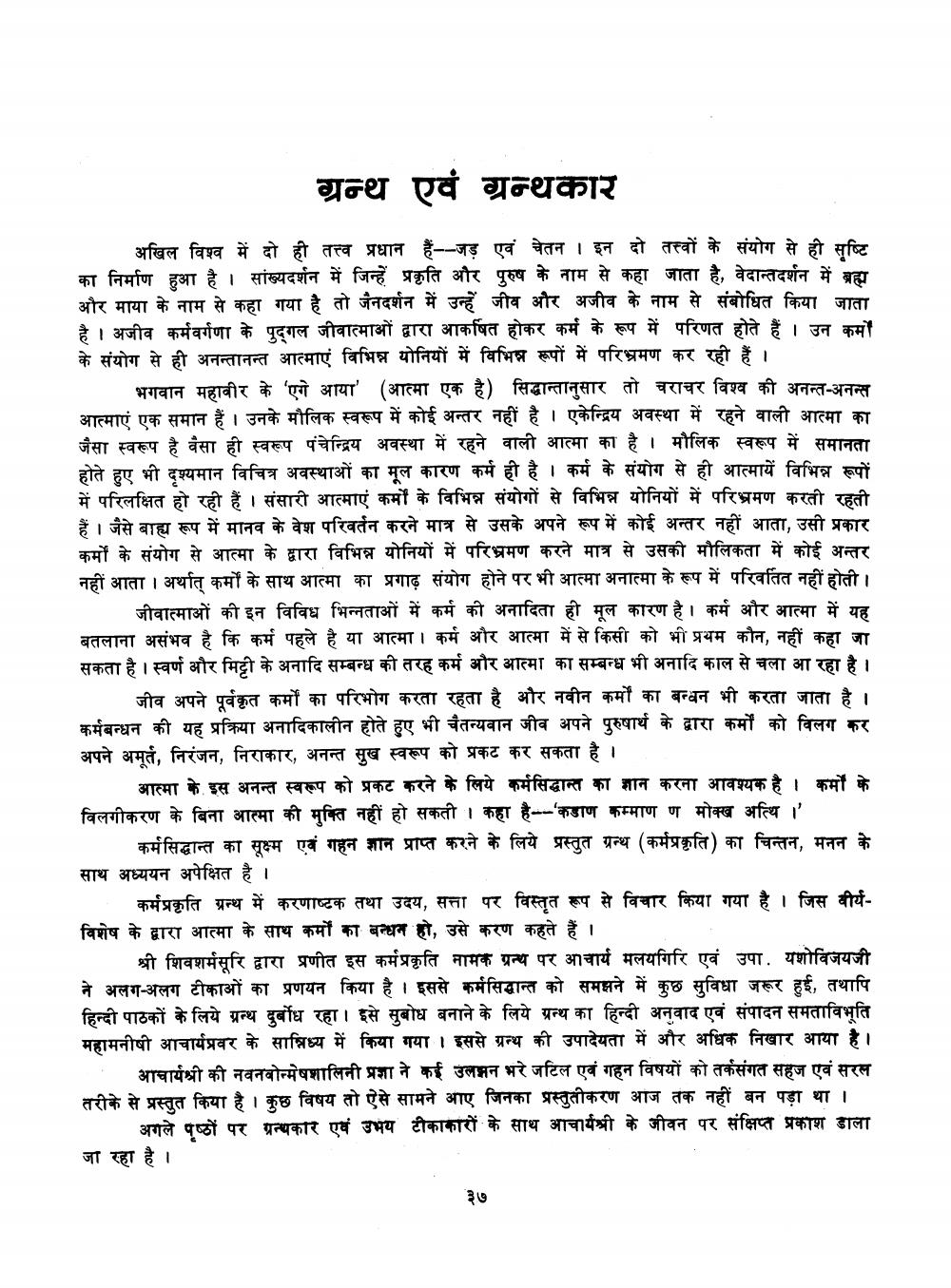________________
ग्रन्थ एवं एवं ग्रन्थकार
अखिल विश्व में दो ही तत्व प्रधान हैं--जड़ एवं चेतन इन दो तत्वों के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। सांख्यदर्शन में जिन्हें प्रकृति और पुरुष के नाम से कहा जाता है, वेदान्तदर्शन में ब्रह्म और माया के नाम से कहा गया है तो जैनदर्शन में उन्हें जीव और अजीव के नाम से संबोधित किया जाता है । अजीव कर्मवर्गणा के पुद्गल जीवात्माओं द्वारा आकर्षित होकर कर्म के रूप में परिणत होते हैं । उन कर्मों के संयोग से ही अनन्तानन्त आत्माएं विभिन्न योनियों में विभिन्न रूपों में परिभ्रमण कर रही हैं।
भगवान महावीर के 'एगे आया' (आत्मा एक है) सिद्धान्तानुसार तो चराचर विश्व की अनन्त - अनन्त आत्माएं एक समान हैं। उनके मौलिक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है । एकेन्द्रिय अवस्था में रहने वाली आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप पंचेन्द्रिय अवस्था में रहने वाली आत्मा का है। मौलिक स्वरूप में समानता होते हुए भी दृश्यमान विचित्र अवस्थाओं का मूल कारण कर्म ही है। कर्म के संयोग से ही आत्मायें विभिन्न रूपों में परिलक्षित हो रही हैं । संसारी आत्माएं कर्मों के विभिन्न संयोगों से विभिन्न योनियों में परिभ्रमण करती रहती हैं। जैसे बाह्य रूप में मानव के वेश परिवर्तन करने मात्र से उसके अपने रूप में कोई अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार कर्मों के संयोग से आत्मा के द्वारा विभिन्न योनियों में परिभ्रमण करने मात्र से उसकी मौलिकता में कोई अन्तर नहीं आता । अर्थात् कर्मों के साथ आत्मा का प्रगाढ़ संयोग होने पर भी आत्मा अनात्मा के रूप में परिवर्तित नहीं होती । जीवात्माओं की इन विविध भिन्नताओं में कर्म की अनादिता ही मूल कारण है। कर्म और आत्मा में यह बतलाना असंभव है कि कर्म पहले है या आत्मा । कर्म और आत्मा में से किसी को भी प्रथम कौन, नहीं कहा जा सकता है। स्वर्ण और मिट्टी के अनादि सम्बन्ध की तरह कर्म और आत्मा का सम्बन्ध भी अनादि काल से चला आ रहा है।
जीव अपने पूर्वकृत कर्मों का परिभोग करता रहता है और नवीन कर्मों का बन्धन भी करता जाता है । कर्मबन्धन की यह प्रक्रिया अनादिकालीन होते हुए भी चैतन्यवान जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों को विलग कर अपने अमूर्त, निरंजन, निराकार, अनन्त सुख स्वरूप को प्रकट कर सकता है ।
आत्मा के इस अनन्त स्वरूप को प्रकट करने के लिये कर्मसिद्धान्त का ज्ञान करना आवश्यक है । कर्मों के विलगीकरण के बिना आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। कहा है- 'कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि ।'
कर्मसिद्धान्त का सूक्ष्म एवं गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ ( कर्मप्रकृति) का चिन्तन, मनन के साथ अध्ययन अपेक्षित है ।
कर्मप्रकृति ग्रन्थ में करणाष्टक तथा उदय, सत्ता पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। जिस वीर्य विशेष के द्वारा आत्मा के साथ कर्मों का बन्धन हो, उसे करण कहते हैं।
श्री शिवशमंसूरि द्वारा प्रणीत इस कर्मप्रकृति नामक ग्रन्थ पर आचार्य मलयगिरि एवं उपा यशोविजयजी ने अलग-अलग टीकाओं का प्रणयन किया है। इससे कर्मसिद्धान्त को समझने में कुछ सुविधा जरूर हुई, तथापि हिन्दी पाठकों के लिये ग्रन्थ दुर्बोध रहा। इसे सुबोध बनाने के लिये ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद एवं संपादन समताविभूति महामनीषी आचार्यप्रवर के सान्निध्य में किया गया। इससे ग्रन्थ की उपादेयता में और अधिक निखार आया है।
आचार्यश्री की नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा ने कई उलझन भरे जटिल एवं गहन विषयों को तर्कसंगत सहज एवं सरल तरीके से प्रस्तुत किया है। कुछ विषय तो ऐसे सामने आए जिनका प्रस्तुतीकरण आज तक नहीं बन पड़ा था । अगले पृष्ठों पर ग्रन्थकार एवं उभय टीकाकारों के साथ आचार्यश्री के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला
जा रहा है।
३७