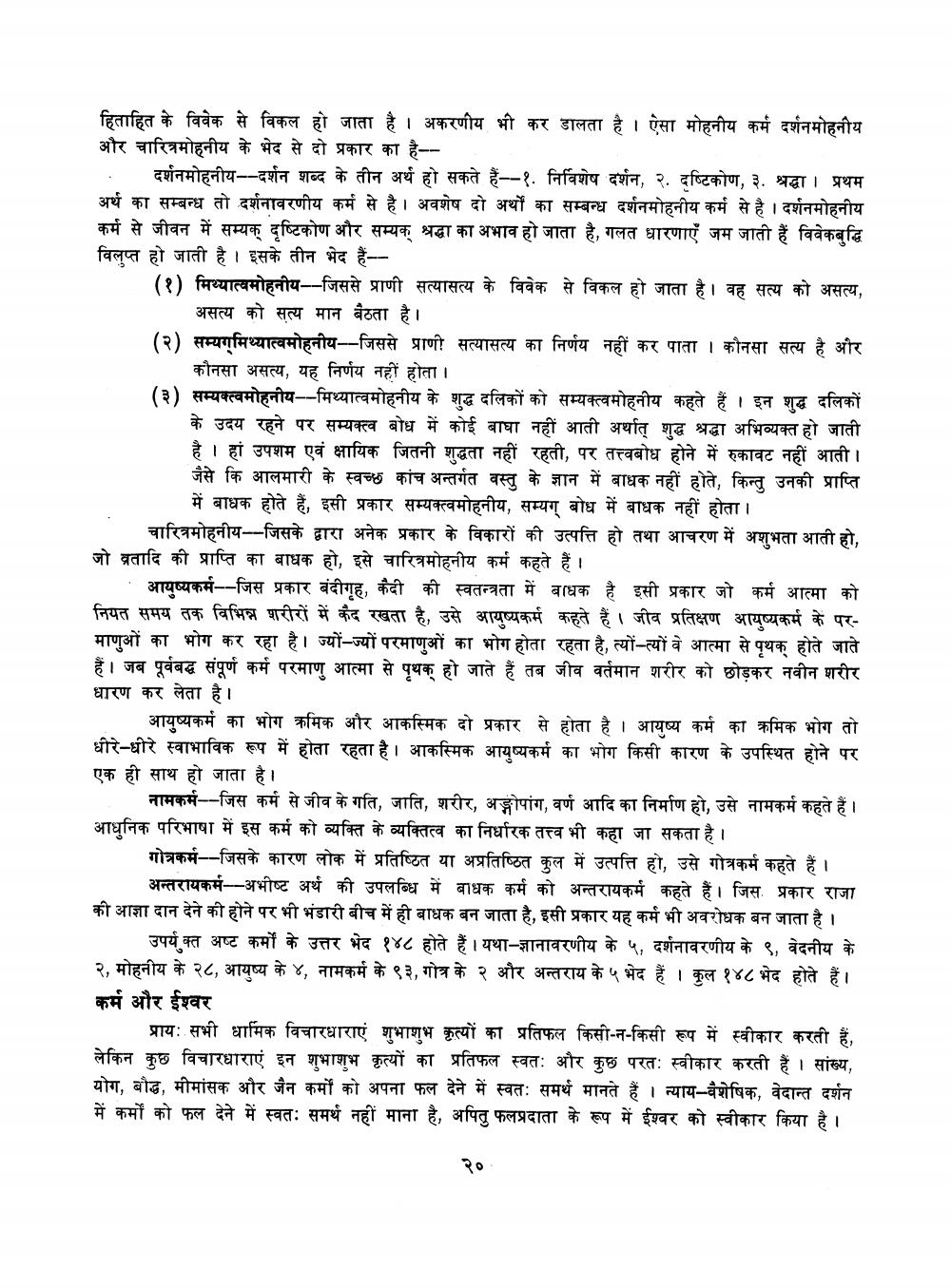________________
(३)
हिताहित के विवेक से विकल हो जाता है । अकरणीय भी कर डालता है । ऐसा मोहनीय कर्म दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के भेद से दो प्रकार का है-- . दर्शनमोहनीय-दर्शन शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं-१. निविशेष दर्शन, २. दष्टिकोण, ३. श्रद्धा। प्रथम अर्थ का सम्बन्ध तो दर्शनावरणीय कर्म से है। अवशेष दो अर्थों का सम्बन्ध दर्शनमोहनीय कर्म से है । दर्शनमोहनीय कर्म से जीवन में सम्यक दृष्टिकोण और सम्यक श्रद्धा का अभाव हो जाता है, गलत धारणाएँ जम जाती हैं विवेकबुद्धि विलुप्त हो जाती है। इसके तीन भेद हैं--
(१) मिथ्यात्वमोहनीय-जिससे प्राणी सत्यासत्य के विवेक से विकल हो जाता है। वह सत्य को असत्य,
असत्य को सत्य मान बैठता है। (२) सम्यगमिथ्यात्वमोहनीय-जिससे प्राणी सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर पाता । कौनसा सत्य है और
कौनसा असत्य, यह निर्णय नहीं होता। सम्यक्त्वमोहनीय-मिथ्यात्वमोहनीय के शुद्ध दलिकों को सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं । इन शुद्ध दलिकों के उदय रहने पर सम्यक्त्व बोध में कोई बाधा नहीं आती अर्थात् शुद्ध श्रद्धा अभिव्यक्त हो जाती है । हां उपशम एवं क्षायिक जितनी शुद्धता नहीं रहती, पर तत्त्वबोध होने में रुकावट नहीं आती। जैसे कि आलमारी के स्वच्छ कांच अन्तर्गत वस्तु के ज्ञान में बाधक नहीं होते, किन्तु उनकी प्राप्ति
में बाधक होते हैं, इसी प्रकार सम्यक्त्वमोहनीय, सम्यग् बोध में बाधक नहीं होता। चारित्रमोहनीय-जिसके द्वारा अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति हो तथा आचरण में अशुभता आती हो, जो व्रतादि की प्राप्ति का बाधक हो, इसे चारित्रमोहनीय कर्म कहते हैं।
- आयुष्यकर्म-जिस प्रकार बंदीगृह, कैदी की स्वतन्त्रता में बाधक है इसी प्रकार जो कर्म आत्मा को नियत समय तक विभिन्न शरीरों में कैद रखता है, उसे आयुष्यकर्म कहते हैं । जीव प्रतिक्षण आयुष्यकर्म के परमाणुओं का भोग कर रहा है। ज्यों-ज्यों परमाणुओं का भोग होता रहता है, त्यों-त्यों वे आत्मा से पृथक् होते जाते हैं। जब पूर्वबद्ध संपूर्ण कर्म परमाणु आत्मा से पृथक् हो जाते हैं तब जीव वर्तमान शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है।
आयुष्यकर्म का भोग क्रमिक और आकस्मिक दो प्रकार से होता है । आयुष्य कर्म का क्रमिक भोग तो धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप में होता रहता है। आकस्मिक आयष्यकर्म का भोग किसी कारण के उपस्थित होने पर एक ही साथ हो जाता है।
नामकर्म--जिस कर्म से जीव के गति, जाति, शरीर, अङ्गोपांग, वर्ण आदि का निर्माण हो, उसे नामकर्म कहते हैं। आधुनिक परिभाषा में इस कर्म को व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारक तत्त्व भी कहा जा सकता है।
गोत्रकर्म-जिसके कारण लोक में प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित कुल में उत्पत्ति हो, उसे गोत्रकर्म कहते हैं।
अन्तरायकर्म-अभीष्ट अर्थ की उपलब्धि में बाधक कर्म को अन्तरायकर्म कहते हैं। जिस प्रकार राजा की आज्ञा दान देने की होने पर भी भंडारी बीच में ही बाधक बन जाता है, इसी प्रकार यह कर्म भी अवरोधक बन जाता है।
उपर्युक्त अष्ट कर्मों के उत्तर भेद १४८ होते हैं । यथा-ज्ञानावरणीय के ५, दर्शनावरणीय के ९, वेदनीय के २, मोहनीय के २८, आयुष्य के ४, नामकर्म के ९३, गोत्र के २ और अन्तराय के ५ भेद हैं । कुल १४८ भेद होते हैं। कर्म और ईश्वर
प्रायः सभी धार्मिक विचारधाराएं शुभाशुभ कृत्यों का प्रतिफल किसी-न-किसी रूप में स्वीकार करती हैं, लेकिन कुछ विचारधाराएं इन शुभाशुभ कृत्यों का प्रतिफल स्वत: और कुछ परतः स्वीकार करती हैं। सांख्य, योग, बौद्ध, मीमांसक और जैन कर्मों को अपना फल देने में स्वतः समर्थ मानते हैं । न्याय-वैशेषिक, वेदान्त दर्शन में कर्मों को फल देने में स्वतः समर्थ नहीं माना है, अपितु फलप्रदाता के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया है।
२०