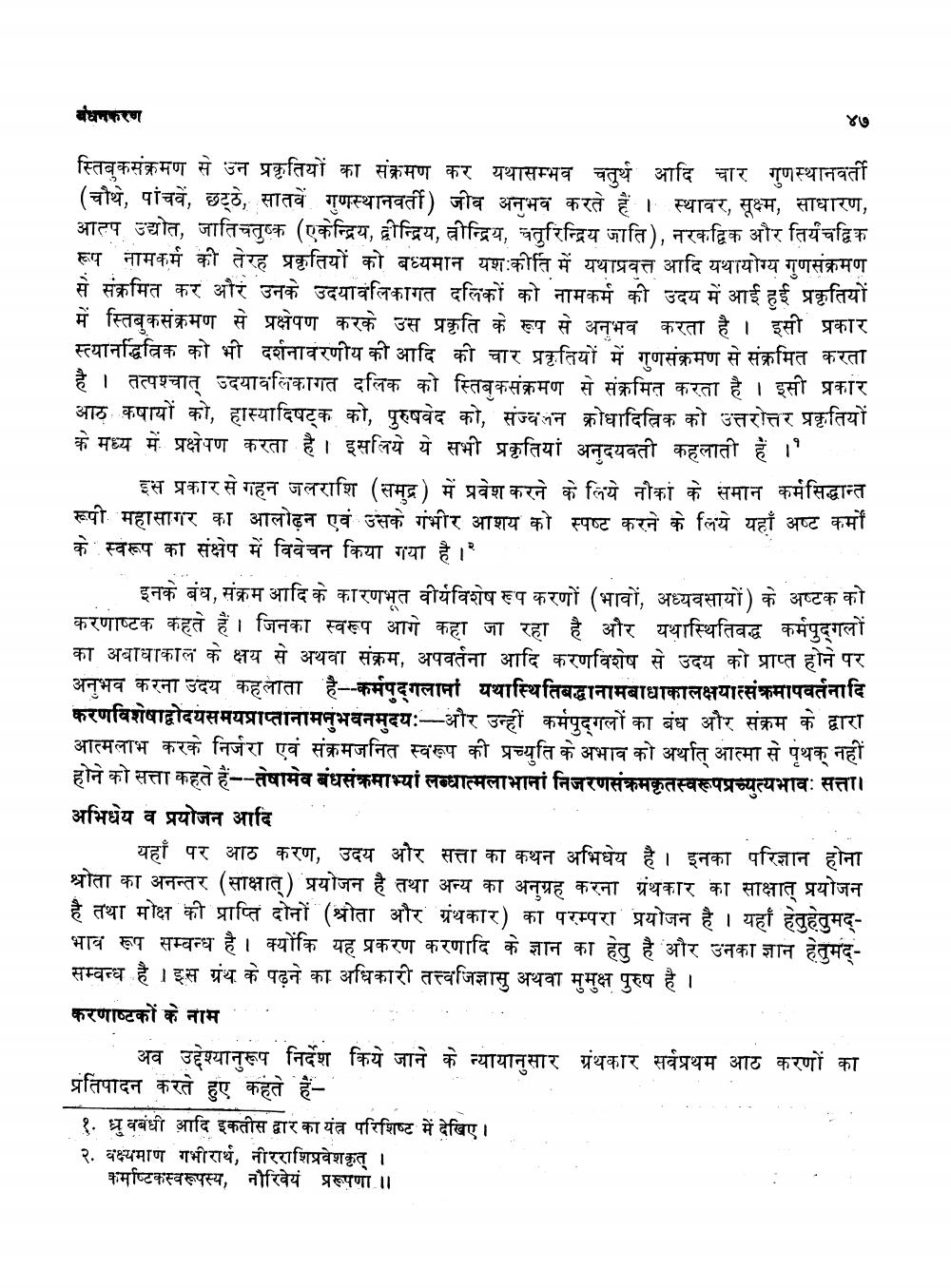________________
बंधनकरण
स्तिबुकसंक्रमण से उन प्रकृतियों का संक्रमण कर यथासम्भव चतुर्थ आदि चार गुणस्थानवर्ती (चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थानवर्ती) जीव अनुभव करते हैं । स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, आतप उद्योत, जातिचतुष्क (एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति), नरकद्विक और तिर्यंचद्विक रूप नामकर्म की तेरह प्रकृतियों को बध्यमान यशःकीति में यथाप्रवत्त आदि यथायोग्य गुणसंक्रमण से संक्रमित कर और उनके उदयावलिकागत दलिकों को नामकर्म की उदय में आई हुई प्रकृतियों में स्तिबुकसंक्रमण से प्रक्षेपण करके उस प्रकृति के रूप से अनभव करता है । इसी प्रकार स्त्यानद्धित्रिक को भी दर्शनावरणीय की आदि की चार प्रकृतियों में गुणसंक्रमण से संक्रमित करता है । तत्पश्चात् उदयावलिकागत दलिक को स्तिबकसंक्रमण से संक्रमित करता है । इसी प्रकार आठ कषायों को, हास्यादिषट्क को, पुरुषवेद को, संज्वलन क्रोधादित्रिक को उत्तरोत्तर प्रकृतियों के मध्य में प्रक्षेपण करता है। इसलिये ये सभी प्रकृतियां अनुदयक्ती कहलाती हैं ।'
इस प्रकार से गहन जलराशि (समुद्र) में प्रवेश करने के लिये नौका के समान कर्मसिद्धान्त रूपी महासागर का आलोढ़न एवं उसके गंभीर आशय को स्पष्ट करने के लिये यहाँ अष्ट कर्मों के स्वरूप का संक्षेप में विवेचन किया गया है।
इनके बंध, संक्रम आदि के कारणभूत वीर्यविशेष रूप करणों (भावों, अध्यवसायों) के अष्टक को करणाष्टक कहते हैं। जिनका स्वरूप आगे कहा जा रहा है और यथास्थितिबद्ध कर्मपुद्गलों का अबाधाकाल के क्षय से अथवा संक्रम, अपवर्तना आदि करणविशेष से उदय को प्राप्त होने पर अनुभव करना उदय कहलाता है--कर्मपद्गलानां यथास्थितिबद्धानामबाधाकालक्षयात्संक्रमापवर्तनादि करणविशेषाद्वोदयसमयप्राप्तानामनुभवनमुदयः-और उन्हीं कर्मपुद्गलों का बंध और संक्रम के द्वारा आत्मलाभ करके निर्जरा एवं संक्रमजनित स्वरूप की प्रच्युति के अभाव को अर्थात् आत्मा से पृथक् नहीं होने को सत्ता कहते हैं--तेषामेव बंधसंक्रमाभ्यां लब्धात्मलाभानां निजरणसंक्रमकृतस्वरूपप्रच्युत्यभावः सत्ता। अभिधेय व प्रयोजन आदि
___यहाँ पर आठ करण, उदय और सत्ता का कथन अभिधेय है। इनका परिज्ञान होना श्रोता का अनन्तर (साक्षात्) प्रयोजन है तथा अन्य का अनुग्रह करना ग्रंथकार का साक्षात् प्रयोजन है तथा मोक्ष की प्राप्ति दोनों (श्रोता और ग्रंथकार) का परम्परा प्रयोजन है । यहाँ हेतुहेतुमद्भाव रूप सम्बन्ध है। क्योंकि यह प्रकरण करणादि के ज्ञान का हेतु है और उनका ज्ञान हेतुमद्सम्वन्ध है । इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी तत्त्वजिज्ञासु अथवा मुमुक्ष पुरुष है । करणाष्टकों के नाम
अव उद्देश्यानुरूप निर्देश किये जाने के न्यायानुसार ग्रंथकार सर्वप्रथम आठ करणों का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं१. ध्रुवबंधी आदि इकतीस द्वार का यंत्र परिशिष्ट में देखिए। २. वक्ष्यमाण गभीरार्थ, नीरराशिप्रवेशकृत् ।
कर्माष्टकस्वरूपस्य, नौरिवेयं प्ररूपणा ।।