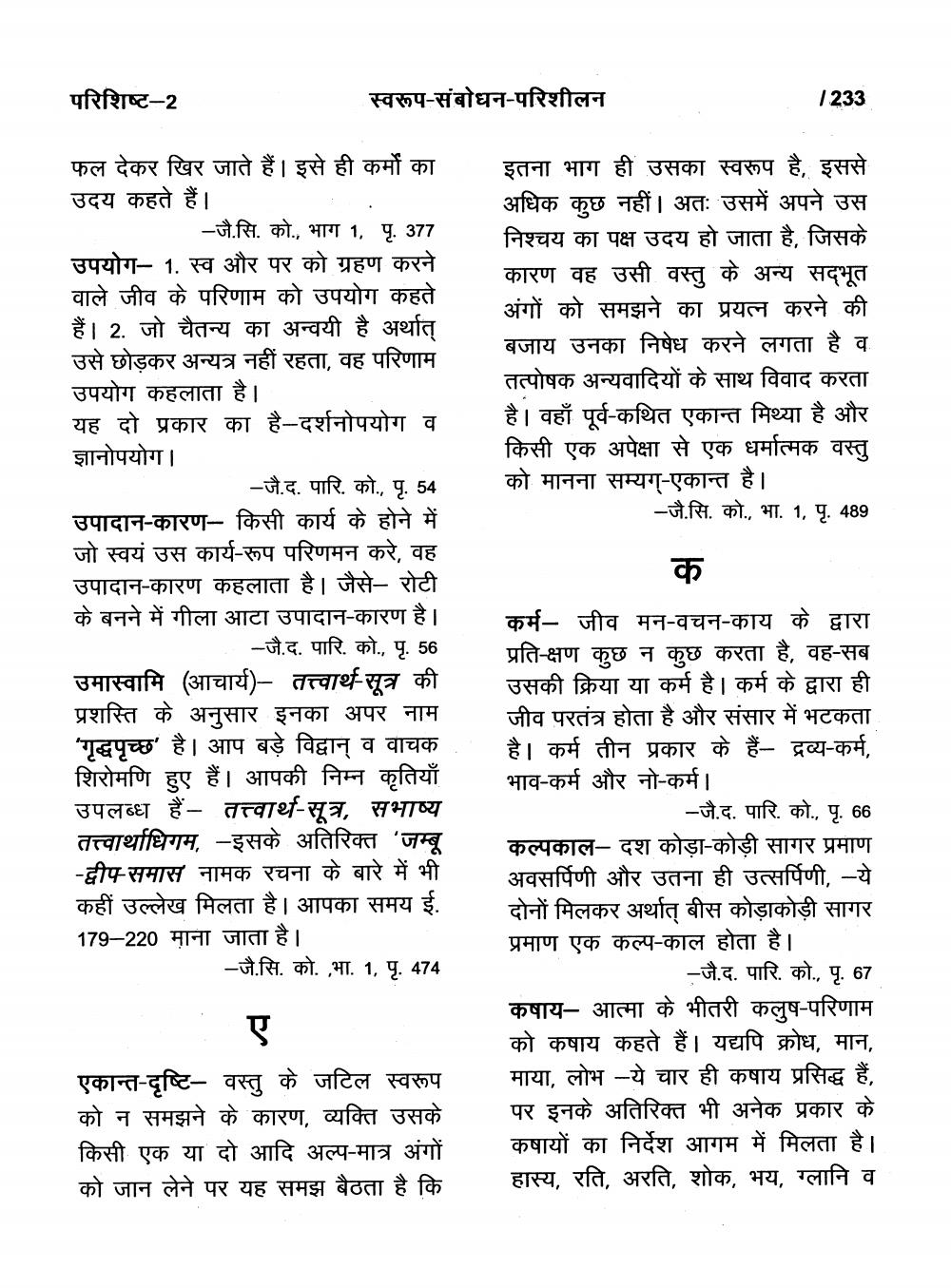________________
परिशिष्ट-2
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
1233
इतना भाग ही उसका स्वरूप है, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः उसमें अपने उस निश्चय का पक्ष उदय हो जाता है, जिसके कारण वह उसी वस्तु के अन्य सद्भूत अंगों को समझने का प्रयत्न करने की बजाय उनका निषेध करने लगता है व तत्पोषक अन्यवादियों के साथ विवाद करता है। वहाँ पूर्व-कथित एकान्त मिथ्या है और किसी एक अपेक्षा से एक धर्मात्मक वस्तु को मानना सम्यग्-एकान्त है।
-जै.सि. को., भा. 1, पृ. 489
फल देकर खिर जाते हैं। इसे ही कर्मों का उदय कहते हैं।
___-जै.सि. को., भाग 1, पृ. 377 उपयोग- 1. स्व और पर को ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। 2. जो चैतन्य का अन्वयी है अर्थात् उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, वह परिणाम उपयोग कहलाता है। यह दो प्रकार का है-दर्शनोपयोग व ज्ञानोपयोग।
___ -जै.द. पारि. को., पृ. 54 उपादान-कारण- किसी कार्य के होने में जो स्वयं उस कार्य-रूप परिणमन करे, वह उपादान-कारण कहलाता है। जैसे- रोटी के बनने में गीला आटा उपादान-कारण है।
_ -जै.द. पारि. को., पृ. 56 उमास्वामि (आचार्य)- तत्त्वार्थ-सूत्र की प्रशस्ति के अनुसार इनका अपर नाम 'गृद्धपृच्छ' है। आप बड़े विद्वान् व वाचक शिरोमणि हुए हैं। आपकी निम्न कृतियाँ उपलब्ध हैं- तत्त्वार्थ-सूत्र, सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम, -इसके अतिरिक्त 'जम्बू -द्वीप-समास नामक रचना के बारे में भी कहीं उल्लेख मिलता है। आपका समय ई. 179-220 माना जाता है।
-जै.सि. को. भा. 1, पृ. 474
कर्म- जीव मन-वचन-काय के द्वारा प्रति-क्षण कुछ न कुछ करता है, वह-सब उसकी क्रिया या कर्म है। कर्म के द्वारा ही जीव परतंत्र होता है और संसार में भटकता है। कर्म तीन प्रकार के हैं- द्रव्य-कर्म, भाव-कर्म और नो-कर्म।
-जै.द. पारि. को., पृ. 66 कल्पकाल-दश कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पिणी और उतना ही उत्सर्पिणी, –ये दोनों मिलकर अर्थात् बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण एक कल्प-काल होता है।
-जै.द. पारि. को., पृ. 67 कषाय- आत्मा के भीतरी कलुष-परिणाम को कषाय कहते हैं। यद्यपि क्रोध, मान, माया, लोभ -ये चार ही कषाय प्रसिद्ध हैं, पर इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के कषायों का निर्देश आगम में मिलता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि व
एकान्त-दृष्टि- वस्तु के जटिल स्वरूप को न समझने के कारण, व्यक्ति उसके किसी एक या दो आदि अल्प-मात्र अंगों को जान लेने पर यह समझ बैठता है कि