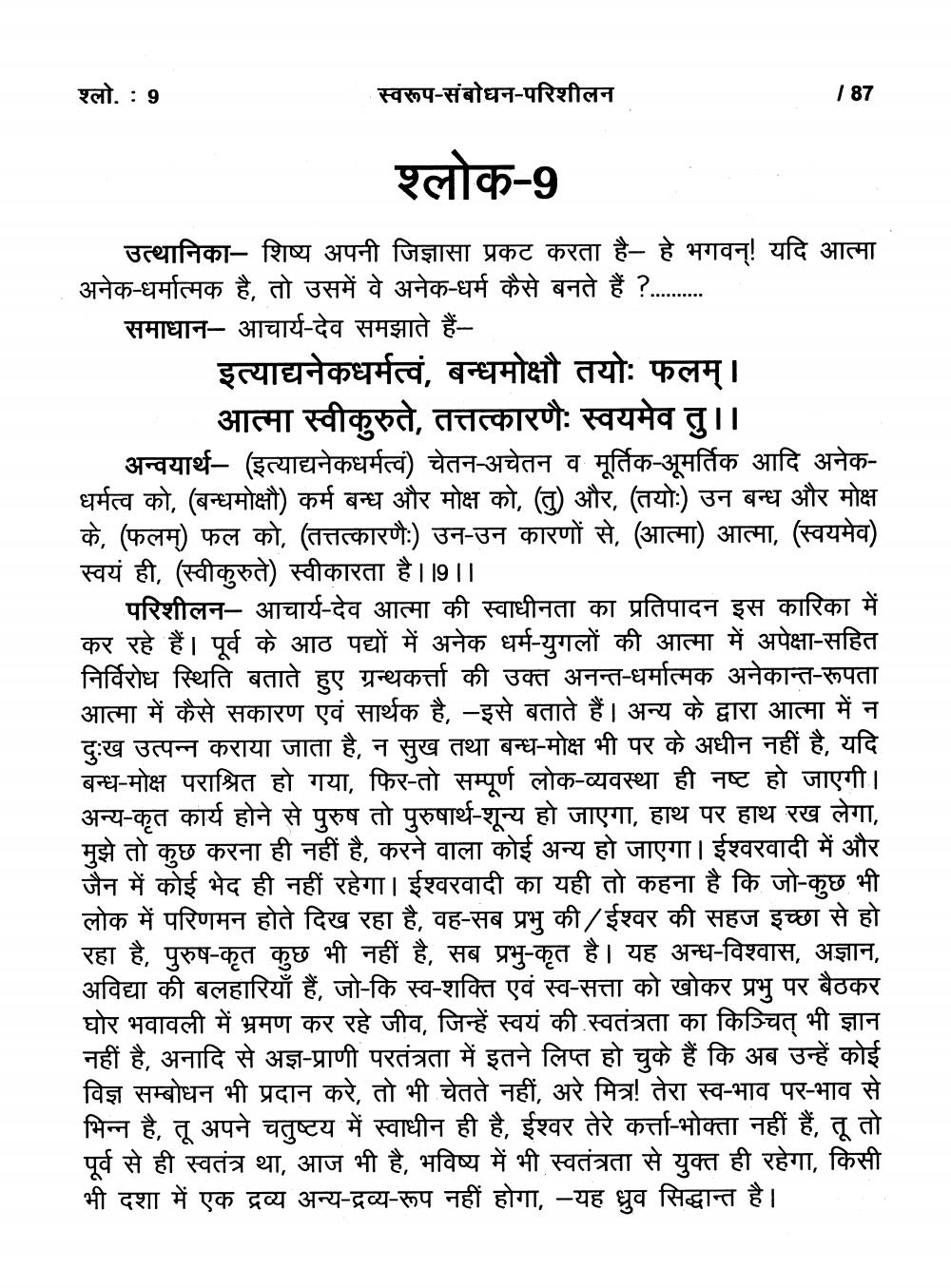________________
श्लो. : 9
स्वरूप-संबोधन-परिशीलन
/ 87
श्लोक - 9
उत्थानिका— शिष्य अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है- हे भगवन्! यदि आत्मा अनेक-धर्मात्मक है, तो उसमें वे अनेक-धर्म कैसे बनते हैं ? . समाधान- आचार्य-देव समझाते हैं
इत्याद्यनेकधर्मत्वं, बन्धमोक्षौ तयोः फलम् । आत्मा स्वीकुरुते तत्तत्कारणैः स्वयमेव तु ।।
अन्वयार्थ– (इत्याद्यनेकधर्मत्वं) चेतन-अचेतन व मूर्तिक- अमर्तिक आदि अनेकधर्मत्व को, (बन्धमोक्षौ ) कर्म बन्ध और मोक्ष को, (तु) और (तयोः) उन बन्ध और मोक्ष के, (फलम् ) फल को, (तत्तत्कारणैः) उन-उन कारणों से, (आत्मा) आत्मा, ( स्वयमेव ) स्वयं ही, (स्वीकुरुते) स्वीकारता है । ।9।।
परिशीलन- आचार्य देव आत्मा की स्वाधीनता का प्रतिपादन इस कारिका में कर रहे हैं। पूर्व के आठ पद्यों में अनेक धर्म-युगलों की आत्मा में अपेक्षा - सहित निर्विरोध स्थिति बताते हुए ग्रन्थकर्त्ता की उक्त अनन्त-धर्मात्मक अनेकान्त-रूपता आत्मा में कैसे सकारण एवं सार्थक है, - इसे बताते हैं । अन्य के द्वारा आत्मा में न दुःख उत्पन्न कराया जाता है, न सुख तथा बन्ध - मोक्ष भी पर के अधीन नहीं है, यदि बन्ध-मोक्ष पराश्रित हो गया, फिर तो सम्पूर्ण लोक-व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी । अन्य-कृत कार्य होने से पुरुष तो पुरुषार्थ - शून्य हो जाएगा, हाथ पर हाथ रख लेगा, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, करने वाला कोई अन्य हो जाएगा । ईश्वरवादी में और जैन में कोई भेद ही नहीं रहेगा। ईश्वरवादी का यही तो कहना है कि जो कुछ भी लोक में परिणमन होते दिख रहा है, वह सब प्रभु की / ईश्वर की सहज इच्छा से हो रहा है, पुरुष - कृत कुछ भी नहीं है, सब प्रभु - कृत है । यह अन्ध-विश्वास, अज्ञान, अविद्या की बलहारियाँ हैं, जो कि स्व-शक्ति एवं स्व-सत्ता को खोकर प्रभु पर बैठकर घोर भवावली में भ्रमण कर रहे जीव, जिन्हें स्वयं की स्वतंत्रता का किञ्चित् भी ज्ञान नहीं है, अनादि से अज्ञ - प्राणी परतंत्रता में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब उन्हें कोई विज्ञ सम्बोधन भी प्रदान करे, तो भी चेतते नहीं, अरे मित्र! तेरा स्व-भाव पर-भाव से भिन्न है, तू अपने चतुष्टय में स्वाधीन ही है, ईश्वर तेरे कर्त्ता - भोक्ता नहीं हैं, तू तो पूर्व से ही स्वतंत्र था, आज भी है, भविष्य में भी स्वतंत्रता से युक्त ही रहेगा, किसी भी दशा में एक द्रव्य अन्य- द्रव्य रूप नहीं होगा, - यह ध्रुव सिद्धान्त है ।