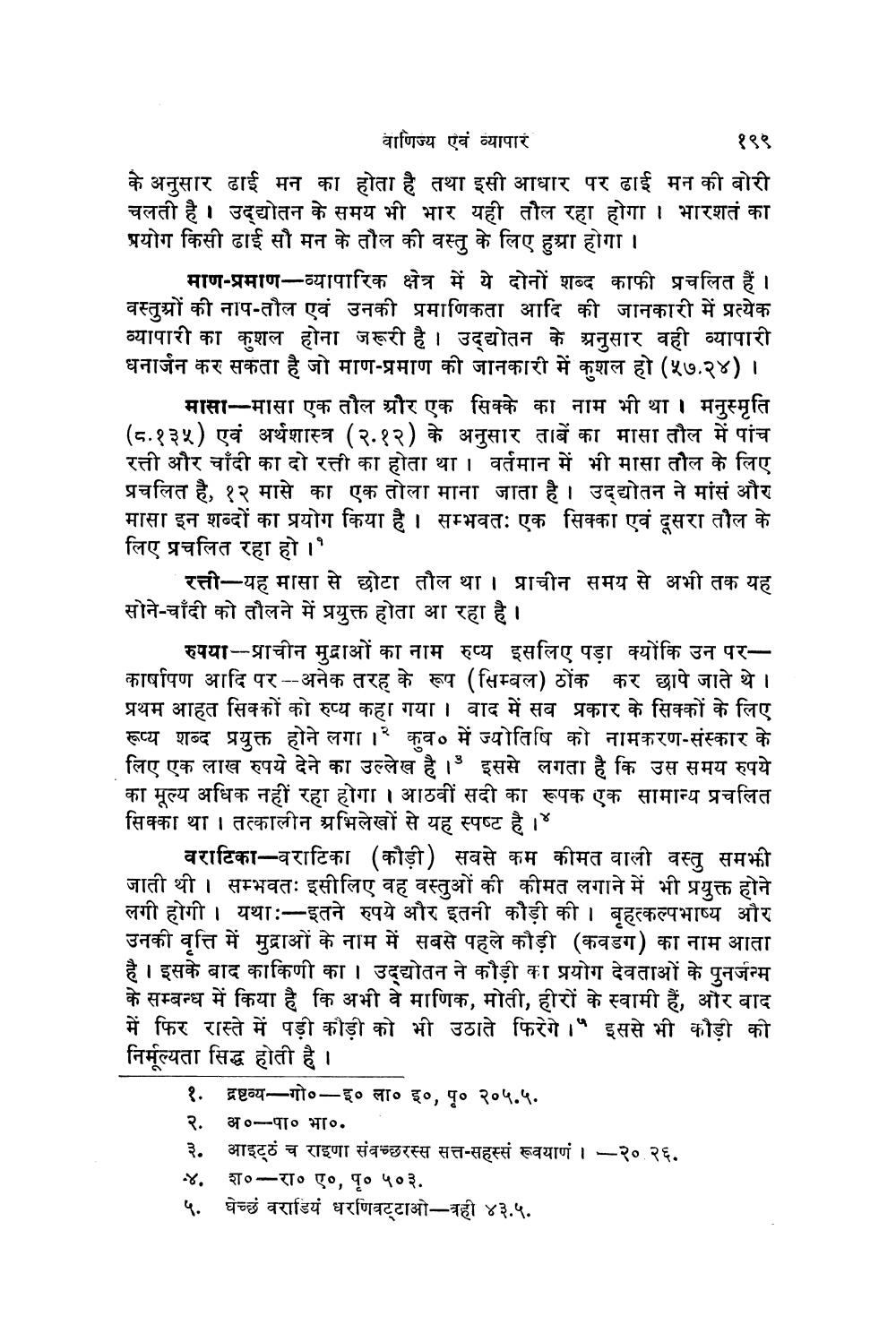________________
वाणिज्य एवं व्यापार
१९९ के अनुसार ढाई मन का होता है तथा इसी आधार पर ढाई मन की बोरी चलती है। उद्योतन के समय भी भार यही तौल रहा होगा । भारशतं का प्रयोग किसी ढाई सौ मन के तौल की वस्तु के लिए हुआ होगा।
माण-प्रमाण-व्यापारिक क्षेत्र में ये दोनों शब्द काफी प्रचलित हैं। वस्तुओं की नाप-तौल एवं उनकी प्रमाणिकता आदि की जानकारी में प्रत्येक व्यापारी का कुशल होना जरूरी है। उद्योतन के अनुसार वही व्यापारी धनार्जन कर सकता है जो माण-प्रमाण की जानकारी में कुशल हो (५७.२४) ।
मासा-मासा एक तौल और एक सिक्के का नाम भी था। मनुस्मृति (८.१३५) एवं अर्थशास्त्र (२.१२) के अनुसार ताबें का मासा तौल में पांच रत्ती और चाँदी का दो रत्ती का होता था। वर्तमान में भी मासा तौल के लिए प्रचलित है, १२ मासे का एक तोला माना जाता है। उद्योतन ने मांसं और मासा इन शब्दों का प्रयोग किया है। सम्भवतः एक सिक्का एवं दूसरा तौल के लिए प्रचलित रहा हो।'
रत्ती-यह मासा से छोटा तौल था। प्राचीन समय से अभी तक यह सोने-चाँदी को तौलने में प्रयुक्त होता आ रहा है।
रुपया-प्राचीन मुद्राओं का नाम रुप्य इसलिए पड़ा क्योंकि उन परकार्षापण आदि पर --अनेक तरह के रूप (सिम्बल) ठोंक कर छापे जाते थे। प्रथम आहत सिक्कों को रुप्य कहा गया। बाद में सब प्रकार के सिक्कों के लिए रूप्य शब्द प्रयुक्त होने लगा। कुव० में ज्योतिषि को नामकरण-संस्कार के लिए एक लाख रुपये देने का उल्लेख है। इससे लगता है कि उस समय रुपये का मूल्य अधिक नहीं रहा होगा। आठवीं सदी का रूपक एक सामान्य प्रचलित सिक्का था । तत्कालीन अभिलेखों से यह स्पष्ट है।
वराटिका-वराटिका (कौड़ी) सबसे कम कीमत वाली वस्तु समझी जाती थी। सम्भवतः इसीलिए वह वस्तुओं की कीमत लगाने में भी प्रयुक्त होने लगी होगी। यथा:-इतने रुपये और इतनी कौड़ी की। बृहत्कल्पभाष्य और उनकी वृत्ति में मुद्राओं के नाम में सबसे पहले कौड़ी (कवडग) का नाम आता है । इसके बाद काकिणी का । उद्द्योतन ने कौड़ी का प्रयोग देवताओं के पुनर्जन्म के सम्बन्ध में किया है कि अभी वे माणिक, मोती, हीरों के स्वामी हैं, और बाद में फिर रास्ते में पड़ी कौड़ी को भी उठाते फिरेगे।" इससे भी कौड़ी को निर्मूल्यता सिद्ध होती है।
द्रष्टव्य-गो०-इ० ला० इ०, पृ० २०५.५. २. अ०--पा० भा०.
आइट्ठं च राइणा संवच्छरस्स सत्त-सहस्सं रूवयाणं । -२०२६. ४. श०--रा० ए०, पृ० ५०३. ५. घेच्छं वराडियं धरणिवट्टाओ-वही ४३.५.
m