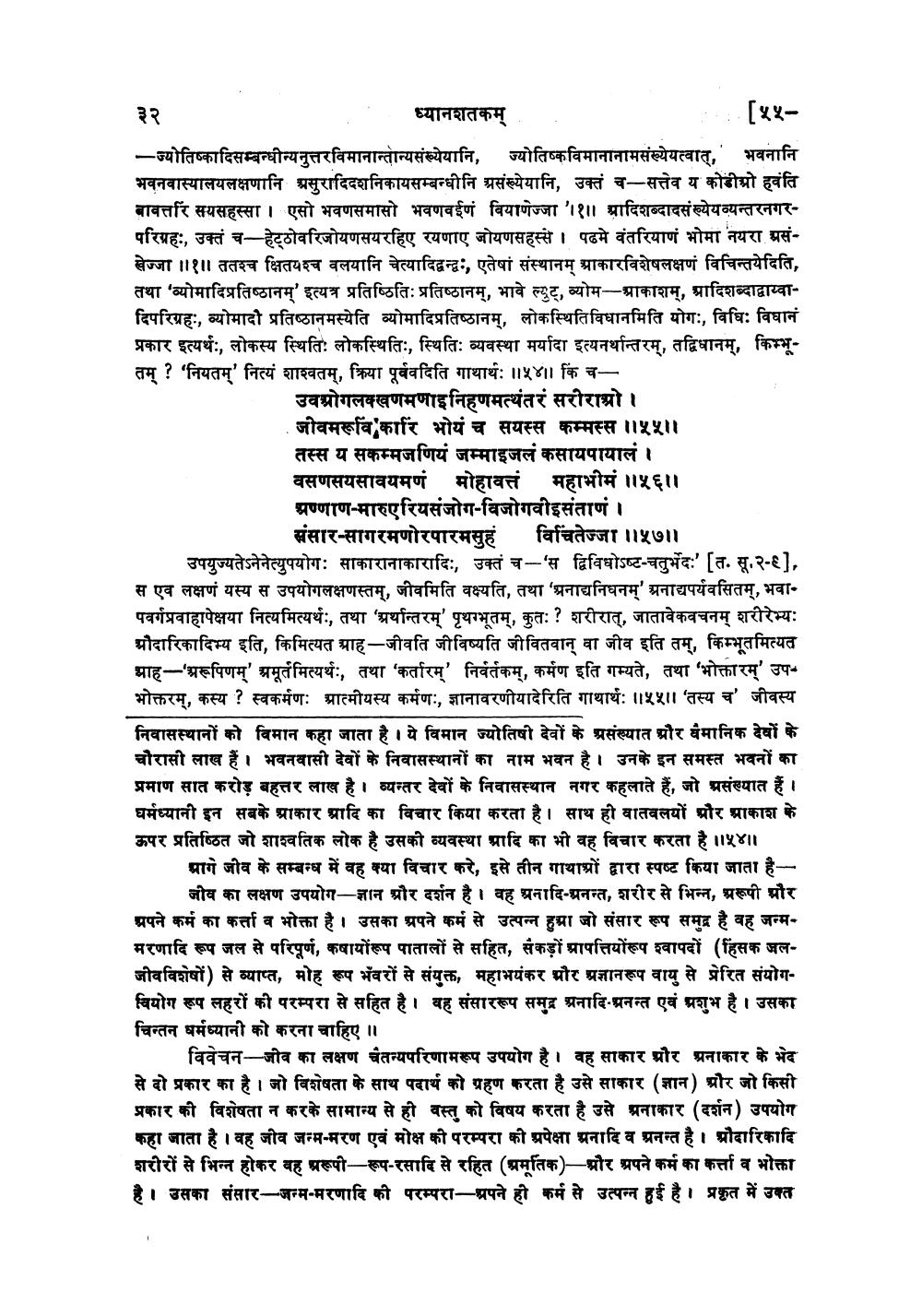________________
[५५
३२
- ज्योतिष्कादिसम्बन्धीन्यनुत्तरविमानान्तोन्यसंख्येयानि, ज्योतिष्कविमानानामसंख्येयत्वात्, ' भवनानि भवनवास्यालयलक्षणानि श्रसुरादिदशनिकायसम्बन्धीनि असंख्येयानि उक्तं च- सत्तेव य कोंडीग्रो हवंति बावतर सयसहस्सा । एसो भवणसमासो भवणवईणं बियाणेज्जा ' | १|| श्रादिशब्दादसंख्येय व्यन्तरनगरपरिग्रहः, उक्तं च- हेट्ठोवरिजोयणसयरहिए रयणाए जोयणसहस्से । पढमे वंतरियाणं भोमा नयरा असंखेज्जा ॥१॥ ततश्च क्षितयश्च वलयानि चेत्यादिद्वन्द्वः, एतेषां संस्थानम् आकारविशेषलक्षणं विचिन्तयेदिति, तथा 'व्योमादिप्रतिष्ठानम्' इत्यत्र प्रतिष्ठितिः प्रतिष्ठानम्, भावे ल्युट् व्योम - श्राकाशम्, श्रादिशब्दाद्वाय्वादिपरिग्रहः, व्योमादी प्रतिष्ठानमस्येति व्योमादिप्रतिष्ठानम्, लोकस्थितिविधानमिति योगः, विधिः विधानं प्रकार इत्यर्थः, लोकस्य स्थितिः लोकस्थितिः, स्थितिः व्यवस्था मर्यादा इत्यनर्थान्तरम्, तद्विधानम् किम्भूतम् ? 'नियतम्' नित्यं शाश्वतम्, क्रिया पूर्ववदिति गाथार्थः || ५४ || किचउवोगलक्खणमणाइनिहणमत्यंतरं सरीराम्रो । जीवमविकार भोयं च सयस्स कम्मस्स ॥५५॥ तस्स य सकम्मजणियं जम्माइजलं कसायपायालं । वसणसयसावयमणं मोहावत्तं महाभीमं ॥ ५६ ॥ अण्णाण - मारुएरियसंजोग - विजोगवीइसंताणं । संसार-सागरमणोरपारमसुहं विचितेज्जा ॥५७॥
उपयुज्यतेऽनेनेत्युपयोगः साकारानाकारादिः उक्तं च- 'स द्विविधोऽष्ट चतुर्भेद:' [त. सू.२ - [], स एव लक्षणं यस्य स उपयोगलक्षणस्तम्, जीवमिति वक्ष्यति, तथा 'श्रनाद्यनिधनम्' अनाद्यपर्यवसितम्, भवापवर्गप्रवाहापेक्षया नित्यमित्यर्थः तथा 'अर्थान्तरम्' पृथग्भूतम्, कुतः ? शरीरात्, जातावेकवचनम् शरीरेभ्यः श्रदारिकादिभ्य इति किमित्यत आह - जीवति जीविष्यति जीवितवान् वा जीव इति तम्, किम्भूतमित्यत ग्रह - 'अरूपिणम्' अमूर्तमित्यर्थः तथा 'कर्तारम्' निर्वर्तकम्, कर्मण इति गम्यते, तथा 'भोक्तारम्' उपभोक्तरम्, कस्य ? स्वकर्मणः आत्मीयस्य कर्मणः, ज्ञानावरणीयादेरिति गाथार्थः || ५५|| 'तस्य च' जीवस्य निवासस्थानों को विमान कहा जाता है। ये विमान ज्योतिषी देवों के श्रसंख्यात और वैमानिक देवों के चौरासी लाख हैं । भवनवासी देवों के निवासस्थानों का नाम भवन है। उनके इन समस्त भवनों का प्रमाण सात करोड़ बहत्तर लाख है । व्यन्तर देवों के निवासस्थान नगर कहलाते हैं, जो असंख्यात हैं । धर्मध्यानी इन सबके प्राकार श्रादि का विचार किया करता है। साथ ही वातवलयों और श्राकाश के ऊपर प्रतिष्ठित जो शाश्वतिक लोक है उसकी व्यवस्था आदि का भी वह विचार करता है ॥५४॥ प्रागे जीव के सम्बन्ध में वह क्या विचार करे, इसे तीन गाथाओं द्वारा स्पष्ट किया जाता हैजीव का लक्षण उपयोग - ज्ञान और दर्शन है। वह अनादि अनन्त, शरीर से भिन्न रूपी और अपने कर्म का कर्ता व भोक्ता है। उसका अपने कर्म से उत्पन्न हुआ जो संसार रूप समुद्र है वह जन्ममरणादि रूप जल से परिपूर्ण, कषायोंरूप पातालों से सहित, सैकड़ों प्रापत्तियोंरूप श्वापदों (हिंसक जलजीवविशेषों) से व्याप्त, मोह रूप भँवरों से संयुक्त, महाभयंकर और प्रज्ञानरूप वायु से प्रेरित संयोगवियोग रूप लहरों की परम्परा से सहित है। वह संसाररूप समुद्र अनादि अनन्त एवं अशुभ है । उसका चिन्तन धर्मध्यानी को करना चाहिए ॥
विवेचन - जीव का लक्षण चैतन्यपरिणामरूप उपयोग है। वह साकार और अनाकार के भेद से दो प्रकार का है । जो विशेषता के साथ पदार्थ को ग्रहण करता है उसे साकार (ज्ञान) और जो किसी प्रकार की विशेषता न करके सामान्य से ही वस्तु को विषय करता है उसे अनाकार (दर्शन) उपयोग कहा जाता है । वह जीव जन्म-मरण एवं मोक्ष की परम्परा की अपेक्षा अनादि व अनन्त है । प्रौदारिकादि शरीरों से भिन्न होकर वह श्ररूपी - रूप रसादि से रहित ( श्रमूर्तिक) — और अपने कर्म का कर्त्ता व भोक्ता है । उसका संसार – जन्म-मरणादि की परम्परा - अपने ही कर्म से उत्पन्न हुई है । प्रकृत में उक्त
1
ध्यानशतकम्