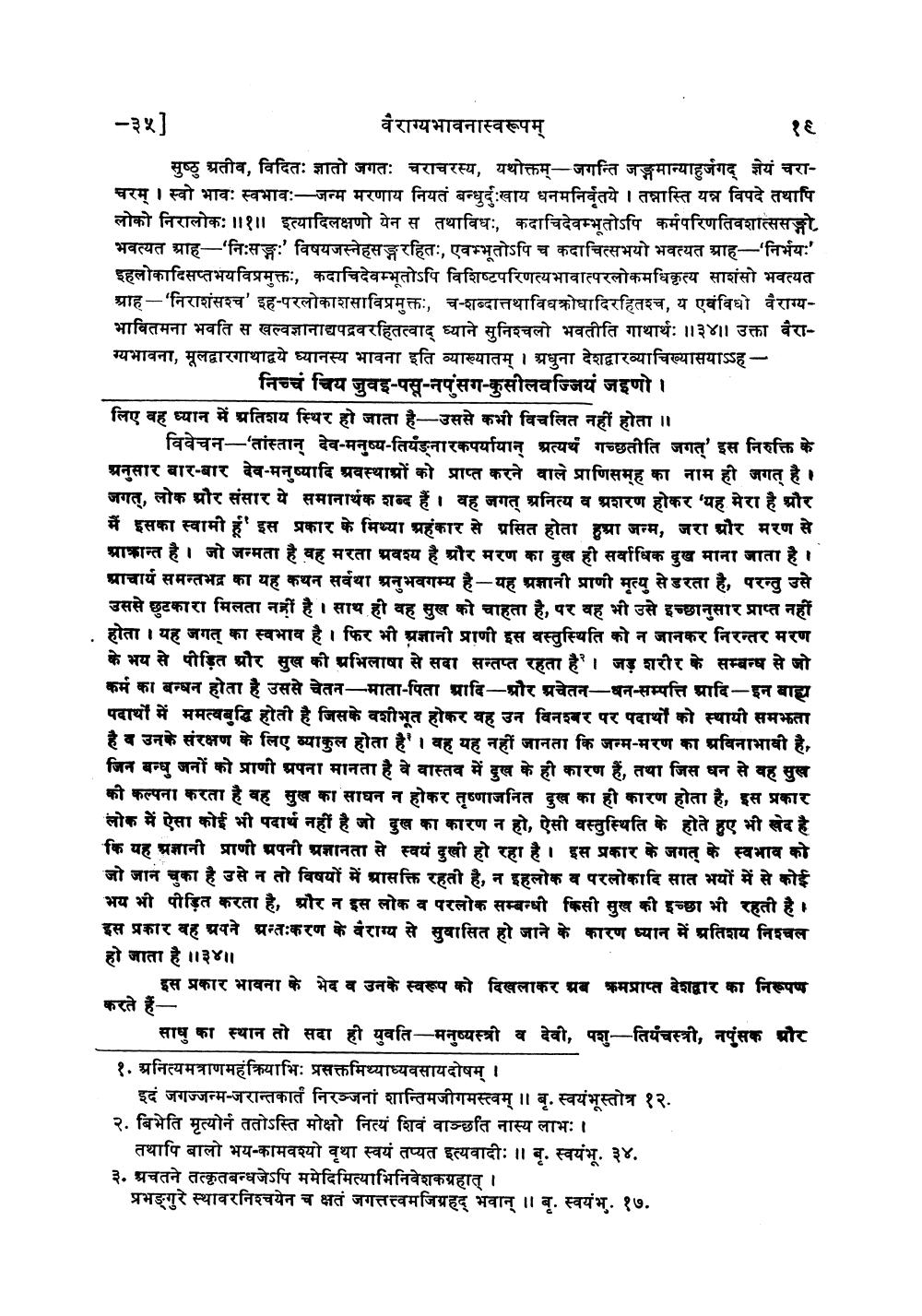________________
-३५]
वैराग्यभावनास्वरूपम्
सुष्ठु अतीव, विदितः ज्ञातो जगतः चराचरस्य, यथोक्तम्-जगन्ति जङ्गमान्याहुर्जगद् ज्ञेयं चराचरम् । स्वो भावः स्वभाव:-जन्म मरणाय नियतं बन्धुःखाय धनमनिर्वतये । तन्नास्ति यन्न विपदे तथापि लोको निरालोकः ॥१॥ इत्यादिलक्षणो येन स तथाविधः, कदाचिदेवम्भूतोऽपि कर्मपरिणतिवशात्ससङ्गो भवत्यत आह–'निःसङ्गः' विषयजस्नेहसङ्गरहितः, एवम्भूतोऽपि च कदाचित्सभयो भवत्यत आह–'निर्भय' इहलोकादिसप्तभयविप्रमुक्तः, कदाचिदेवम्भूतोऽपि विशिष्टपरिणत्यभावात्परलोकमधिकृत्य साशंसो भवत्यत पाह-निराशंसश्च' इह-परलोकाशसाविप्रमुक्तः, च-शब्दात्तथाविधक्रोधादिरहितश्च, य एवंविधो वैराग्यभावितमना भवति स खल्वज्ञानाद्यपद्रवरहितत्वाद् ध्याने सुनिश्चलो भवतीति गाथार्थः ॥३४।। उक्ता वैराग्यभावना, मूलद्वारगाथाद्वये ध्यानस्य भावना इति व्याख्यातम् । अधुना देशद्वारव्याचिख्यासयाह
निच्चं चिय जुवइ-पसू-नपुंसग-कुसीलवज्जियं जइणो। लिए वह ध्यान में अतिशय स्थिर हो जाता है-उससे कभी विचलित नहीं होता।
विवेचन–'तांस्तान देव-मनुष्य-तियङनारकपर्यायान प्रत्यर्थ गच्छतीति जगत' इस निरुक्ति के अनुसार बार-बार देव-मनुष्यादि अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले प्राणिसम्ह का नाम ही जगत् है। जगत्, लोक और संसार ये समानार्थक शब्द हैं। वह जगत् अनित्य व प्रशरण होकर 'यह मेरा है और में इसका स्वामी हूं' इस प्रकार के मिथ्या अहंकार से प्रसित होता हा जन्म, जरा और मरण से प्राक्रान्त है। जो जन्मता है वह मरता अवश्य है और मरण का दुख ही सर्वाधिक दुख माना जाता है।
चार्य समन्तभद्र का यह कथन सर्वथा अनभवगम्य है-यह अज्ञानी प्राणी मृत्यु से डरता है, परन्तु उसे उससे छुटकारा मिलता नहीं है । साथ ही वह सुख को चाहता है, पर वह भी उसे इच्छानुसार प्राप्त नहीं , होता । यह जगत् का स्वभाव है। फिर भी अज्ञानी प्राणी इस वस्तुस्थिति को न जानकर निरन्तर मरण
के भय से पीड़ित और सुख की अभिलाषा से सदा सन्तप्त रहता है। जड़ शरीर के सम्बन्ध से जो कर्म का बन्धन होता है उससे चेतन-माता-पिता प्रादि-और प्रचेतन-धन-सम्पत्ति प्रादि-इन बाह्य पदार्थों में ममत्वबुद्धि होती है जिसके वशीभूत होकर वह उन विनश्वर पर पदार्थों को स्थायी समझता है व उनके संरक्षण के लिए व्याकुल होता है। वह यह नहीं जानता कि जन्म-मरण का अविनाभावी है, जिन बन्धु जनों को प्राणी अपना मानता है वे वास्तव में दुख के ही कारण हैं, तथा जिस धन से वह सुख की कल्पना करता है वह सुख का साधन न होकर तृष्णाजनित दुख का ही कारण होता है, इस प्रकार लोक में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो दुख का कारण न हो, ऐसी वस्तुस्थिति के होते हुए भी खेद है कि यह अज्ञानी प्राणी अपनी प्रज्ञानता से स्वयं दुखी हो रहा है। इस प्रकार के जगत् के स्वभाव को जो जान चुका है उसे न तो विषयों में प्रासक्ति रहती है, न इहलोक व परलोकादि सात भयों में से कोई भय भी पीड़ित करता है, और न इस लोक व परलोक सम्बन्धी किसी सुख की इच्छा भी रहती है। इस प्रकार वह अपने अन्तःकरण के वैराग्य से सुवासित हो जाने के कारण ध्यान में अतिशय निश्चल हो जाता है ॥३४॥
इस प्रकार भावना के भेद व उनके स्वरूप को दिखलाकर अब क्रमप्राप्त देशद्वार का निरूपण करते हैं
साधु का स्थान तो सदा ही युवति–मनुष्यस्त्री व देवी, पशु-तियंचस्त्री, नपुंसक और १. अनित्यमत्राणमहंक्रियाभिः प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम् ।
इदं जगज्जन्म-जरान्तकात निरञ्जनां शान्तिमजीगमस्त्वम् ।। बृ. स्वयंभूस्तोत्र १२. २. बिभेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः ।
तथापि बालो भय-कामवश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥ बृ. स्वयंभू. ३४. ३. प्रचतने तत्कृतबन्धजेऽपि ममेदिमित्याभिनिवेशकग्रहात् । प्रभङ्गरे स्थावरनिश्चयेन च क्षतं जगत्तत्त्वमजिग्रहद् भवान् ।। 5. स्वयंभ. १७.