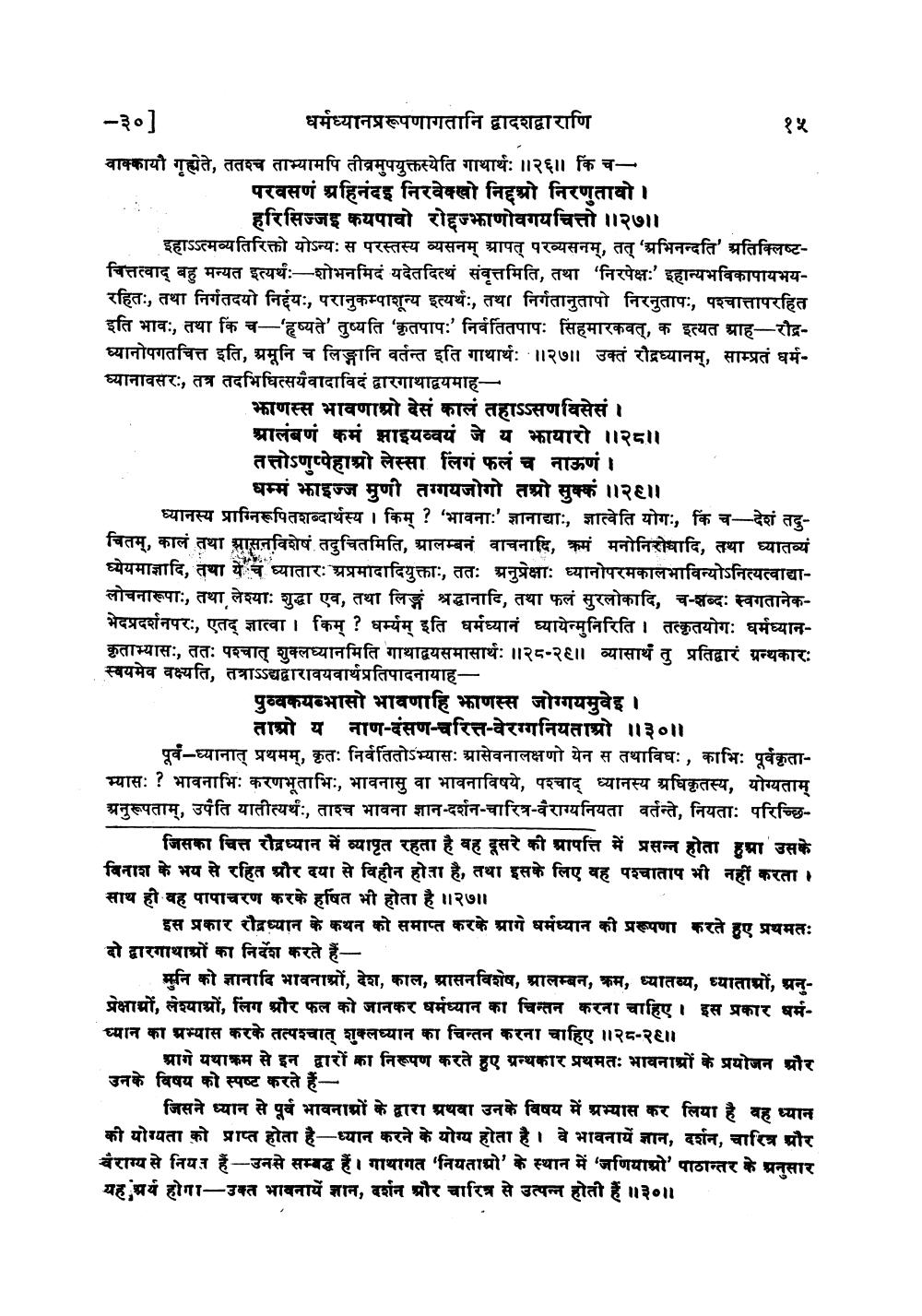________________
-३०]
धर्मध्यानप्ररूपणागतानि द्वादशद्वाराणि वाक्कायौ गृह्येते, ततश्च ताभ्यामपि तीव्रमुपयुक्तस्येति गाथार्थः ॥२६॥ किं च
परवसणं अहिनंदइ निरवेक्खो निद्दनो निरणुतायो।
हरिसिज्जइ कयपावो रोद्दज्झाणोवगयचित्तो ॥२७॥ इहाऽऽत्मव्यतिरिक्तो योऽन्यः स परस्तस्य व्यसनम् आपत् परव्यसनम्, तत् 'अभिनन्दति' प्रतिक्लिष्टचित्तत्वाद बह मन्यत इत्यर्थः-शोभनमिदं यदेतदित्थं संवृत्तमिति, तथा 'निरपेक्षः' इहान्यभविकापायभयरहितः, तथा निर्गतदयो निर्दयः, परानुकम्पाशून्य इत्यर्थः, तथा निर्गतानुतापो निरनुतापः, पश्चात्तापरहित इति भावः, तथा कि च–'हृष्यते' तुष्यति 'कृतपापः' निर्वतितपापः सिंहमारकवत्, क इत्यत आह-रौद्रध्यानोपगतचित्त इति, अमूनि च लिङ्गानि वर्तन्त इति गाथार्थः ॥२७॥ उक्तं रौद्रध्यानम्, साम्प्रतं धर्मध्यानावसरः, तत्र तदभिधित्सयवादाविदं द्वारगाथाद्वयमाह
झाणस्स भावणाम्रो देसं कालं तहाऽऽसणविसेसं। प्रालंबणं कम झाइयव्वयं जे य झायारो ॥२८॥ तत्तोऽणुप्पेहाम्रो लेस्सा लिंगं फलं च नाऊणं ।
धम्म झाइज्ज मुणी तग्गयजोगो तो सुक्कं ॥२६॥ ध्यानस्य प्राग्निरूपितशब्दार्थस्य । किम् ? 'भावनाः' ज्ञानाद्याः, ज्ञात्वेति योगः, किं च-देशं तदुचितम्, कालं तथा आसनविशेषं तदुचितमिति, पालम्बनं वाचनादि, क्रम मनोनिरोधादि, तथा ध्यातव्यं ध्येयमाज्ञादि, तथा ये च ध्यातारः अप्रमादादियुक्ताः, ततः अनुप्रेक्षाः ध्यानोपरमकालभाविन्योऽनित्यत्वाद्यालोचनारूपाः, तथा लेश्याः शुद्धा एव, तथा लिङ्गं श्रद्धानादि, तथा फलं सुरलोकादि, च-शब्दः स्वगतानेकभेदप्रदर्शनपरः, एतद् ज्ञात्वा। किम् ? धर्म्यम् इति धर्मध्यानं ध्यायेन्मुनिरिति। तत्कृतयोगः धर्मध्यानकृताभ्यासः, ततः पश्चात् शुक्लध्यानमिति गाथाद्वयसमासार्थः ॥२८-२९॥ व्यासार्थ तु प्रतिद्वारं ग्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति, तत्राऽऽद्यद्वारावयवार्थप्रतिपादनायाह
पुवकयन्भासो भावणाहि झाणस्स जोग्गयमुवेइ ।
ताप्रो य नाण-दंसण-चरित्त-वेरग्गनियताप्रो ॥३०॥ पूर्व-ध्यानात् प्रथमम्, कृतः निर्वतितोऽभ्यासः प्रासेवनालक्षणो येन स तथाविधः, काभिः पूर्वकृताभ्यासः ? भावनाभिः करणभूताभिः, भावनासु वा भावनाविषये, पश्चाद् ध्यानस्य अधिकृतस्य, योग्यताम् अनुरूपताम्, उपैति यातीत्यर्थः, ताश्च भावना ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वैराग्यनियता वर्तन्ते, नियताः परिच्छि
जिसका चित्त रौद्रध्यान में व्यापृत रहता है वह दूसरे की आपत्ति में प्रसन्न होता हमा उसके विनाश के भय से रहित और दया से विहीन होता है, तथा इसके लिए वह पश्चाताप भी नहीं करता। साथ ही वह पापाचरण करके हर्षित भी होता है ॥२७॥
इस प्रकार रौद्रध्यान के कथन को समाप्त करके आगे धर्मध्यान की प्ररूपणा करते हुए प्रथमतः दो द्वारगाथाओं का निर्देश करते हैं
मनि को ज्ञानादि भावनाओं, देश, काल, प्रासनविशेष, पालम्बन, क्रम, ध्यातव्य, ध्यातामों, अनप्रेक्षामों, लेश्याओं, लिंग और फल को जानकर धर्मध्यान का चिन्तन करना चाहिए। इस प्रकार धर्मध्यान का अभ्यास करके तत्पश्चात् शुक्लध्यान का चिन्तन करना चाहिए ॥२८-२६॥
आगे यथाक्रम से इन द्वारों का निरूपण करते हुए ग्रन्थकार प्रथमतः भावनात्रों के प्रयोजन और उनके विषय को स्पष्ट करते हैं
जिसने ध्यान से पूर्व भावनामों के द्वारा अथवा उनके विषय में अभ्यास कर लिया है वह ध्यान की योग्यता को प्राप्त होता है-ध्यान करने के योग्य होता है। वे भावनायें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य से नियत हैं-उनसे सम्बद्ध हैं। गाथागत 'नियताम्रो' के स्थान में 'जणियानो' पाठान्तर के अनुसार यह प्रर्य होगा-उक्त भावनायें ज्ञान, दर्शन और चारित्र से उत्पन्न होती हैं ॥३०॥