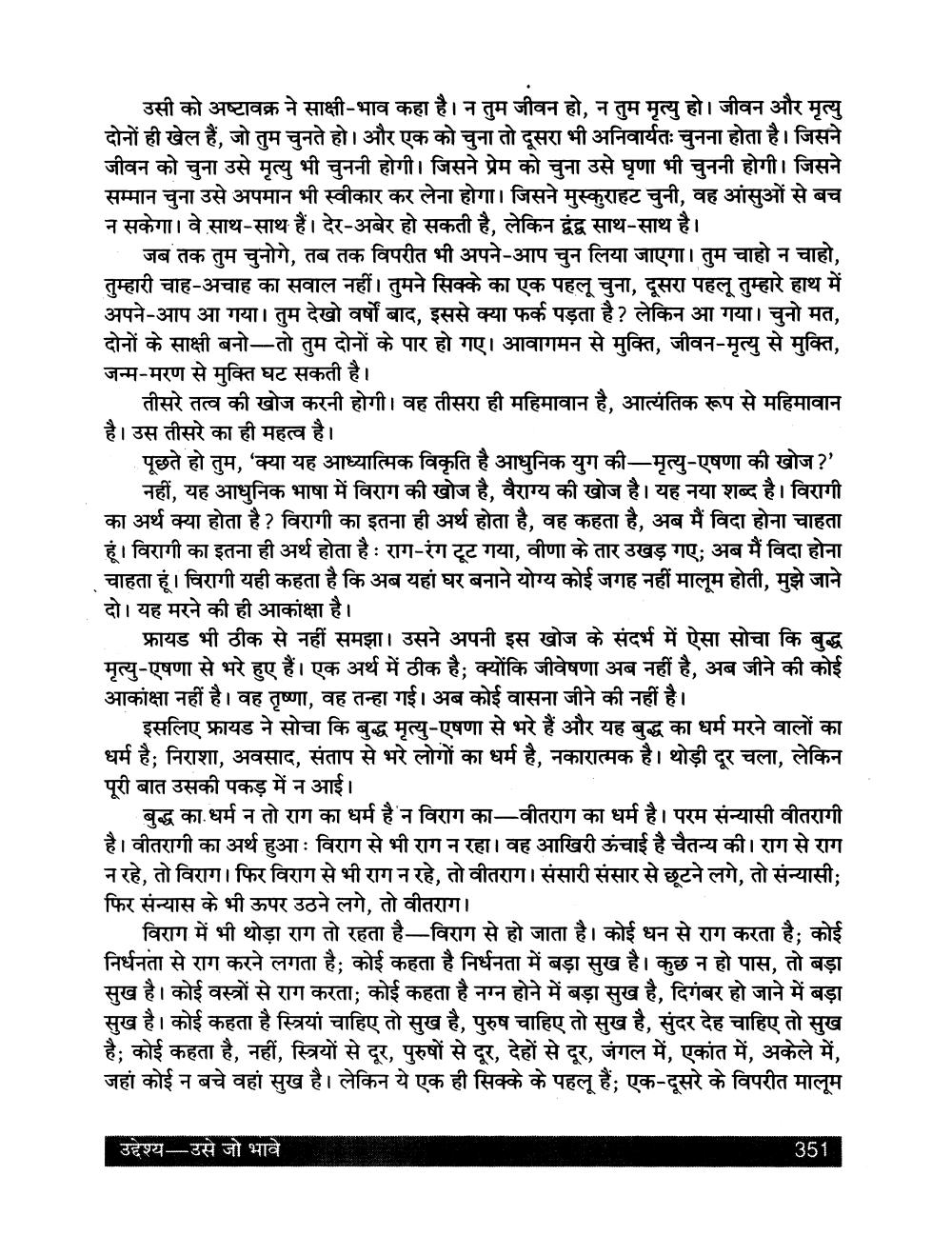________________
उसी को अष्टावक्र ने साक्षी भाव कहा है । न तुम जीवन हो, न तुम मृत्यु हो । जीवन और मृत्यु दोनों ही खेल हैं, जो तुम चुनते हो। और एक को चुना तो दूसरा भी अनिवार्यतः चुनना होता है। जिसने जीवन को चुना उसे मृत्यु भी चुननी होगी। जिसने प्रेम को चुना उसे घृणा भी चुननी होगी। जिसने सम्मान चुना उसे अपमान भी स्वीकार कर लेना होगा। जिसने मुस्कुराहट चुनी, वह आंसुओं से बच न सकेगा। वे साथ-साथ हैं। देर-अबेर हो सकती है, लेकिन द्वंद्व साथ-साथ है।
जब तक तुम चुनोगे, तब तक विपरीत भी अपने-आप चुन लिया जाएगा। तुम चाहो न चाहो, तुम्हारी चाह-अचाह का सवाल नहीं । तुमने सिक्के का एक पहलू चुना, दूसरा पहलू तुम्हारे हाथ में अपने-आप आ गया। तुम देखो वर्षों बाद, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आ गया। चुनो मत, दोनों के साक्षी बनो - तो तुम दोनों के पार हो गए। आवागमन से मुक्ति, जीवन-मृत्यु से मुक्ति, जन्म-मरण से मुक्ति घट सकती है।
I
तीसरे तत्व की खोज करनी होगी। वह तीसरा ही महिमावान है, आत्यंतिक रूप से महिमावान है । उस तीसरे का ही महत्व है।
-
पूछते हो तुम, 'क्या यह आध्यात्मिक विकृति है आधुनिक युग की — मृत्यु - एषणा की खोज ?" नहीं, यह आधुनिक भाषा में विराग की खोज है, वैराग्य की खोज है। यह नया शब्द है । विरागी का अर्थ क्या होता है? विरागी का इतना ही अर्थ होता है, वह कहता है, अब मैं विदा होना चाहता हूं। विरागी का इतना ही अर्थ होता है : राग-रंग टूट गया, वीणा के तार उखड़ गए; अब मैं विदा होना चाहता हूं। विरागी यही कहता है कि अब यहां घर बनाने योग्य कोई जगह नहीं मालूम होती, मुझे जाने दो। यह मरने की ही आकांक्षा है।
फ्रायड भी ठीक से नहीं समझा। उसने अपनी इस खोज के संदर्भ में ऐसा सोचा कि बुद्ध मृत्यु - एषणा से भरे हुए हैं । एक अर्थ में ठीक है; क्योंकि जीवेषणा अब नहीं है, अब जीने की कोई आकांक्षा नहीं है। वह तृष्णा, वह तन्हा गई। अब कोई वासना जीने की नहीं है ।
इसलिए फ्रायड ने सोचा कि बुद्ध मृत्यु-एषणा से भरे हैं और यह बुद्ध का धर्म मरने वालों का धर्म है; निराशा, अवसाद, संताप से भरे लोगों का धर्म है, नकारात्मक है। थोड़ी दूर चला, लेकिन पूरी बात उसकी पकड़ में न आई।
बुद्ध का धर्म न तो राग का धर्म हैं न विराग का – वीतराग का धर्म है । परम संन्यासी वीतरागी है। वीतरागी का अर्थ हुआ : विराग से भी राग न रहा । वह आखिरी ऊंचाई है चैतन्य की । राग से राग न रहे, तो विराग। फिर विराग से भी राग न रहे, तो वीतराग । संसारी संसार से छूटने लगे, तो संन्यासी; फिर संन्यास के भी ऊपर उठने लगे, तो वीतराग ।
विराग में भी थोड़ा राग तो रहता है -विराग से हो जाता है। कोई धन से राग करता है; कोई निर्धनता से राग करने लगता है; कोई कहता है निर्धनता में बड़ा सुख है। कुछ न हो पास, तो बड़ा सुख है। कोई वस्त्रों से राग करता; कोई कहता है नग्न होने में बड़ा सुख है, दिगंबर हो जाने में बड़ा सुख है। कोई कहता है स्त्रियां चाहिए तो सुख है, पुरुष चाहिए तो सुख है, सुंदर देह चाहिए तो सुख है; कोई कहता है, नहीं, स्त्रियों से दूर, पुरुषों से दूर, देहों से दूर, जंगल में, एकांत में, अकेले में, जहां कोई न बचे वहां सुख है । लेकिन ये एक ही सिक्के के पहलू हैं; एक-दूसरे के विपरीत मालूम
उद्देश्य — उसे जो भावे
351