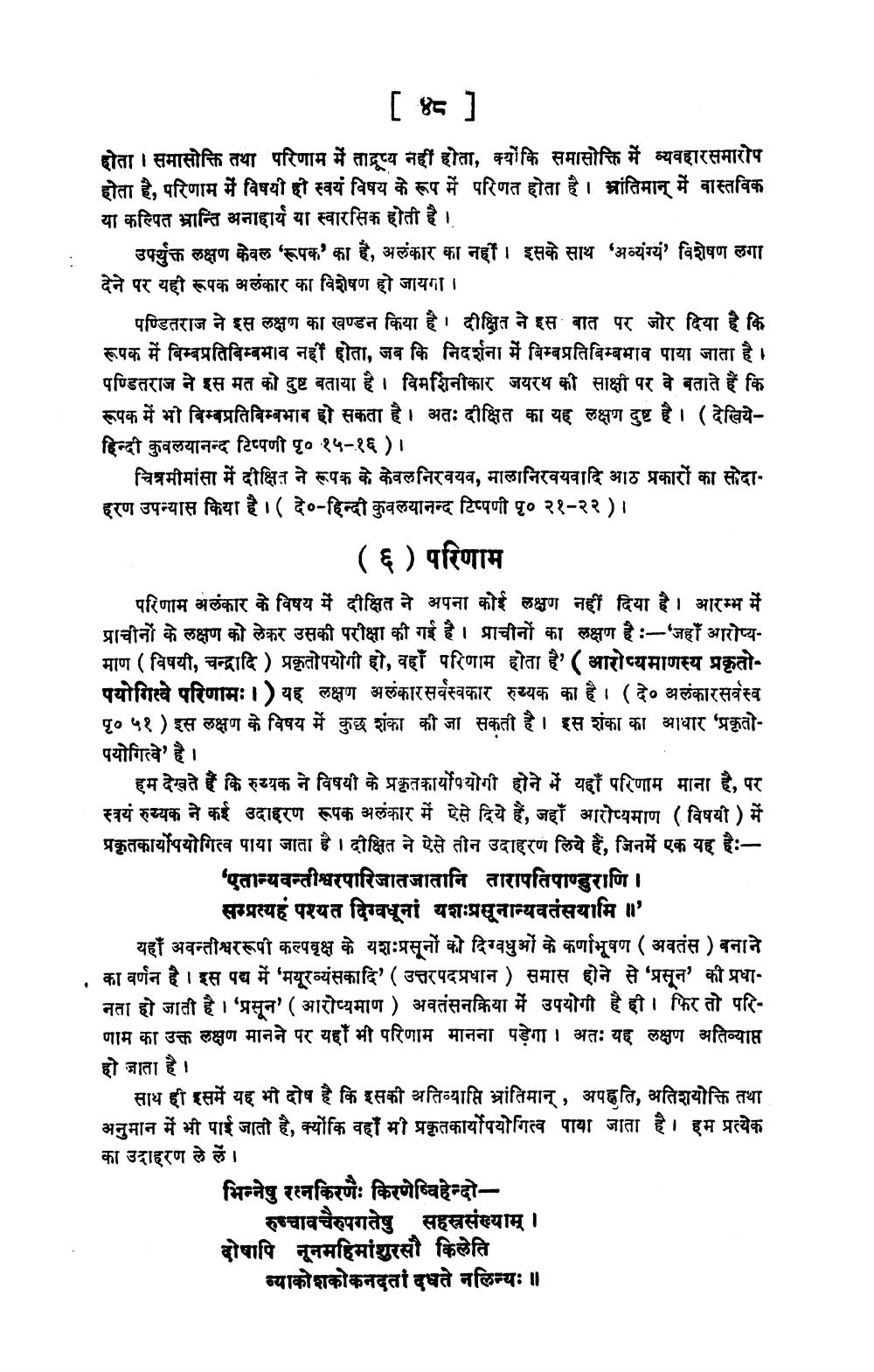________________
[४
]
होता । समासोक्ति तथा परिणाम में ताद्रूप्य नहीं होता, क्योंकि समासोक्ति में व्यवहारसमारोप होता है, परिणाम में विषयी ही स्वयं विषय के रूप में परिणत होता है। भ्रांतिमान में वास्तविक या कल्पित भ्रान्ति अनाहार्य या स्वारसिक होती है। ___ उपर्युक्त लक्षण केवल 'रूपक' का है, अलंकार का नहीं। इसके साथ 'अव्यंग्यं विशेषण लगा देने पर यही रूपक अलंकार का विशेषण हो जायगा ।
पण्डितराज ने इस लक्षण का खण्डन किया है। दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया है कि रूपक में बिम्बप्रतिबिम्बमाव नहीं होता, जब कि निदर्शना में बिम्बप्रतिबिम्बमाव पाया जाता है। पण्डितराज ने इस मत को दुष्ट बताया है। विमर्शिनीकार जयरथ की साक्षी पर वे बताते हैं कि रूपक में भी बिम्बप्रतिबिम्बभाव हो सकता है। अतः दीक्षित का यह लक्षण दुष्ट है। ( देखियेहिन्दी कुवलयानन्द टिप्पणी पृ० १५-१६)।
चित्रमीमांसा में दीक्षित ने रूपक के केवलनिरवयव, मालानिरवयवादि आठ प्रकारों का सोदा. हरण उपन्यास किया है । ( दे०-हिन्दी कुवलयानन्द टिप्पणी पृ० २१-२२)।
(६) परिणाम परिणाम अलंकार के विषय में दीक्षित ने अपना कोई लक्षण नहीं दिया है। आरम्भ में प्राचीनों के लक्षण को लेकर उसकी परीक्षा की गई है। प्राचीनों का लक्षण है :-'जहाँ आरोप्यमाण (विषयी, चन्द्रादि) प्रकृतोपयोगी हो, वहाँ परिणाम होता है' (आरोग्यमाणस्य प्रकृतो. पयोगिस्वे परिणामः।) यह लक्षण अलंकारसर्वस्वकार रुय्यक का है। (दे० अलंकारसर्वस्व पृ०५१) इस लक्षण के विषय में कुछ शंका की जा सकती है। इस शंका का आधार 'प्रकृतोपयोगित्वे' है।
हम देखते हैं कि रुय्यक ने विषयी के प्रकृतकार्योपयोगी होने में यहाँ परिणाम माना है, पर स्वयं रुय्यक ने कई उदाहरण रूपक अलंकार में ऐसे दिये हैं, जहाँ आरोप्यमाण (विषयी ) में प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है । दीक्षित ने ऐसे तीन उदाहरण लिये हैं, जिनमें एक यह है:
'एतान्यवन्तीश्वरपारिजातजातानि तारापतिपाण्डुराणि ।
सम्प्रत्यहं पश्यत दिग्वधूनां यशःप्रसूनान्यवतंसयामि ॥' यहाँ अवन्तीश्वररूपी कल्पवृक्ष के यशःप्रसूनों को दिग्वधुओं के कर्णाभूषण ( अवतंस ) बनाने . का वर्णन है । इस पद्य में 'मयूरव्यंसकादि' ( उत्तरपदप्रधान ) समास होने से 'प्रसून' की प्रधा.
नता हो जाती है । 'प्रसून' ( आरोप्यमाण) अवतंसनक्रिया में उपयोगी है ही। फिर तो परिणाम का उक्त लक्षण मानने पर यहाँ भी परिणाम मानना पड़ेगा। अतः यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाता है।
साथ ही इसमें यह भी दोष है कि इसकी अतिव्याप्ति भ्रांतिमान् , अपह्नति, अतिशयोक्ति तथा अनुमान में भी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ भी प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है। हम प्रत्येक का उदाहरण ले लें।
भिन्नेषु रत्नकिरणैः किरणेविहेन्दो
रुच्चावचैरुपगतेषु सहस्रसंख्याम् । दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति
व्याकोशकोकनदता दधते नलिन्यः॥