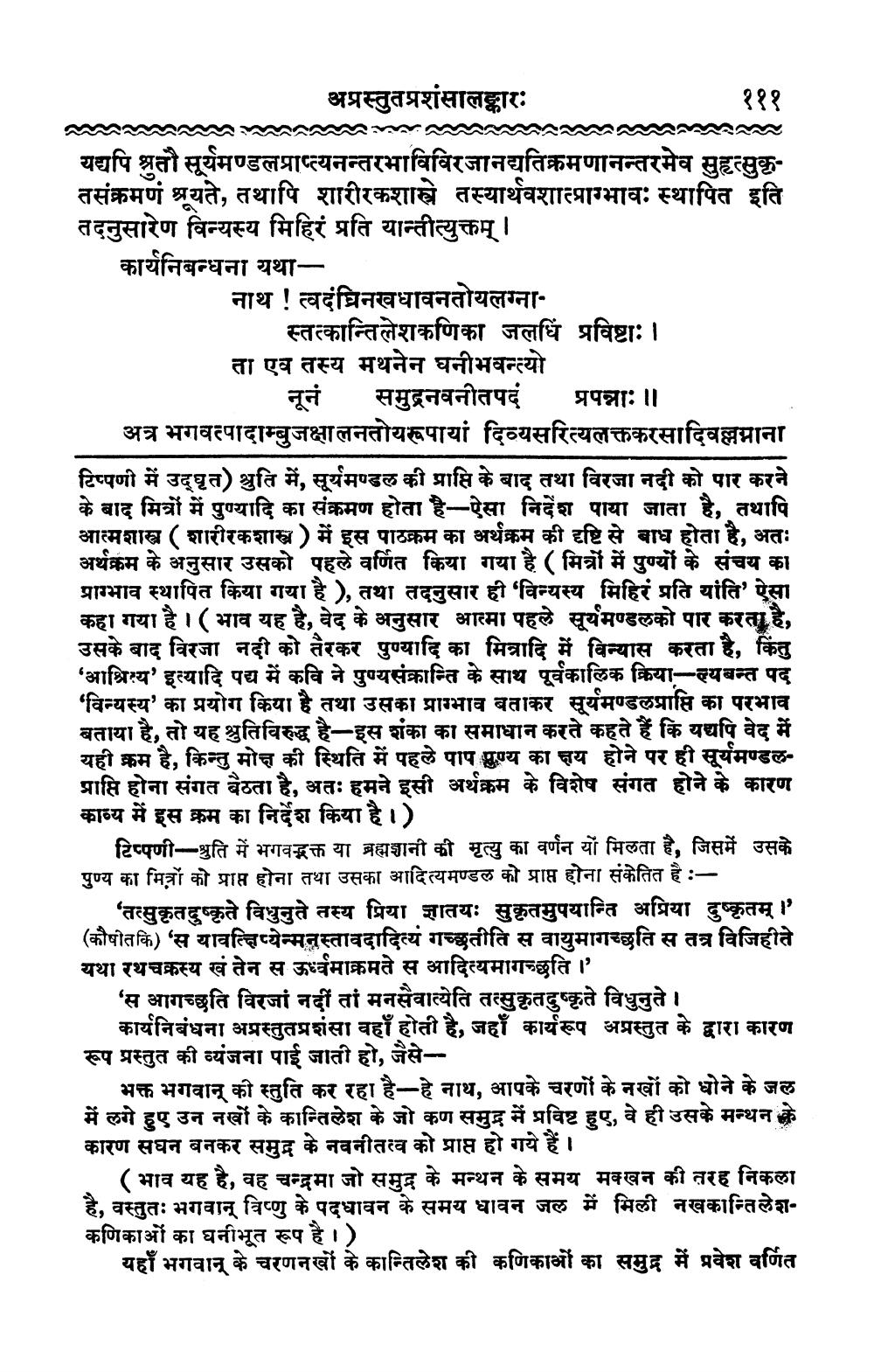________________
अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः
१११
यद्यपि श्रुतौ सूर्यमण्डलप्राप्त्यनन्तरभाविविरजानद्यतिक्रमणानन्तरमेव सुहृत्सुकृतसंक्रमणं श्रूयते, तथापि शारीरकशास्त्रे तस्यार्थवशात्प्राग्भावः स्थापित इति तदनुसारेण विन्यस्य मिहिरं प्रति यान्तीत्युक्तम् । कार्यनिबन्धना यथा
नाथ ! त्वदंघ्रिनखधावनतोयलग्ना
स्तत्कान्तिलेशकणिका जलधिं प्रविष्टाः। ता एव तस्य मथनेन घनीभवन्त्यो
नूनं समुद्रनवनीतपदं प्रपन्नाः ॥ अत्र भगवत्पादाम्बुजक्षालनतोयरूपायां दिव्यसरित्यलक्तकरसादिवल्लग्नाना टिप्पणी में उद्धृत) श्रुति में, सूर्यमण्डल की प्राप्ति के बाद तथा विरजा नदी को पार करने के बाद मित्रों में पुण्यादि का संक्रमण होता है-ऐसा निदेश पाया जाता है, तथापि आत्मशास्त्र (शारीरकशास्त्र) में इस पाठक्रम का अर्थक्रम की दृष्टि से बाध होता है, अतः अर्थक्रम के अनुसार उसको पहले वर्णित किया गया है (मित्रों में पुण्यों के संचय का प्राग्भाव स्थापित किया गया है), तथा तदनुसार ही 'विन्यस्य मिहिरं प्रति यांति' ऐसा कहा गया है। (भाव यह है, वेद के अनुसार आत्मा पहले सूर्यमण्डलको पार करता है, उसके बाद विरजा नदी को तैरकर पुण्यादि का मित्रादि में विन्यास करता है, किंतु 'आश्रित्य' इत्यादि पद्य में कवि ने पुण्यसंक्रान्ति के साथ पूर्वकालिक क्रिया-ल्यबन्त पद 'विन्यस्य' का प्रयोग किया है तथा उसका प्राग्भाव बताकर सूर्यमण्डलप्राप्ति का परभाव बताया है, तो यह श्रुतिविरुद्ध है-इस शंका का समाधान करते कहते हैं कि यद्यपि वेद में यही क्रम है, किन्तु मोक्ष की स्थिति में पहले पाप पुण्य का क्षय होने पर ही सूर्यमण्डलप्राप्ति होना संगत बैठता है, अतः हमने इसी अर्थक्रम के विशेष संगत होने के कारण काव्य में इस क्रम का निर्देश किया है।)
टिप्पणी-श्रुति में भगवद्भक्त या ब्रह्मज्ञानी की मृत्यु का वर्णन यों मिलता है, जिसमें उसके पुण्य का मित्रों को प्राप्त होना तथा उसका आदित्यमण्डल को प्राप्त होना संकेतित है :
'तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयान्ति अप्रिया दुष्कृतम् ।' (कौषीतकि) 'स यावक्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छतीति स वायुमागच्छति स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति ।' ।
'स आगच्छति विरजां नदी तां मनसैवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते ।
कार्यनिबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होती है, जहाँ कार्यरूप अप्रस्तुत के द्वारा कारण रूप प्रस्तुत की व्यंजना पाई जाती हो, जैसे
भक्त भगवान् की स्तुति कर रहा है-हे नाथ, आपके चरणों के नखों को धोने के जल में लगे हुए उन नखों के कान्तिलेश के जो कण समुद्र में प्रविष्ट हुए, वे ही उसके मन्थन के कारण सघन बनकर समुद्र के नवनीतत्व को प्राप्त हो गये हैं।
(भाव यह है, वह चन्द्रमा जो समुद्र के मन्थन के समय मक्खन की तरह निकला है, वस्तुतः भगवान् विष्णु के पदधावन के समय धावन जल में मिली नखकान्तिलेशकणिकाओं का घनीभूत रूप है।) __ यहाँ भगवान् के चरणनखों के कान्तिलेश की कणिकाओं का समुद्र में प्रवेश वर्णित