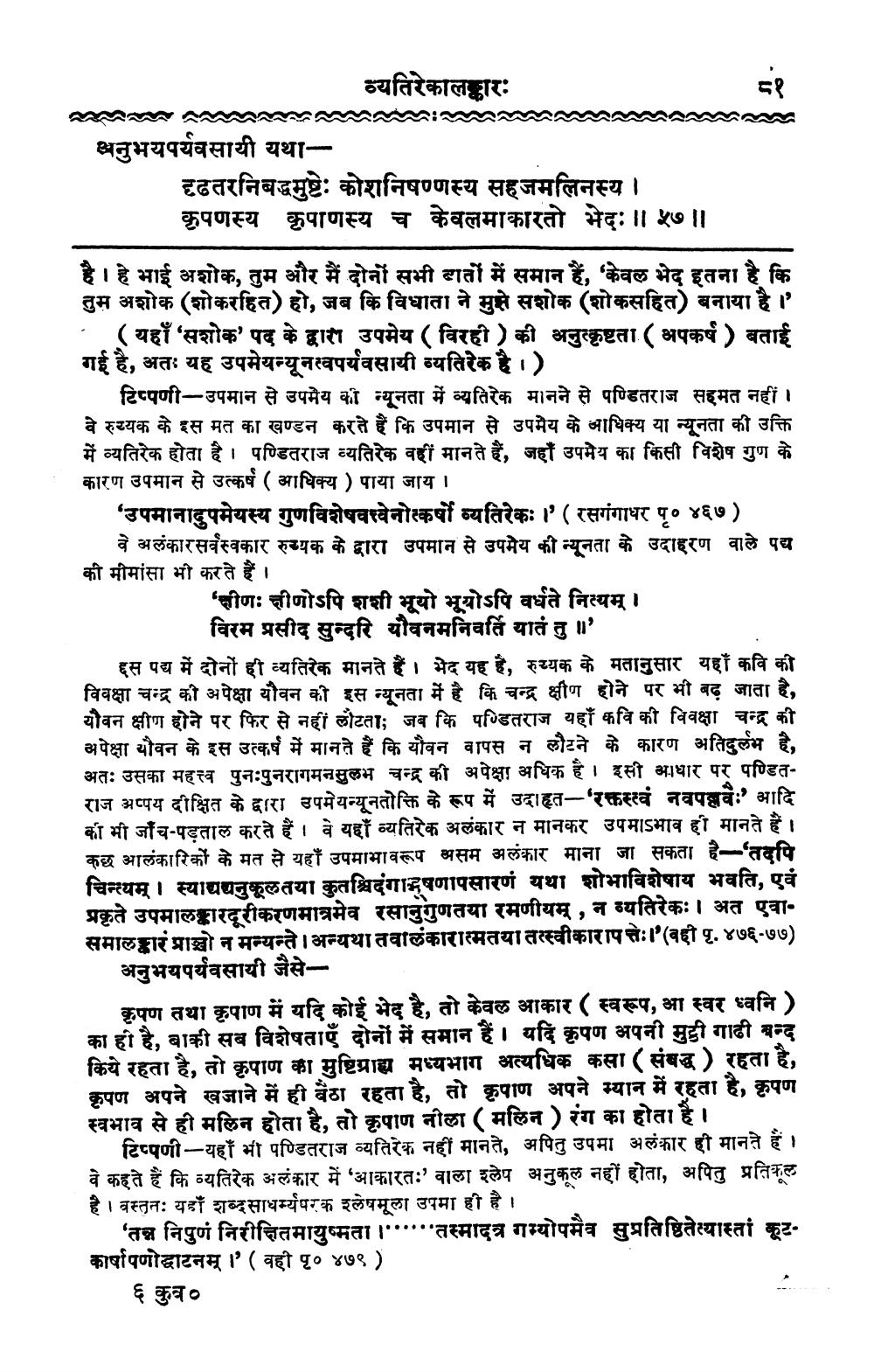________________
www
अनुभयपर्यवसायी यथा
व्यतिरेकालङ्कारः
तर निबद्धमुष्टेः कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ।। ५७ ।।
=
है । हे भाई अशोक, तुम और मैं दोनों सभी बातों में समान हैं, 'केवल भेद इतना है कि तुम अशोक (शोकरहित) हो, जब कि विधाता ने मुझे सशोक (शोकसहित ) बनाया है ।"
( यहाँ 'सशोक' पद के द्वारा उपमेय ( विरही ) की अनुत्कृष्टता ( अपकर्ष ) बताई गई है, अतः यह उपमेयन्यूनत्वपर्यवसायी व्यतिरेक है । )
टिप्पणी- - उपमान से उपमेय की न्यूनता में व्यतिरेक मानने से पण्डितराज सहमत नहीं । वे रुय्यक के इस मत का खण्डन करते हैं कि उपमान से उपमेय के आधिक्य या न्यूनता की उक्ति में व्यतिरेक होता है । पण्डितराज व्यतिरेक वहीं मानते हैं, जहाँ उपमेय का किसी विशेष गुण के कारण उपमान से उत्कर्ष ( आधिक्य ) पाया जाय ।
'उपमानादुपमेयस्य गुणविशेषवश्वेनोत्कर्षो व्यतिरेकः । ' ( रसगंगाधर पृ० ४६७ )
वे अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक के द्वारा उपमान से उपमेय की न्यूनता के उदाहरण वाले पद्य की मीमांसा भी करते हैं ।
'क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽपि वर्धते नित्यम् । विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥
इस पद्य में दोनों ही व्यतिरेक मानते हैं । भेद यह है, रुय्यक के मतानुसार यहाँ कवि की विवक्षा चन्द्र की अपेक्षा यौवन की इस न्यूनता में है कि चन्द्र क्षीण होने पर भी बढ़ जाता है, यौवन क्षीण होने पर फिर से नहीं लौटता; जब कि पण्डितराज यहाँ कवि की विवक्षा चन्द्र की अपेक्षा यौवन के इस उत्कर्ष में मानते हैं कि यौवन वापस न लौटने के कारण अतिदुर्लभ है, अतः उसका महत्त्व पुनःपुनरागमन सुलभ चन्द्र की अपेक्षा अधिक है। इसी आधार पर पण्डितराज अप्पय दीक्षित के द्वारा उपमेयन्यूनतोक्ति के रूप में उदाहृत- 'रक्तस्त्वं नवपल्लवैः' आदि की भी जाँच-पड़ताल करते हैं। वे यहाँ व्यतिरेक अलंकार न मानकर उपमाऽभाव ही मानते हैं । कुछ आलंकारिकों के मत से यहाँ उपमाभावरूप असम अलंकार माना जा सकता है—'तदपि चिन्त्यम् । स्याद्यद्यनुकूलतया कुतश्चिदंगाषणापसारणं यथा शोभाविशेषाय भवति, एवं प्रकृते उपमालङ्कारदूरीकरणमात्रमेव रसानुगुणतया रमणीयम्, न व्यतिरेकः । अत एवासमालङ्कारं प्राञ्चो न मन्यन्ते । अन्यथा तवालंकारात्मतया तत्स्वीकार राप प्तेः । ( वही पृ. ४७६-७७) अनुभयपर्यवसायी जैसे
कृपण तथा कृपाण में यदि कोई भेद है, तो केवल आकार ( स्वरूप, आ स्वर ध्वनि ) का ही है, बाकी सब विशेषताएँ दोनों में समान हैं। यदि कृपण अपनी मुट्ठी गाढी बन्द किये रहता है, तो कृपाण का मुष्टिग्राह्य मध्यभाग अत्यधिक कसा (संबद्ध ) रहता है, कृपण अपने खजाने में ही बैठा रहता है, तो कृपाण अपने म्यान में रहता है, कृपण स्वभाव से ही मलिन होता है, तो कृपाण नीला ( मलिन ) रंग का होता है ।
टिप्पणी- यहाँ भी पण्डितराज व्यतिरेक नहीं मानते, अपितु उपमा अलंकार ही मानते हैं । वे कहते हैं कि व्यतिरेक अलंकार में 'आकारतः ' वाला इलेप अनुकूल नहीं होता, अपितु प्रतिकूल है । वस्तुतः यहाँ शब्दसाधर्म्यपरक श्लेषमूला उपमा ही है ।
'तन्न निपुणं निरीक्षितमायुष्मता ।...... " तस्मादत्र गम्योपमैव सुप्रतिष्ठितेत्यास्तां कूटकार्षापणोद्घाटनम् ।' ( वही पृ० ४७९ )
६ कुत्र ०