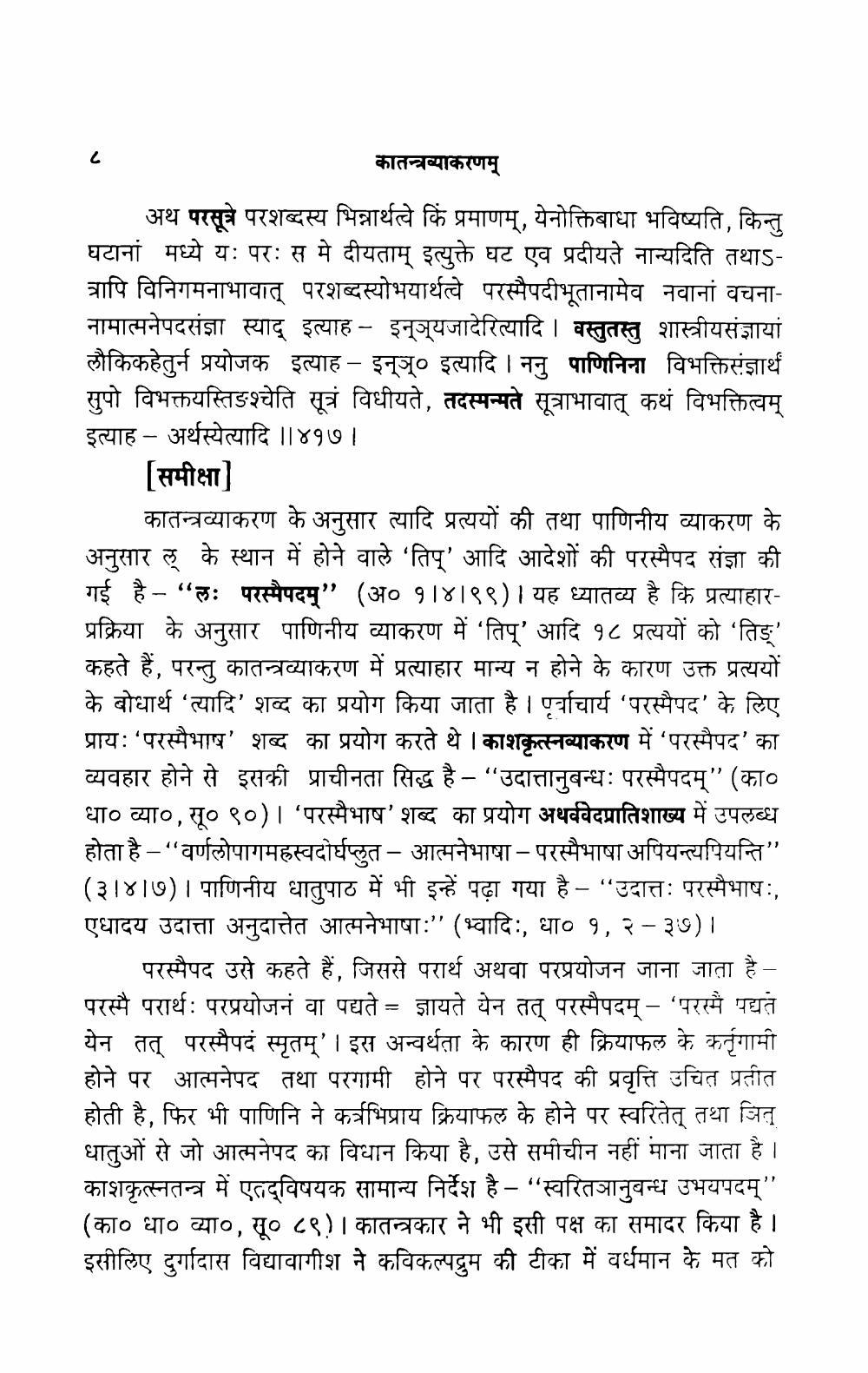________________
कातन्त्रव्याकरणम्
अथ परसूत्रे परशब्दस्य भिन्नार्थत्वे किं प्रमाणम्, येनोक्तिबाधा भविष्यति, किन्तु घटानां मध्ये यः परः स मे दीयताम् इत्युक्ते घट एव प्रदीयते नान्यदिति तथाऽत्रापि विनिगमनाभावात् परशब्दस्योभयार्थत्वे परस्मैपदीभूतानामेव नवानां वचनानामात्मनेपदसंज्ञा स्याद् इत्याह - इयजादेरित्यादि । वस्तुतस्तु शास्त्रीयसंज्ञायां लौकिकहेतुर्न प्रयोजक इत्याह – इञ्० इत्यादि । ननु पाणिनिना विभक्तिसंज्ञार्थं सुपो विभक्तयस्तिङश्चेति सूत्रं विधीयते, तदस्मन्मते सूत्राभावात् कथं विभक्तित्वम् इत्याह - अर्थस्येत्यादि ।। ४१७ ।
[समीक्षा
कातन्त्रव्याकरण के अनुसार त्यादि प्रत्ययों की तथा पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ल् के स्थान में होने वाले 'तिप्' आदि आदेशों की परस्मैपद संज्ञा की गई है - "लः परस्मैपदम्" (अ० १।४।९९)। यह ध्यातव्य है कि प्रत्याहारप्रक्रिया के अनुसार पाणिनीय व्याकरण में 'तिप्' आदि १८ प्रत्ययों को ‘तिङ्' कहते हैं, परन्तु कातन्त्रव्याकरण में प्रत्याहार मान्य न होने के कारण उक्त प्रत्ययों के बोधार्थ 'त्यादि' शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूर्वाचार्य 'परस्मैपद' के लिए प्राय: ‘परस्मैभाष' शब्द का प्रयोग करते थे । काशकृत्स्नव्याकरण में परस्मैपद' का व्यवहार होने से इसकी प्राचीनता सिद्ध है - "उदात्तानुबन्धः परस्मैपदम्' (का० धा० व्या०, सू० ९०)। 'परस्मैभाष' शब्द का प्रयोग अथर्ववेदप्रातिशाख्य में उपलब्ध होता है - "वर्णलोपागमहस्वदोघप्लुत - आत्मनेभाषा-परस्मैभाषा अपियन्त्यपियन्ति" (३।४।७) । पाणिनीय धातुपाठ में भी इन्हें पढ़ा गया है – “उदात्तः परस्मैभाषः, एधादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा:' (भ्वादिः, धा० १, २ - ३७)।
परस्मैपद उसे कहते हैं, जिससे परार्थ अथवा परप्रयोजन जाना जाता है - परस्मै परार्थ : परप्रयोजनं वा पद्यते = ज्ञायते येन तत् परस्मैपदम् – 'परस्में पद्यत येन तत् परस्मैपदं स्मृतम्' । इस अन्वर्थता के कारण ही क्रियाफल के कर्तृगामी होने पर आत्मनेपद तथा परगामी होने पर परस्मैपद की प्रवृत्ति उचित प्रतीत होती है, फिर भी पाणिनि ने कत्रभिप्राय क्रियाफल के होने पर स्वरितेत् तथा जित धातुओं से जो आत्मनेपद का विधान किया है, उसे समीचीन नहीं माना जाता है । काशकृत्स्नतन्त्र में एतद्विषयक सामान्य निर्देश है - "स्वरितञानुबन्ध उभयपदम्" (का० धा० व्या०, सू० ८९) । कातन्त्रकार ने भी इसी पक्ष का समादर किया है । इसीलिए दुर्गादास विद्यावागीश ने कविकल्पद्रुम की टीका में वर्धमान के मत को