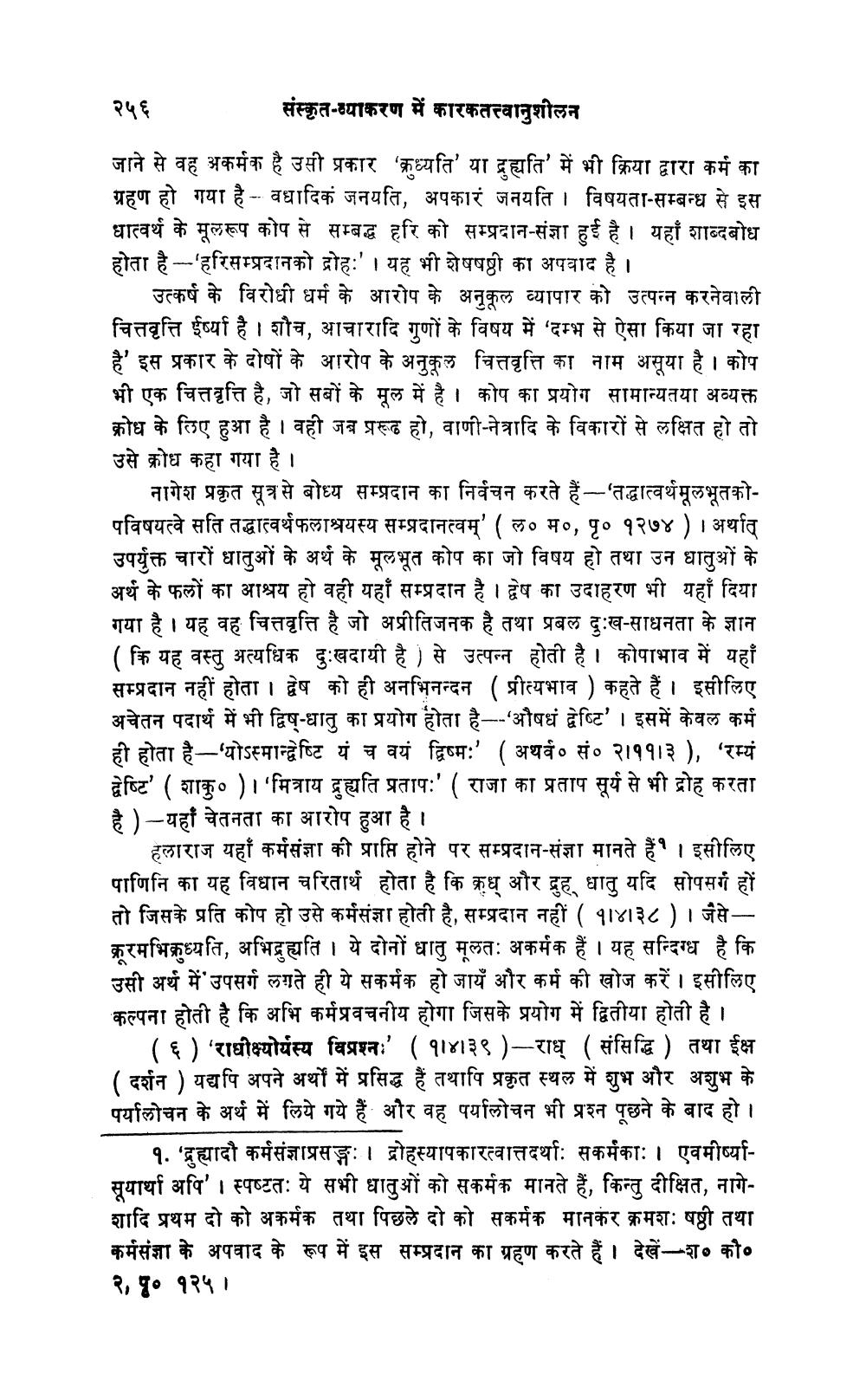________________
२५६ संस्कृत-व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन जाने से वह अकर्मक है उसी प्रकार 'क्रुध्यति' या द्रुह्यति' में भी क्रिया द्वारा कर्म का ग्रहण हो गया है -- वधादिकं जनयति, अपकारं जनयति । विषयता-सम्बन्ध से इस धात्वर्थ के मूलरूप कोप से सम्बद्ध हरि को सम्प्रदान-संज्ञा हुई है। यहाँ शाब्दबोध होता है ---'हरिसम्प्रदानको द्रोहः' । यह भी शेषषष्ठी का अपवाद है ।
उत्कर्ष के विरोधी धर्म के आरोप के अनुकूल व्यापार को उत्पन्न करनेवाली चित्तवृत्ति ईर्ष्या है । शौच, आचारादि गुणों के विषय में 'दम्भ से ऐसा किया जा रहा है' इस प्रकार के दोषों के आरोप के अनुकूल चित्तवृत्ति का नाम असूया है । कोप भी एक चित्तवृत्ति है, जो सबों के मूल में है। कोप का प्रयोग सामान्यतया अव्यक्त क्रोध के लिए हुआ है । वही जब प्ररूढ हो, वाणी-नेत्रादि के विकारों से लक्षित हो तो उसे क्रोध कहा गया है। ___ नागेश प्रकृत सूत्र से बोध्य सम्प्रदान का निर्वचन करते हैं-'तद्वात्वर्थमूलभूतकोपविषयत्वे सति तद्धात्वर्थफलाश्रयस्य सम्प्रदानत्वम्' ( ल० म०, पृ० १२७४ ) । अर्थात् उपर्युक्त चारों धातुओं के अर्थ के मूलभूत कोप का जो विषय हो तथा उन धातुओं के अर्थ के फलों का आश्रय हो वही यहाँ सम्प्रदान है । द्वेष का उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। यह वह चित्तवृत्ति है जो अप्रीतिजनक है तथा प्रबल दुःख-साधनता के ज्ञान ( कि यह वस्तु अत्यधिक दुःखदायी है ) से उत्पन्न होती है। कोपाभाव में यहाँ सम्प्रदान नहीं होता । द्वेष को ही अनभिनन्दन (प्रीत्यभाव ) कहते हैं। इसीलिए अचेतन पदार्थ में भी द्विष्-धातु का प्रयोग होता है--'औषधं द्वेष्टि' । इसमें केवल कर्म ही होता है—'योऽस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः' ( अथर्व० सं० २।११।३ ), 'रम्यं द्वेष्टि' ( शाकु० )। 'मित्राय द्रुह्यति प्रतापः' ( राजा का प्रताप सूर्य से भी द्रोह करता है )-यहाँ चेतनता का आरोप हुआ है।
हलाराज यहाँ कर्मसंज्ञा की प्राप्ति होने पर सम्प्रदान-संज्ञा मानते हैं । इसीलिए पाणिनि का यह विधान चरितार्थ होता है कि वध और द्रुह धातु यदि सोपसर्ग हों तो जिसके प्रति कोप हो उसे कर्मसंज्ञा होती है, सम्प्रदान नहीं ( १।४।३८ ) । जैसेकरमभिध्यति, अभिद्रुह्यति । ये दोनों धातु मूलतः अकर्मक हैं । यह सन्दिग्ध है कि उसी अर्थ में उपसर्ग लगते ही ये सकर्मक हो जायँ और कर्म की खोज करें। इसीलिए कल्पना होती है कि अभि कर्मप्रवचनीय होगा जिसके प्रयोग में द्वितीया होती है।
(६ ) 'राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः' (१।४।३९ )-राध् ( संसिद्धि ) तथा ईक्ष ( दर्शन ) यद्यपि अपने अर्थों में प्रसिद्ध हैं तथापि प्रकृत स्थल में शुभ और अशुभ के पर्यालोचन के अर्थ में लिये गये हैं और वह पर्यालोचन भी प्रश्न पूछने के बाद हो।
१. 'ह्यादौ कर्मसंज्ञाप्रसङ्गः । द्रोहस्यापकारत्वात्तदर्थाः सकर्मकाः । एवमासूयार्था अपि' । स्पष्टतः ये सभी धातुओं को सकर्मक मानते हैं, किन्तु दीक्षित, नागेशादि प्रथम दो को अकर्मक तथा पिछले दो को सकर्मक मानकर क्रमशः षष्ठी तथा कर्मसंज्ञा के अपवाद के रूप में इस सम्प्रदान का ग्रहण करते हैं। देखें-श० को० २, पृ० १२५।