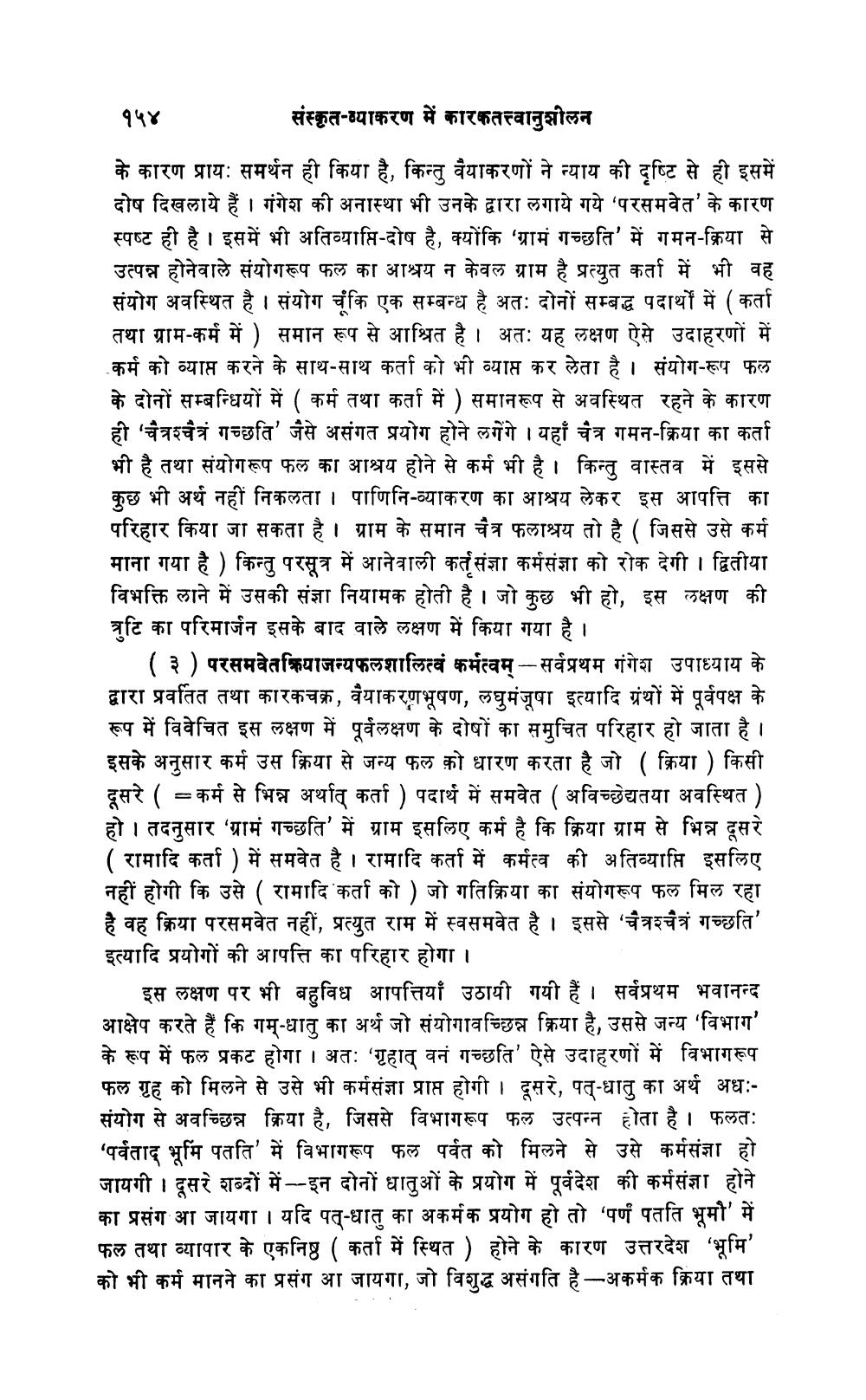________________
१५४
संस्कृत-व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन
के कारण प्रायः समर्थन ही किया है, किन्तु वैयाकरणों ने न्याय की दृष्टि से ही इसमें दोष दिखलाये हैं । गंगेश की अनास्था भी उनके द्वारा लगाये गये 'परसमवेत' के कारण स्पष्ट ही है। इसमें भी अतिव्याप्ति-दोष है, क्योंकि 'ग्रामं गच्छति' में गमन-क्रिया से उत्पन्न होनेवाले संयोगरूप फल का आश्रय न केवल ग्राम है प्रत्युत कर्ता में भी वह संयोग अवस्थित है । संयोग चूंकि एक सम्बन्ध है अत: दोनों सम्बद्ध पदार्थों में (कर्ता तथा ग्राम-कर्म में ) समान रूप से आश्रित है। अत: यह लक्षण ऐसे उदाहरणों में कर्म को व्याप्त करने के साथ-साथ कर्ता को भी व्याप्त कर लेता है। संयोग-रूप फल के दोनों सम्बन्धियों में ( कर्म तथा कर्ता में ) समानरूप से अवस्थित रहने के कारण ही 'चैत्रश्चत्रं गच्छति' जैसे असंगत प्रयोग होने लगेंगे । यहाँ चैत्र गमन-क्रिया का कर्ता भी है तथा संयोगरूप फल का आश्रय होने से कर्म भी है। किन्तु वास्तव में इससे कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। पाणिनि-व्याकरण का आश्रय लेकर इस आपत्ति का परिहार किया जा सकता है। ग्राम के समान चैत्र फलाश्रय तो है ( जिससे उसे कर्म माना गया है ) किन्तु परसूत्र में आनेवाली कर्तृ संज्ञा कर्मसंज्ञा को रोक देगी। द्वितीया विभक्ति लाने में उसकी संज्ञा नियामक होती है । जो कुछ भी हो, इस लक्षण की त्रुटि का परिमार्जन इसके बाद वाले लक्षण में किया गया है।
( ३ ) परसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वं कर्मत्वम् – सर्वप्रथम गंगेश उपाध्याय के द्वारा प्रवर्तित तथा कारकचक्र, वैयाकरणभूषण, लघुमंजूषा इत्यादि ग्रंथों में पूर्वपक्ष के रूप में विवेचित इस लक्षण में पूर्वलक्षण के दोषों का समुचित परिहार हो जाता है । इसके अनुसार कर्म उस क्रिया से जन्य फल को धारण करता है जो ( क्रिया ) किसी दूसरे ( = कर्म से भिन्न अर्थात् कर्ता ) पदार्थ में समवेत ( अविच्छेद्यतया अवस्थित ) हो । तदनुसार 'ग्रामं गच्छति' में ग्राम इसलिए कर्म है कि क्रिया ग्राम से भिन्न दूसरे ( रामादि कर्ता ) में समवेत है। रामादि कर्ता में कर्मत्व की अतिव्याप्ति इसलिए नहीं होगी कि उसे ( रामादि कर्ता को ) जो गतिक्रिया का संयोगरूप फल मिल रहा है वह क्रिया परसमवेत नहीं, प्रत्युत राम में स्वसमवेत है। इससे 'चैत्रश्चत्रं गच्छति' इत्यादि प्रयोगों की आपत्ति का परिहार होगा।
इस लक्षण पर भी बहुविध आपत्तियाँ उठायी गयी हैं। सर्वप्रथम भवानन्द आक्षेप करते हैं कि गम्-धातु का अर्थ जो संयोगावच्छिन्न क्रिया है, उससे जन्य 'विभाग' के रूप में फल प्रकट होगा । अत: 'गृहात् वनं गच्छति' ऐसे उदाहरणों में विभागरूप फल गृह को मिलने से उसे भी कर्मसंज्ञा प्राप्त होगी। दूसरे, पत्-धातु का अर्थ अधःसंयोग से अवच्छिन्न क्रिया है, जिससे विभागरूप फल उत्पन्न होता है। फलत: 'पर्वताद् भूमि पतति' में विभागरूप फल पर्वत को मिलने से उसे कर्मसंज्ञा हो जायगी। दूसरे शब्दों में --इन दोनों धातुओं के प्रयोग में पूर्वदेश की कर्मसंज्ञा होने का प्रसंग आ जायगा । यदि पत्-धातु का अकर्मक प्रयोग हो तो 'पणं पतति भूमौ' में फल तथा व्यापार के एकनिष्ठ ( कर्ता में स्थित ) होने के कारण उत्तरदेश 'भूमि' को भी कर्म मानने का प्रसंग आ जायगा, जो विशुद्ध असंगति है-अकर्मक क्रिया तथा