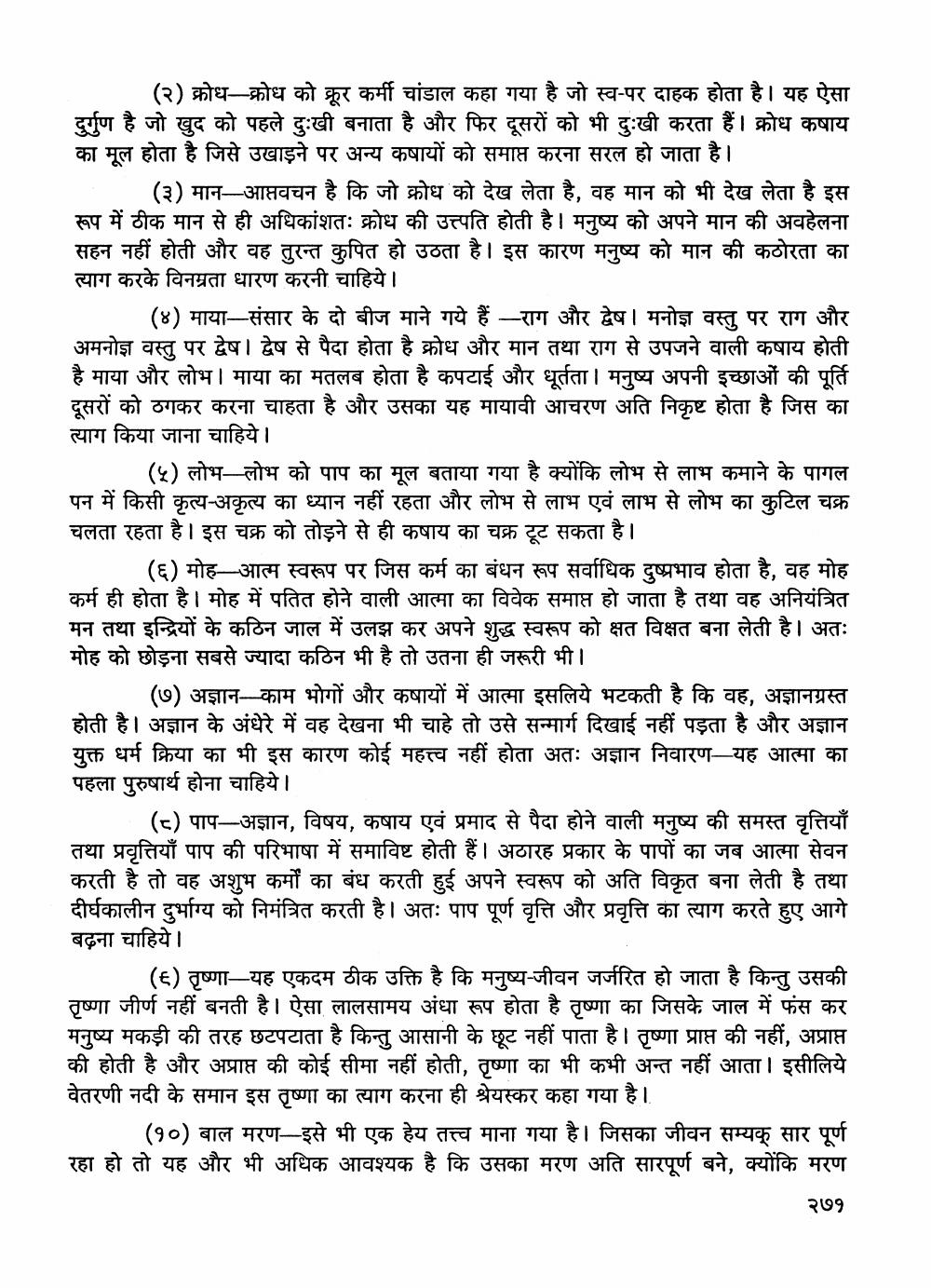________________
(२) क्रोध - क्रोध को क्रूर कर्मी चांडाल कहा गया है जो स्व-पर दाहक होता है। यह ऐसा दुर्गुण है जो खुद को पहले दुःखी बनाता है और फिर दूसरों को भी दुःखी करता हैं। क्रोध कषाय का मूल होता है जिसे उखाड़ने पर अन्य कषायों को समाप्त करना सरल हो जाता है।
(३) मान – आप्तवचन है कि जो क्रोध को देख लेता है, वह मान को भी देख लेता है इस रूप में ठीक मान से ही अधिकांशतः क्रोध की उत्त्पति होती है। मनुष्य को अपने मान की अवहेलना सहन नहीं होती और वह तुरन्त कुपित हो उठता है । इस कारण मनुष्य को मान की कठोरता का त्याग करके विनम्रता धारण करनी चाहिये ।
(४) माया – संसार के दो बीज माने गये हैं – राग और द्वेष । मनोज्ञ वस्तु पर राग और अमनोज्ञ वस्तु पर द्वेष। द्वेष से पैदा होता है क्रोध और मान तथा राग से उपजने वाली कषाय होती है माया और लोभ । माया का मतलब होता है कपटाई और धूर्तता । मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति दूसरों को ठगकर करना चाहता है और उसका यह मायावी आचरण अति निकृष्ट होता है जिस का त्याग किया जाना चाहिये ।
क्योंकि लोभ से लाभ कमाने के पागल लाभ एवं लाभ लोभ का कुटिल चक्र
(५) लोभ - लोभ को पाप का मूल बताया गया है पन में किसी कृत्य - अकृत्य का ध्यान नहीं रहता और लोभ चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ने से ही कषाय का चक्र टूट सकता है।
(६) मोह - आत्म स्वरूप पर जिस कर्म का बंधन रूप सर्वाधिक दुष्प्रभाव होता है, वह मोह कर्म ही होता है। मोह में पतित होने वाली आत्मा का विवेक समाप्त हो जाता है तथा वह अनियंत्रित मन तथा इन्द्रियों के कठिन जाल में उलझ कर अपने शुद्ध स्वरूप को क्षत विक्षत बना लेती है । अतः मोह को छोड़ना सबसे ज्यादा कठिन भी है तो उतना ही जरूरी भी ।
(७) अज्ञान - काम भोगों और कषायों में आत्मा इसलिये भटकती है कि वह, अज्ञानग्रस्त होती है। अज्ञान के अंधेरे में वह देखना भी चाहे तो उसे सन्मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है और अज्ञान युक्त धर्म क्रिया का भी इस कारण कोई महत्त्व नहीं होता अतः अज्ञान निवारण – यह आत्मा का पहला पुरुषार्थ होना चाहिये ।
(८) पाप – अज्ञान, विषय, कषाय एवं प्रमाद से पैदा होने वाली मनुष्य की समस्त वृत्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ पाप की परिभाषा में समाविष्ट होती हैं । अठारह प्रकार के पापों का जब आत्मा सेवन करती है तो वह अशुभ कर्मों का बंध करती हुई अपने स्वरूप को अति विकृत बना लेती है तथा दीर्घकालीन दुर्भाग्य को निमंत्रित करती है । अतः पाप पूर्ण वृत्ति और प्रवृत्ति का त्याग करते हुए आगे बढ़ना चाहिये ।
(६) तृष्णा - यह एकदम ठीक उक्ति है कि मनुष्य जीवन जर्जरित हो जाता है किन्तु उसकी तृष्णा जीर्ण नहीं बनती है। ऐसा लालसामय अंधा रूप होता है तृष्णा का जिसके जाल में फंस कर मनुष्य मकड़ी की तरह छटपटाता है किन्तु आसानी के छूट नहीं पाता है । तृष्णा प्राप्त की नहीं, अप्राप्त की होती है और अप्राप्त की कोई सीमा नहीं होती, तृष्णा का भी कभी अन्त नहीं आता । इसीलिये वेतरणी नदी के समान इस तृष्णा का त्याग करना ही श्रेयस्कर कहा गया है।
(१०) बाल मरण - इसे भी एक हेय तत्त्व माना गया है। जिसका जीवन सम्यक् सार पूर्ण रहा हो तो यह और भी अधिक आवश्यक है कि उसका मरण अति सारपूर्ण बने, क्योंकि मरण
२७१