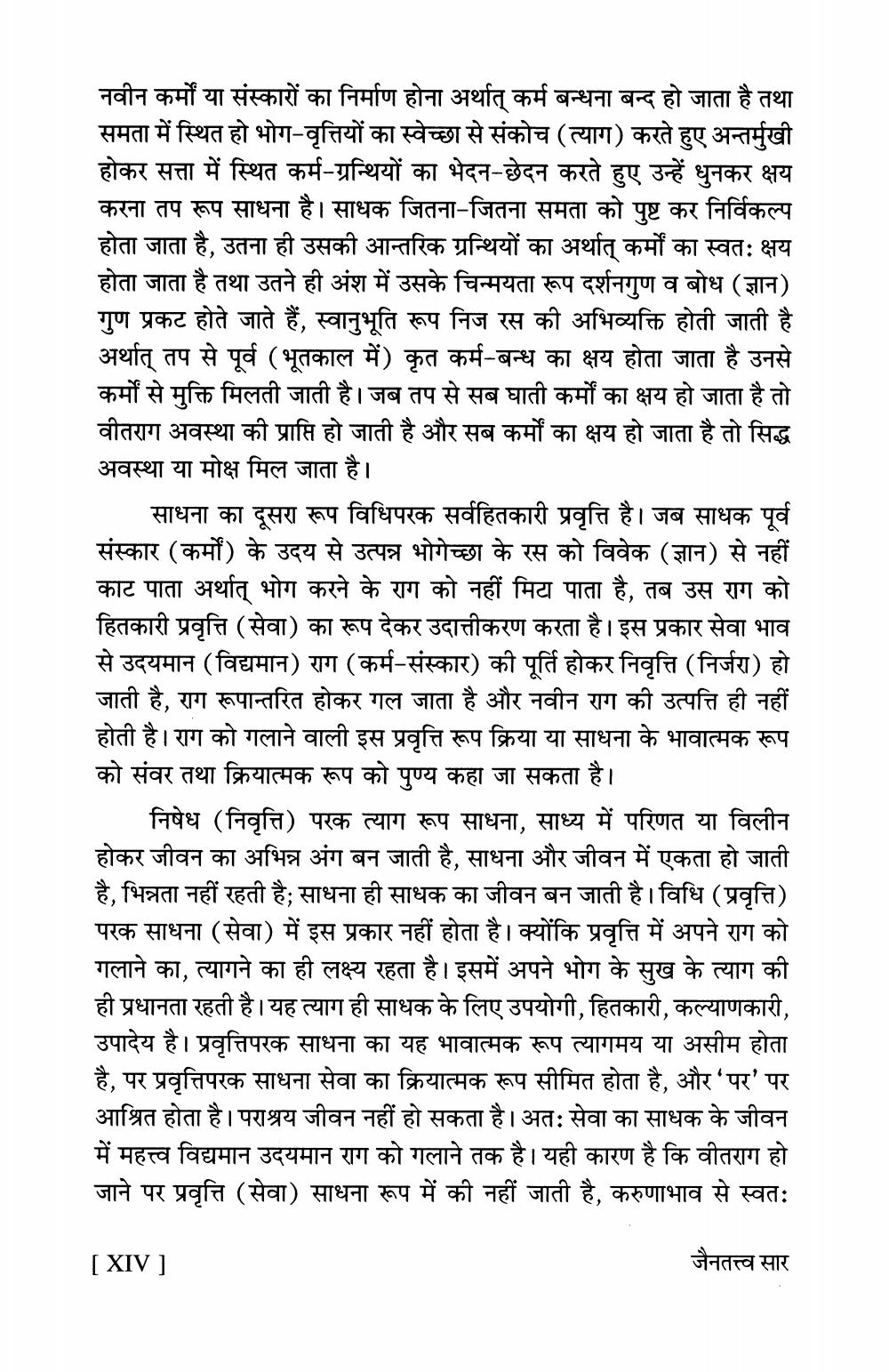________________
नवीन कर्मों या संस्कारों का निर्माण होना अर्थात् कर्म बन्धना बन्द हो जाता है तथा समता में स्थित हो भोग-वृत्तियों का स्वेच्छा से संकोच (त्याग) करते हुए अन्तर्मुखी होकर सत्ता में स्थित कर्म-ग्रन्थियों का भेदन-छेदन करते हुए उन्हें धुनकर क्षय करना तप रूप साधना है। साधक जितना-जितना समता को पुष्ट कर निर्विकल्प होता जाता है, उतना ही उसकी आन्तरिक ग्रन्थियों का अर्थात् कर्मों का स्वतः क्षय होता जाता है तथा उतने ही अंश में उसके चिन्मयता रूप दर्शनगुण व बोध (ज्ञान) गुण प्रकट होते जाते हैं, स्वानुभूति रूप निज रस की अभिव्यक्ति होती जाती है अर्थात् तप से पूर्व (भूतकाल में) कृत कर्म-बन्ध का क्षय होता जाता है उनसे कर्मों से मुक्ति मिलती जाती है। जब तप से सब घाती कर्मों का क्षय हो जाता है तो वीतराग अवस्था की प्राप्ति हो जाती है और सब कर्मों का क्षय हो जाता है तो सिद्ध अवस्था या मोक्ष मिल जाता है।
साधना का दूसरा रूप विधिपरक सर्वहितकारी प्रवृत्ति है। जब साधक पूर्व संस्कार (कर्मों) के उदय से उत्पन्न भोगेच्छा के रस को विवेक (ज्ञान) से नहीं काट पाता अर्थात् भोग करने के राग को नहीं मिटा पाता है, तब उस राग को हितकारी प्रवृत्ति (सेवा) का रूप देकर उदात्तीकरण करता है। इस प्रकार सेवा भाव से उदयमान (विद्यमान) राग (कर्म-संस्कार) की पूर्ति होकर निवृत्ति (निर्जरा) हो जाती है, राग रूपान्तरित होकर गल जाता है और नवीन राग की उत्पत्ति ही नहीं होती है। राग को गलाने वाली इस प्रवृत्ति रूप क्रिया या साधना के भावात्मक रूप को संवर तथा क्रियात्मक रूप को पुण्य कहा जा सकता है।
निषेध (निवृत्ति) परक त्याग रूप साधना, साध्य में परिणत या विलीन होकर जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है, साधना और जीवन में एकता हो जाती है, भिन्नता नहीं रहती है; साधना ही साधक का जीवन बन जाती है। विधि (प्रवृत्ति) परक साधना (सेवा) में इस प्रकार नहीं होता है। क्योंकि प्रवृत्ति में अपने राग को गलाने का, त्यागने का ही लक्ष्य रहता है। इसमें अपने भोग के सुख के त्याग की ही प्रधानता रहती है। यह त्याग ही साधक के लिए उपयोगी, हितकारी, कल्याणकारी, उपादेय है। प्रवृत्तिपरक साधना का यह भावात्मक रूप त्यागमय या असीम होता है, पर प्रवृत्तिपरक साधना सेवा का क्रियात्मक रूप सीमित होता है, और 'पर' पर आश्रित होता है। पराश्रय जीवन नहीं हो सकता है। अतः सेवा का साधक के जीवन में महत्त्व विद्यमान उदयमान राग को गलाने तक है। यही कारण है कि वीतराग हो जाने पर प्रवृत्ति (सेवा) साधना रूप में की नहीं जाती है, करुणाभाव से स्वतः
[XIV]
जैनतत्त्व सार