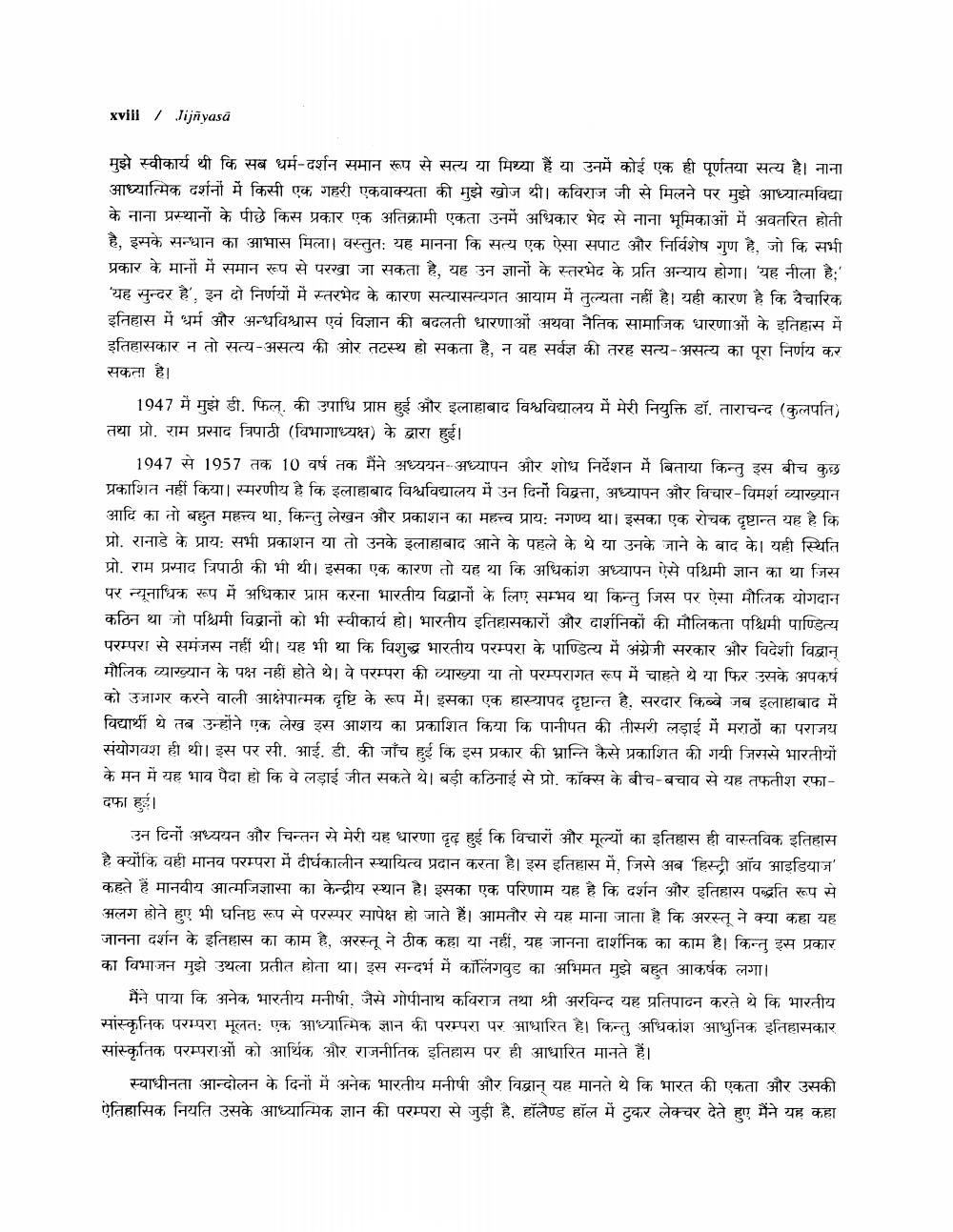________________
xvill / Jijñyasa
मुझे स्वीकार्य थी कि सब धर्म-दर्शन समान रूप से सत्य या मिथ्या हैं या उनमें कोई एक ही पूर्णतया सत्य है। नाना आध्यात्मिक दर्शनों में किसी एक गहरी एकवाक्यता की मुझे खोज थी। कविराज जी से मिलने पर मुझे आध्यात्मविद्या के नाना प्रस्थानों के पीछे किस प्रकार एक अतिक्रामी एकता उनमें अधिकार भेद से नाना भूमिकाओं में अवतरित होती है, इसके सन्धान का आभास मिला। वस्तुतः यह मानना कि सत्य एक ऐसा सपाट और निर्विशेष गुण है, जो कि सभी प्रकार के मानों में समान रूप से परखा जा सकता है, यह उन ज्ञानों के स्तरभेद के प्रति अन्याय होगा। 'यह नीला है; 'यह सुन्दर है, इन दो निर्णयों में स्तरभेद के कारण सत्यासत्यगत आयाम में तुल्यता नहीं है। यही कारण है कि वैचारिक इतिहास में धर्म और अन्धविश्वास एवं विज्ञान की बदलती धारणाओं अथवा नैतिक सामाजिक धारणाओं के इतिहास में इतिहासकार न तो सत्य-असत्य की ओर तटस्थ हो सकता है, न वह सर्वज्ञ की तरह सत्य-असत्य का पूरा निर्णय कर सकता है।
1947 में मुझे डी. फिल. की उपाधि प्राप्त हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति डॉ. ताराचन्द (कुलपति) तथा प्रो. राम प्रसाद त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष) के द्वारा हुई।
1947 से 1957 तक 10 वर्ष तक मैंने अध्ययन-अध्यापन और शोध निर्देशन में बिताया किन्तु इस बीच कुछ प्रकाशित नहीं किया। स्मरणीय है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन दिनों विद्वत्ता, अध्यापन और विचार-विमर्श व्याख्यान आदि का तो बहुत महत्त्व था, किन्तु लेखन और प्रकाशन का महत्त्व प्राय: नगण्य था। इसका एक रोचक दृष्टान्त यह है कि प्रो. रानाडे के प्राय: सभी प्रकाशन या तो उनके इलाहाबाद आने के पहले के थे या उनके जाने के बाद के। यही स्थिति प्रो. राम प्रसाद त्रिपाठी की भी थी। इसका एक कारण तो यह था कि अधिकांश अध्यापन ऐसे पश्चिमी ज्ञान का था जिस पर न्यूनाधिक रूप में अधिकार प्राप्त करना भारतीय विद्वानों के लिए सम्भव था किन्तु जिस पर ऐसा मौलिक योगदान कठिन था जो पश्चिमी विद्वानों को भी स्वीकार्य हो। भारतीय इतिहासकारों और दार्शनिकों की मौलिकता पश्चिमी पाण्डित्य परम्परा से समंजस नहीं थी। यह भी था कि विशुद्ध भारतीय परम्परा के पाण्डित्य में अंग्रेजी सरकार और विदेशी विद्वान् मौलिक व्याख्यान के पक्ष नहीं होते थे। वे परम्परा की व्याख्या या तो परम्परागत रूप में चाहते थे या फिर उसके अपकर्ष को उजागर करने वाली आक्षेपात्मक दृष्टि के रूप में। इसका एक हास्यापद दृष्टान्त है, सरदार किब्वे जब इलाहाबाद में विद्यार्थी थे तब उन्होंने एक लेख इस आशय का प्रकाशित किया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का पराजय संयोगवश ही थी। इस पर सी. आई. डी. की जाँच हुई कि इस प्रकार की भ्रान्ति कैसे प्रकाशित की गयी जिससे भारतीयों के मन में यह भाव पैदा हो कि वे लड़ाई जीत सकते थे। बड़ी कठिनाई से प्रो. कॉक्स के बीच-बचाव से यह तफतीश रफादफा हुई।
उन दिनों अध्ययन और चिन्तन से मेरी यह धारणा दृढ़ हुई कि विचारों और मूल्यों का इतिहास ही वास्तविक इतिहास है क्योंकि वही मानव परम्परा में दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान करता है। इस इतिहास में, जिसे अब 'हिस्ट्री ऑव आइडियाज' कहते हैं मानवीय आत्मजिज्ञासा का केन्द्रीय स्थान है। इसका एक परिणाम यह है कि दर्शन और इतिहास पद्धति रूप से अलग होते हुए भी घनिष्ठ रूप से परस्पर सापेक्ष हो जाते हैं। आमतौर से यह माना जाता है कि अरस्तू ने क्या कहा यह जानना दर्शन के इतिहास का काम है, अरस्तू ने ठीक कहा या नहीं, यह जानना दार्शनिक का काम है। किन्तु इस प्रकार का विभाजन मुझे उथला प्रतीत होता था। इस सन्दर्भ में कॉलिंगवुड का अभिमत मुझे बहुत आकर्षक लगा।
मैंने पाया कि अनेक भारतीय मनीषी, जैसे गोपीनाथ कविराज तथा श्री अरविन्द यह प्रतिपादन करते थे कि भारतीय सांस्कृतिक परम्परा मूलतः एक आध्यात्मिक ज्ञान की परम्परा पर आधारित है। किन्तु अधिकांश आधुनिक इतिहासकार सांस्कृतिक परम्पराओं को आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पर ही आधारित मानते हैं।
स्वाधीनता आन्दोलन के दिनों में अनेक भारतीय मनीषी और विद्वान् यह मानते थे कि भारत की एकता और उसकी ऐतिहासिक नियति उसके आध्यात्मिक ज्ञान की परम्परा से जुड़ी है, हॉलैण्ड हॉल में टुकर लेक्चर देते हुए मैंने यह कहा