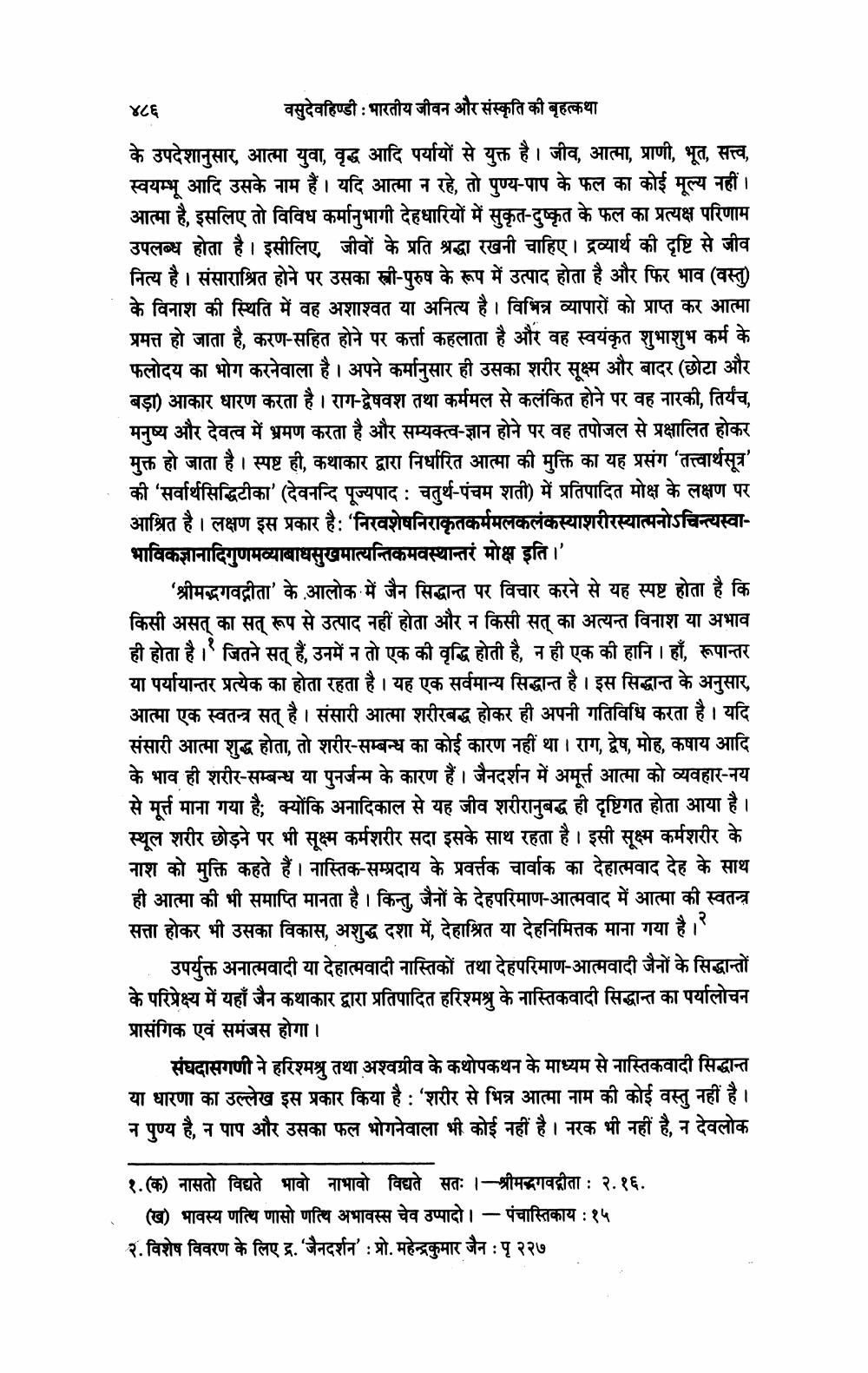________________
४८६
वसुदेवहिण्डी:भारतीय जीवन और संस्कृति की बहत्कथा के उपदेशानुसार, आत्मा युवा, वृद्ध आदि पर्यायों से युक्त है। जीव, आत्मा, प्राणी, भूत, सत्त्व, स्वयम्भू आदि उसके नाम हैं। यदि आत्मा न रहे, तो पुण्य-पाप के फल का कोई मूल्य नहीं। आत्मा है, इसलिए तो विविध कर्मानुभागी देहधारियों में सुकृत-दुष्कृत के फल का प्रत्यक्ष परिणाम उपलब्ध होता है। इसीलिए, जीवों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। द्रव्यार्थ की दृष्टि से जीव नित्य है। संसाराश्रित होने पर उसका स्त्री-पुरुष के रूप में उत्पाद होता है और फिर भाव (वस्तु) के विनाश की स्थिति में वह अशाश्वत या अनित्य है। विभिन्न व्यापारों को प्राप्त कर आत्मा प्रमत्त हो जाता है, करण-सहित होने पर कर्ता कहलाता है और वह स्वयंकृत शुभाशुभ कर्म के फलोदय का भोग करनेवाला है। अपने कर्मानुसार ही उसका शरीर सूक्ष्म और बादर (छोटा और बड़ा) आकार धारण करता है। राग-द्वेषवश तथा कर्ममल से कलंकित होने पर वह नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवत्व में भ्रमण करता है और सम्यक्त्व-ज्ञान होने पर वह तपोजल से प्रक्षालित होकर मुक्त हो जाता है। स्पष्ट ही, कथाकार द्वारा निर्धारित आत्मा की मुक्ति का यह प्रसंग 'तत्त्वार्थसूत्र' की ‘सर्वार्थसिद्धिटीका' (देवनन्दि पूज्यपाद : चतुर्थ-पंचम शती) में प्रतिपादित मोक्ष के लक्षण पर आश्रित है । लक्षण इस प्रकार है: 'निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलंकस्याशरीरस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुणमव्याबाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति।' ___'श्रीमद्भगवद्गीता' के आलोक में जैन सिद्धान्त पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि किसी असत् का सत् रूप से उत्पाद नहीं होता और न किसी सत् का अत्यन्त विनाश या अभाव ही होता है। जितने सत् हैं, उनमें न तो एक की वृद्धि होती है, न ही एक की हानि । हाँ, रूपान्तर या पर्यायान्तर प्रत्येक का होता रहता है । यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के अनुसार, आत्मा एक स्वतन्त्र सत् है । संसारी आत्मा शरीरबद्ध होकर ही अपनी गतिविधि करता है। यदि संसारी आत्मा शुद्ध होता, तो शरीर-सम्बन्ध का कोई कारण नहीं था। राग, द्वेष, मोह, कषाय आदि के भाव ही शरीर-सम्बन्ध या पुनर्जन्म के कारण हैं। जैनदर्शन में अमूर्त आत्मा को व्यवहार-नय से मूर्त माना गया है; क्योंकि अनादिकाल से यह जीव शरीरानुबद्ध ही दृष्टिगत होता आया है। स्थूल शरीर छोड़ने पर भी सूक्ष्म कर्मशरीर सदा इसके साथ रहता है। इसी सूक्ष्म कर्मशरीर के नाश को मुक्ति कहते हैं। नास्तिक-सम्प्रदाय के प्रवर्तक चार्वाक का देहात्मवाद देह के साथ ही आत्मा की भी समाप्ति मानता है। किन्तु, जैनों के देहपरिमाण-आत्मवाद में आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता होकर भी उसका विकास, अशुद्ध दशा में, देहाश्रित या देहनिमित्तक माना गया है। ___उपर्युक्त अनात्मवादी या देहात्मवादी नास्तिकों तथा देहपरिमाण-आत्मवादी जैनों के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ जैन कथाकार द्वारा प्रतिपादित हरिश्मश्रु के नास्तिकवादी सिद्धान्त का पर्यालोचन प्रासंगिक एवं समंजस होगा।
संघदासगणी ने हरिश्मश्रु तथा अश्वग्रीव के कथोपकथन के माध्यम से नास्तिकवादी सिद्धान्त या धारणा का उल्लेख इस प्रकार किया है : 'शरीर से भिन्न आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। न पुण्य है, न पाप और उसका फल भोगनेवाला भी कोई नहीं है। नरक भी नहीं है, न देवलोक
१.(क) नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । श्रीमद्भगवद्गीता : २.१६.
(ख) भावस्य णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो। - पंचास्तिकाय : १५ २. विशेष विवरण के लिए द्र. जैनदर्शन' : प्रो. महेन्द्रकुमार जैन : पृ २२७