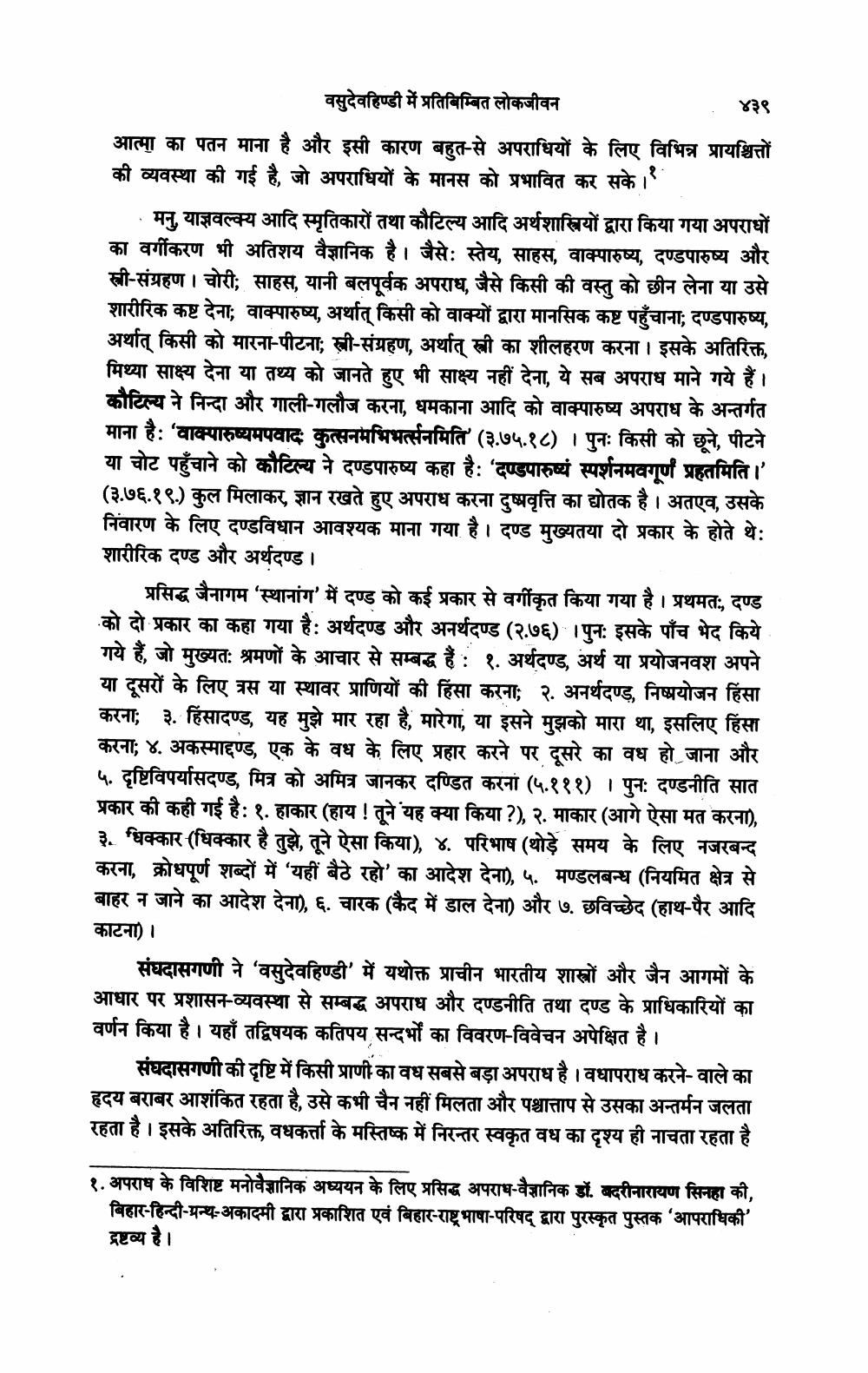________________
वसुदेवहिण्डी में प्रतिबिम्बित लोकजीवन
४३९ आत्मा का पतन माना है और इसी कारण बहुत-से अपराधियों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की गई है, जो अपराधियों के मानस को प्रभावित कर सके।
. मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारों तथा कौटिल्य आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया अपराधों का वर्गीकरण भी अतिशय वैज्ञानिक है। जैसेः स्तेय, साहस, वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य और स्त्री-संग्रहण । चोरी; साहस, यानी बलपूर्वक अपराध, जैसे किसी की वस्तु को छीन लेना या उसे शारीरिक कष्ट देना; वाक्पारुष्य, अर्थात् किसी को वाक्यों द्वारा मानसिक कष्ट पहुँचाना; दण्डपारुष्य, अर्थात् किसी को मारना-पीटना; स्त्री-संग्रहण, अर्थात् स्त्री का शीलहरण करना। इसके अतिरिक्त, मिथ्या साक्ष्य देना या तथ्य को जानते हुए भी साक्ष्य नहीं देना, ये सब अपराध माने गये हैं। कौटिल्य ने निन्दा और गाली-गलौज करना, धमकाना आदि को वाक्पारुष्य अपराध के अन्तर्गत माना है: 'वाक्पारुष्यमपवादः कुत्सनमभिभर्त्सनमिति' (३.७५.१८) । पुनः किसी को छूने, पीटने या चोट पहुँचाने को कौटिल्य ने दण्डपारुष्य कहा है: 'दण्डपारुष्यं स्पर्शनमवगूर्ण प्रहतमिति।' (३.७६.१९.) कुल मिलाकर, ज्ञान रखते हुए अपराध करना दुष्प्रवृत्ति का द्योतक है। अतएव, उसके निवारण के लिए दण्डविधान आवश्यक माना गया है। दण्ड मुख्यतया दो प्रकार के होते थे: शारीरिक दण्ड और अर्थदण्ड।
प्रसिद्ध जैनागम 'स्थानांग' में दण्ड को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। प्रथमतः दण्ड को दो प्रकार का कहा गया है: अर्थदण्ड और अनर्थदण्ड (२.७६) । पुन: इसके पाँच भेद किये गये हैं, जो मुख्यत: श्रमणों के आचार से सम्बद्ध हैं : १. अर्थदण्ड, अर्थ या प्रयोजनवश अपने या दूसरों के लिए त्रस या स्थावर प्राणियों की हिंसा करना; २. अनर्थदण्ड, निष्षयोजन हिंसा करना; ३. हिंसादण्ड, यह मुझे मार रहा है, मारेगा, या इसने मुझको मारा था, इसलिए हिंसा करना; ४. अकस्माद्दण्ड, एक के वध के लिए प्रहार करने पर दूसरे का वध हो जाना और ५. दृष्टिविपर्यासदण्ड, मित्र को अमित्र जानकर दण्डित करना (५.१११) । पुन: दण्डनीति सात प्रकार की कही गई है: १. हाकार (हाय ! तूने यह क्या किया?), २. माकार (आगे ऐसा मत करना), ३. धिक्कार (धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया), ४. परिभाष (थोड़े समय के लिए नजरबन्द करना, क्रोधपूर्ण शब्दों में 'यहीं बैठे रहो' का आदेश देना), ५. मण्डलबन्ध (नियमित क्षेत्र से बाहर न जाने का आदेश देना), ६. चारक (कैद में डाल देना) और ७. छविच्छेद (हाथ-पैर आदि काटना)।
संघदासगणी ने 'वसुदेवहिण्डी' में यथोक्त प्राचीन भारतीय शास्त्रों और जैन आगमों के आधार पर प्रशासन-व्यवस्था से सम्बद्ध अपराध और दण्डनीति तथा दण्ड के प्राधिकारियों का वर्णन किया है। यहाँ तद्विषयक कतिपय सन्दर्भो का विवरण-विवेचन अपेक्षित है।
संघदासगणी की दृष्टि में किसी प्राणी का वधसबसे बड़ा अपराध है । वधापराध करने वाले का हृदय बराबर आशंकित रहता है, उसे कभी चैन नहीं मिलता और पश्चात्ताप से उसका अन्तर्मन जलता रहता है । इसके अतिरिक्त, वधकर्ता के मस्तिष्क में निरन्तर स्वकृत वध का दृश्य ही नाचता रहता है
१. अपराध के विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रसिद्ध अपराध-वैज्ञानिक डॉ. बदरीनारायण सिनहा की, बिहार-हिन्दी-ग्रन्थ-अकादमी द्वारा प्रकाशित एवं बिहार-राष्ट्र भाषा-परिषद् द्वारा पुरस्कृत पुस्तक 'आपराधिकी' द्रष्टव्य है।