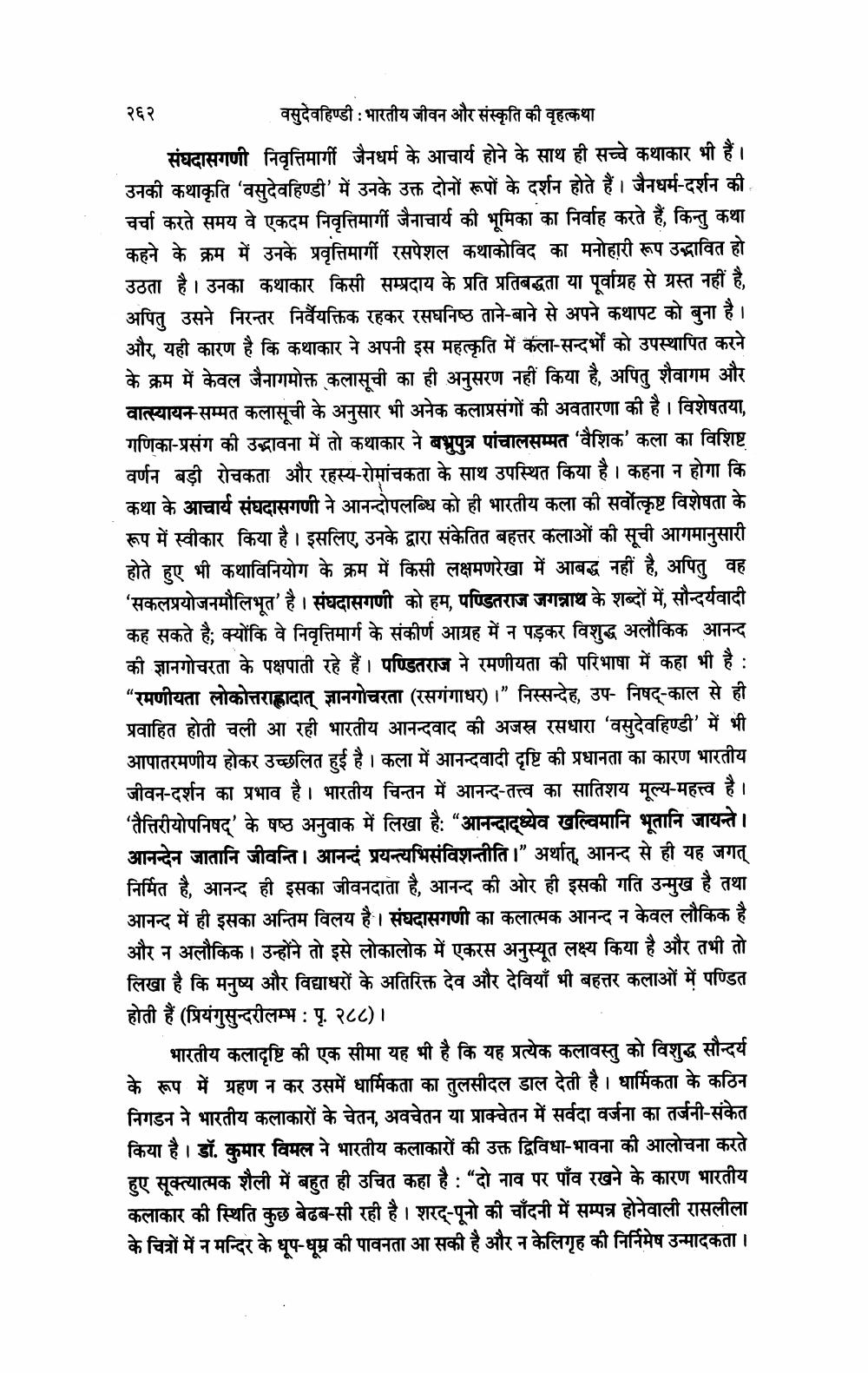________________
२६२
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की वृहत्कथा संघदासगणी निवृत्तिमार्गी जैनधर्म के आचार्य होने के साथ ही सच्चे कथाकार भी हैं। उनकी कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी' में उनके उक्त दोनों रूपों के दर्शन होते हैं। जैनधर्म-दर्शन की चर्चा करते समय वे एकदम निवृत्तिमार्गी जैनाचार्य की भूमिका का निर्वाह करते हैं, किन्तु कथा कहने के क्रम में उनके प्रवृत्तिमार्गी रसपेशल कथाकोविद का मनोहारी रूप उद्भावित हो उठता है। उनका कथाकार किसी सम्प्रदाय के प्रति प्रतिबद्धता या पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, अपितु उसने निरन्तर निर्वैयक्तिक रहकर रसघनिष्ठ ताने-बाने से अपने कथापट को बुना है। और, यही कारण है कि कथाकार ने अपनी इस महत्कृति में कला-सन्दर्भो को उपस्थापित करने के क्रम में केवल जैनागमोक्त कलासूची का ही अनुसरण नहीं किया है, अपितु शैवागम और वात्स्यायन-सम्मत कलासूची के अनुसार भी अनेक कलाप्रसंगों की अवतारणा की है। विशेषतया, गणिका-प्रसंग की उद्भावना में तो कथाकार ने बभ्रुपुत्र पांचालसम्मत 'वैशिक' कला का विशिष्ट वर्णन बड़ी रोचकता और रहस्य-रोमांचकता के साथ उपस्थित किया है। कहना न होगा कि कथा के आचार्य संघदासगणी ने आनन्दोपलब्धि को ही भारतीय कला की सर्वोत्कृष्ट विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए, उनके द्वारा संकेतित बहत्तर कलाओं की सूची आगमानुसारी होते हुए भी कथाविनियोग के क्रम में किसी लक्षमणरेखा में आबद्ध नहीं है, अपितु वह 'सकलप्रयोजनमौलिभूत' है। संघदासगणी को हम, पण्डितराज जगन्नाथ के शब्दों में, सौन्दर्यवादी कह सकते है; क्योंकि वे निवत्तिमार्ग के संकीर्ण आग्रह में न पडकर विशद्ध अलौकिक आनन्द की ज्ञानगोचरता के पक्षपाती रहे हैं। पण्डितराज ने रमणीयता की परिभाषा में कहा भी है : "रमणीयता लोकोत्तराहादात् ज्ञानगोचरता (रसगंगाधर)।” निस्सन्देह, उप- निषद्-काल से ही प्रवाहित होती चली आ रही भारतीय आनन्दवाद की अजस्र रसधारा 'वसुदेवहिण्डी' में भी आपातरमणीय होकर उच्छलित हुई है। कला में आनन्दवादी दृष्टि की प्रधानता का कारण भारतीय जीवन-दर्शन का प्रभाव है। भारतीय चिन्तन में आनन्द-तत्त्व का सातिशय मूल्य-महत्त्व है। 'तैत्तिरीयोपनिषद्' के षष्ठ अनुवाक में लिखा है: “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते।
आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति।" अर्थात्, आनन्द से ही यह जगत् निर्मित है, आनन्द ही इसका जीवनदाता है, आनन्द की ओर ही इसकी गति उन्मुख है तथा आनन्द में ही इसका अन्तिम विलय है। संघदासगणी का कलात्मक आनन्द न केवल लौकिक है और न अलौकिक । उन्होंने तो इसे लोकालोक में एकरस अनुस्यूत लक्ष्य किया है और तभी तो लिखा है कि मनुष्य और विद्याधरों के अतिरिक्त देव और देवियाँ भी बहत्तर कलाओं में पण्डित होती हैं (प्रियंगुसुन्दरीलम्भ : पृ. २८८)।
भारतीय कलादृष्टि की एक सीमा यह भी है कि यह प्रत्येक कलावस्तु को विशुद्ध सौन्दर्य के रूप में ग्रहण न कर उसमें धार्मिकता का तुलसीदल डाल देती है। धार्मिकता के कठिन निगडन ने भारतीय कलाकारों के चेतन, अवचेतन या प्राक्चेतन में सर्वदा वर्जना का तर्जनी-संकेत किया है। डॉ. कुमार विमल ने भारतीय कलाकारों की उक्त द्विविधा-भावना की आलोचना करते हुए सूक्त्यात्मक शैली में बहुत ही उचित कहा है : “दो नाव पर पाँव रखने के कारण भारतीय कलाकार की स्थिति कुछ बेढब-सी रही है। शरद्-पूनो की चाँदनी में सम्पन्न होनेवाली रासलीला के चित्रों में न मन्दिर के धूप-धूम्र की पावनता आ सकी है और न केलिगृह की निर्निमेष उन्मादकता।