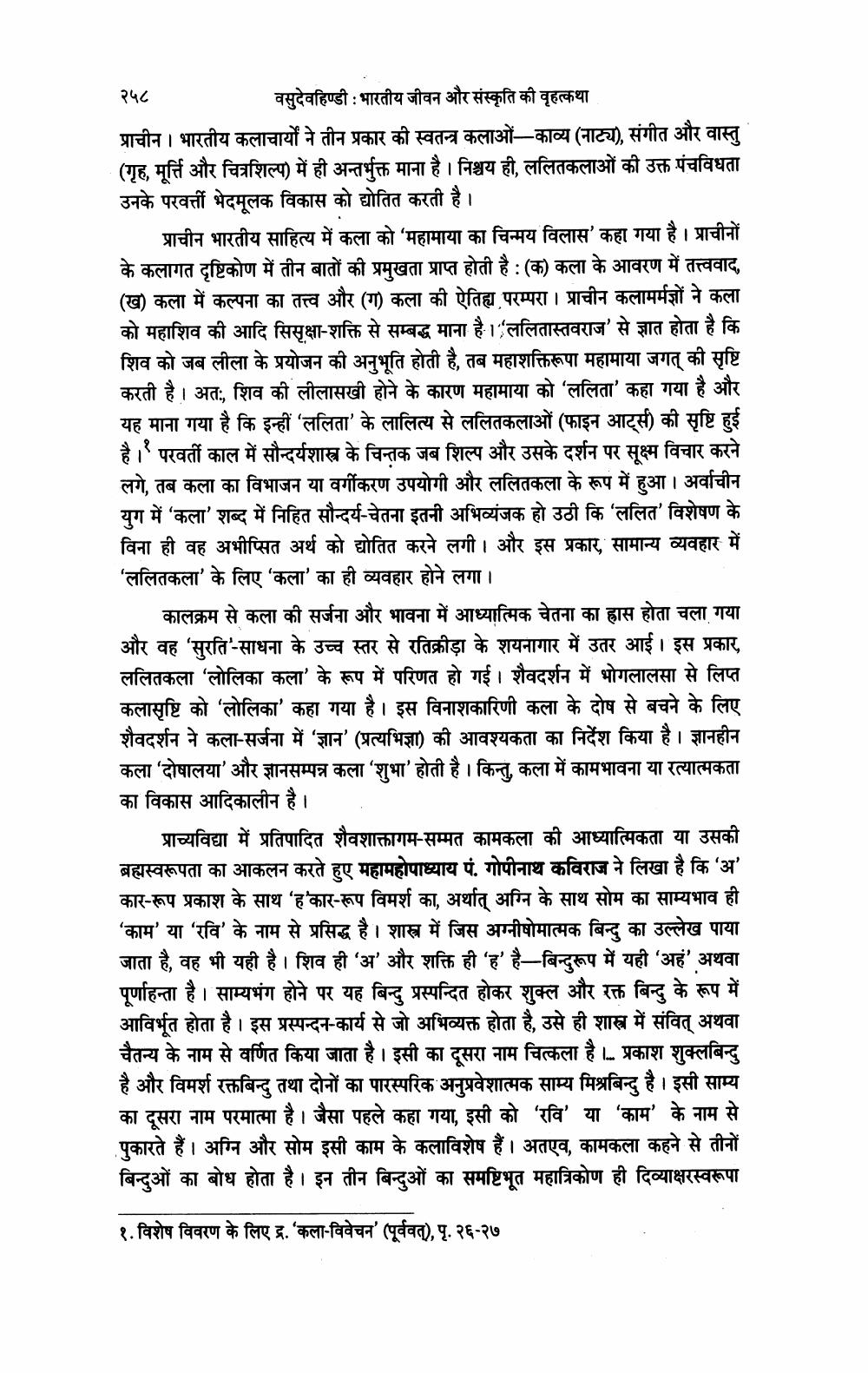________________
२५८
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की वृहत्कथा
प्राचीन । भारतीय कलाचार्यों ने तीन प्रकार की स्वतन्त्र कलाओं-काव्य (नाट्य), संगीत और वास्तु (गृह, मूर्ति और चित्रशिल्प) में ही अन्तर्भुक्त माना है । निश्चय ही, ललितकलाओं की उक्त पंचविधता उनके परवर्त्ती भेदमूलक विकास को द्योतित करती है
1
1
प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को 'महामाया का चिन्मय विलास' कहा गया है। प्राचीनों लागत दृष्टिकोण में तीन बातों की प्रमुखता प्राप्त होती है : (क) कला के आवरण में तत्त्ववाद, (ख) कला में कल्पना का तत्त्व और (ग) कला की ऐतिह्य परम्परा । प्राचीन कलामर्मज्ञों ने कला को महाशिव की आदि सिसृक्षा-शक्ति से सम्बद्ध माना है । 'ललितास्तवराज' से ज्ञात होता है कि शिव को जब लीला के प्रयोजन की अनुभूति होती है, तब महाशक्तिरूपा महामाया जगत् की सृष्टि करती है । अतः, शिव की लीलासखी होने के कारण महामाया को 'ललिता' कहा गया है और यह माना गया है कि इन्हीं 'ललिता' के लालित्य से ललितकलाओं (फाइन आर्ट्स) की सृष्टि हुई है ।' परवर्ती काल में सौन्दर्यशास्त्र के चिन्तक जब शिल्प और उसके दर्शन पर सूक्ष्म विचार करने लगे, तब कला का विभाजन या वर्गीकरण उपयोगी और ललितकला के रूप में हुआ । अर्वाचीन युग में 'कला' शब्द में निहित सौन्दर्य चेतना इतनी अभिव्यंजक हो उठी कि 'ललित' विशेषण के विना ही वह अभीप्सित अर्थ को द्योतित करने लगी। और इस प्रकार, सामान्य व्यवहार में 'ललितकला' के लिए 'कला' का ही व्यवहार होने लगा ।
कालक्रम से कला की सर्जना और भावना में आध्यात्मिक चेतना का ह्रास होता चला गया और वह 'सुरति - साधना के उच्च स्तर से रतिक्रीड़ा के शयनागार में उतर आई। इस प्रकार, ललितकला 'लोलिका कला' के रूप में परिणत हो गई। शैवदर्शन में भोगलालसा से लिप्त कलासृष्टि को 'लोलिका' कहा गया है। इस विनाशकारिणी कला के दोष से बचने के लिए शैवदर्शन ने कला-सर्जना में 'ज्ञान' (प्रत्यभिज्ञा) की आवश्यकता का निर्देश किया है। ज्ञानहीन कला 'दोषालया' और ज्ञानसम्पन्न कला 'शुभा' होती है । किन्तु, कला में कामभावना या रत्यात्मकता का विकास आदिकालीन है ।
प्राच्यविद्या में प्रतिपादित शैवशाक्तागम-सम्मत कामकला की आध्यात्मिकता या उसकी ब्रह्मस्वरूपता का आकलन करते हुए महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ कविराज ने लिखा है कि 'अ' कार-रूप प्रकाश के साथ 'ह' कार - रूप विमर्श का, अर्थात् अग्नि के साथ सोम का साम्यभाव ही 'काम' या 'रवि' के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्र में जिस अग्नीषोमात्मक बिन्दु का उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है। शिव ही 'अ' और शक्ति ही 'ह' है - बिन्दुरूप में यही 'अहं' अथवा पूर्णाहता है । साम्यभंग होने पर यह बिन्दु प्रस्पन्दित होकर शुक्ल और रक्त बिन्दु के रूप में आविर्भूत होता है । इस प्रस्पन्दन - कार्य से जो अभिव्यक्त होता है, उसे ही शास्त्र में संवित् अथवा चैतन्य के नाम से वर्णित किया जाता है। इसी का दूसरा नाम चित्कला है।.. प्रकाश शुक्लबिन्दु है और विमर्श रक्तबिन्दु तथा दोनों का पारस्परिक अनुप्रवेशात्मक साम्य मिश्रबिन्दु है । इसी साम्य का दूसरा नाम परमात्मा है। जैसा पहले कहा गया, इसी को 'रवि' या 'काम' के नाम से पुकारते हैं। अग्नि और सोम इसी काम के कलाविशेष हैं। अतएव, कामकला कहने से तीनों बिन्दुओं का बोध होता है। इन तीन बिन्दुओं का समष्टिभूत महात्रिकोण ही दिव्याक्षरस्वरूपा
१. विशेष विवरण के लिए द्र. 'कला-विवेचन' (पूर्ववत्, पृ. २६-२७