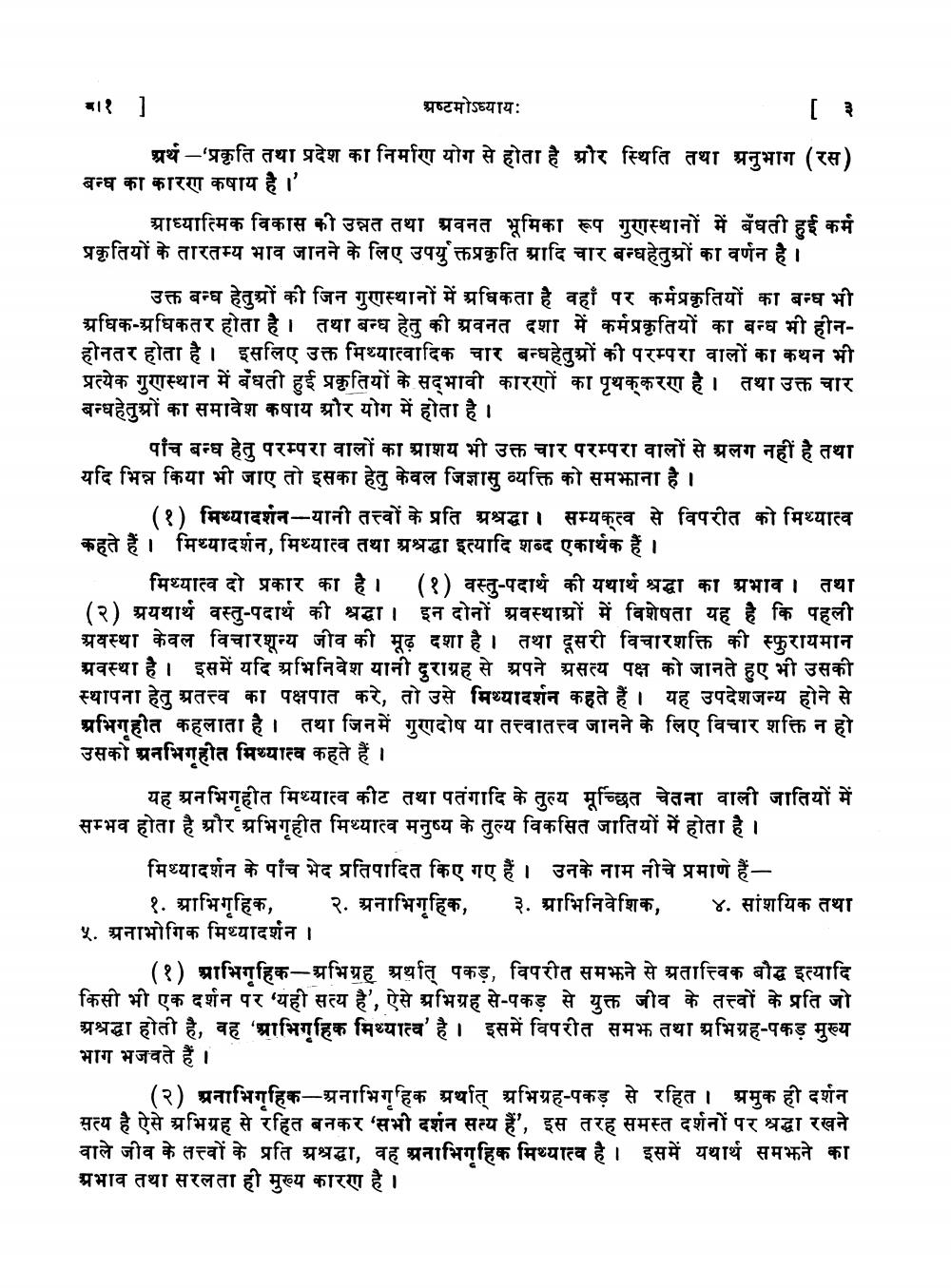________________
बा१ ]
अष्टमोऽध्यायः अर्थ –'प्रकृति तथा प्रदेश का निर्माण योग से होता है और स्थिति तथा अनुभाग (रस) बन्ध का कारण कषाय है।'
आध्यात्मिक विकास की उन्नत तथा अवनत भूमिका रूप गुणस्थानों में बँधती हुई कर्म प्रकृतियों के तारतम्य भाव जानने के लिए उपयुक्तप्रकृति आदि चार बन्धहेतुओं का वर्णन है।
उक्त बन्ध हेतुत्रों की जिन गुणस्थानों में अधिकता है वहाँ पर कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी अधिक-अधिकतर होता है। तथा बन्ध हेतु की अवनत दशा में कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी हीनहोनतर होता है। इसलिए उक्त मिथ्यात्वादिक चार बन्धहेतुओं की परम्परा वालों का कथन भी प्रत्येक गुणस्थान में बंधती हुई प्रकृतियों के सद्भावी कारणों का पृथक्करण है। तथा उक्त चार बन्धहेतुओं का समावेश कषाय और योग में होता है।
पांच बन्ध हेतु परम्परा वालों का आशय भी उक्त चार परम्परा वालों से अलग नहीं है तथा यदि भिन्न किया भी जाए तो इसका हेतु केवल जिज्ञासु व्यक्ति को समझाना है।
(१) मिथ्यादर्शन-यानी तत्त्वों के प्रति अश्रद्धा। सम्यक्त्व से विपरीत को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यादर्शन, मिथ्यात्व तथा अश्रद्धा इत्यादि शब्द एकार्थक हैं।
मिथ्यात्व दो प्रकार का है। (१) वस्तु-पदार्थ की यथार्थ श्रद्धा का अभाव । तथा (२) अयथार्थ वस्तु-पदार्थ की श्रद्धा। इन दोनों अवस्थाओं में विशेषता यह है कि पहली अवस्था केवल विचारशून्य जीव की मूढ़ दशा है। तथा दूसरी विचारशक्ति की स्फुरायमान अवस्था है। इसमें यदि अभिनिवेश यानी दुराग्रह से अपने असत्य पक्ष को जानते हुए भी उसकी स्थापना हेतु प्रतत्त्व का पक्षपात करे, तो उसे मिथ्यादर्शन कहते हैं। यह उपदेशजन्य होने से अभिग्रहीत कहलाता है। तथा जिनमें गुणदोष या तत्त्वातत्त्व जानने के लिए विचार शक्ति न हो उसको अनभिगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं ।
यह अनभिगृहीत मिथ्यात्व कीट तथा पतंगादि के तुल्य मूच्छित चेतना वाली जातियों में सम्भव होता है और अभिगृहीत मिथ्यात्व मनुष्य के तुल्य विकसित जातियों में होता है ।
मिथ्यादर्शन के पांच भेद प्रतिपादित किए गए हैं। उनके नाम नीचे प्रमाणे हैं
१. आभिगृहिक, २. अनाभिगृहिक, ३. आभिनिवेशिक, ४. सांशयिक तथा ५. अनाभोगिक मिथ्यादर्शन ।
(१) प्राभिगहिक-अभिग्रह अर्थात् पकड़, विपरीत समझने से अतात्त्विक बौद्ध इत्यादि किसी भी एक दर्शन पर 'यही सत्य है', ऐसे अभिग्रह से-पकड़ से युक्त जीव के तत्त्वों के प्रति जो अश्रद्धा होती है, वह 'पाभिगृहिक मिथ्यात्व' है। इसमें विपरीत समझ तथा अभिग्रह-पकड़ मुख्य भाग भजवते हैं।
(२) अनाभिगृहिक-अनाभिगृहिक अर्थात् अभिग्रह-पकड़ से रहित । अमुक ही दर्शन सत्य है ऐसे अभिग्रह से रहित बनकर सभी दर्शन सत्य हैं', इस तरह समस्त दर्शनों पर श्रद्धा रखने वाले जीव के तत्त्वों के प्रति प्रश्रद्धा, वह अनाभिगहिक मिथ्यात्व है। इसमें यथार्थ समझने का प्रभाव तथा सरलता ही मुख्य कारण है।