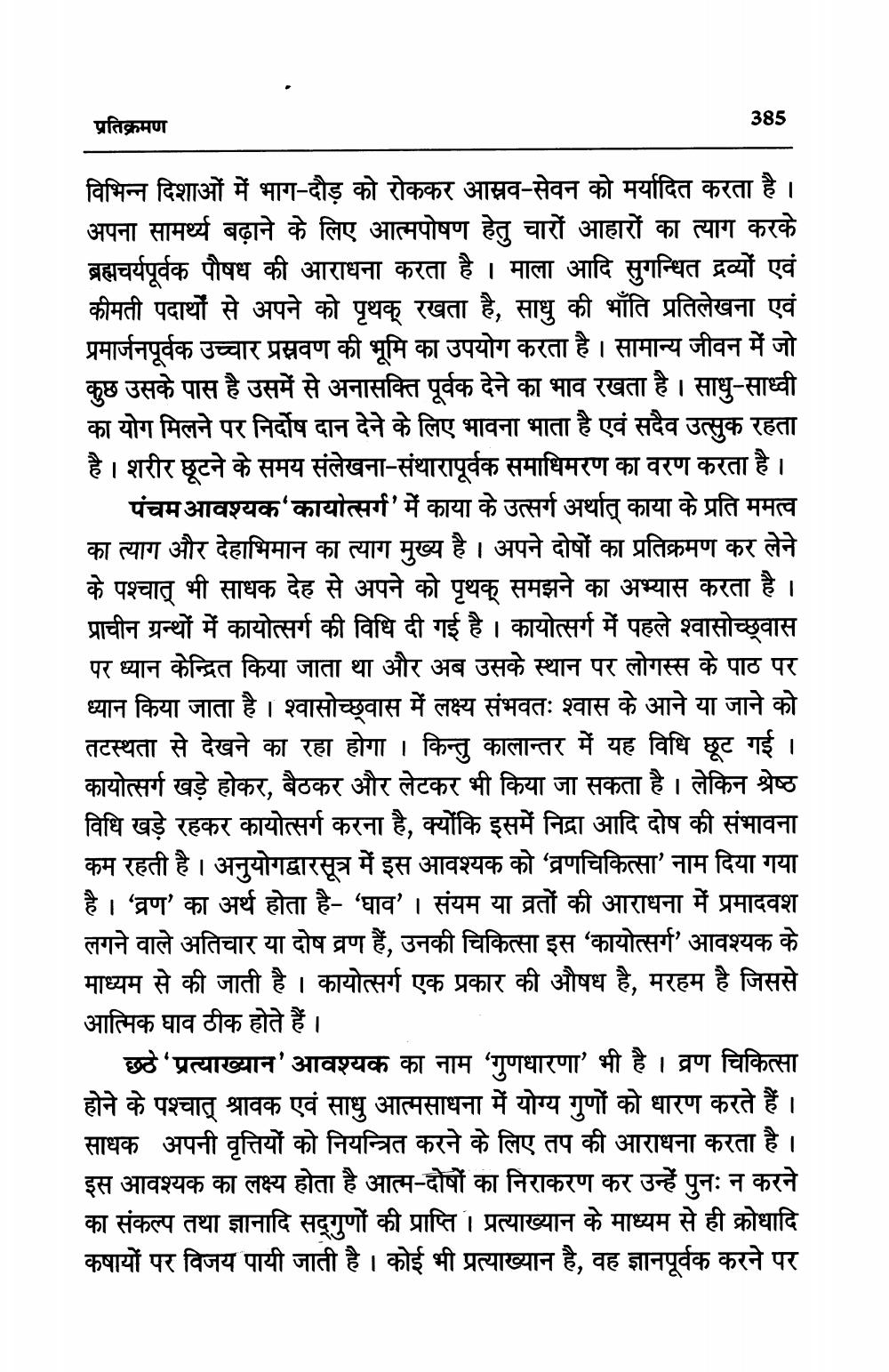________________
प्रतिक्रमण
385
विभिन्न दिशाओं में भाग-दौड़ को रोककर आनव-सेवन को मर्यादित करता है।
अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए आत्मपोषण हेतु चारों आहारों का त्याग करके ब्रह्मचर्यपूर्वक पौषध की आराधना करता है । माला आदि सुगन्धित द्रव्यों एवं कीमती पदार्थों से अपने को पृथक् रखता है, साधु की भाँति प्रतिलेखना एवं प्रमार्जनपूर्वक उच्चार प्रस्रवण की भूमि का उपयोग करता है। सामान्य जीवन में जो कुछ उसके पास है उसमें से अनासक्ति पूर्वक देने का भाव रखता है। साधु-साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान देने के लिए भावना भाता है एवं सदैव उत्सुक रहता है। शरीर छूटने के समय संलेखना-संथारापूर्वक समाधिमरण का वरण करता है।
पंचमआवश्यक कायोत्सर्ग' में काया के उत्सर्ग अर्थात् काया के प्रति ममत्व का त्याग और देहाभिमान का त्याग मुख्य है। अपने दोषों का प्रतिक्रमण कर लेने के पश्चात् भी साधक देह से अपने को पृथक् समझने का अभ्यास करता है । प्राचीन ग्रन्थों में कायोत्सर्ग की विधि दी गई है। कायोत्सर्ग में पहले श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता था और अब उसके स्थान पर लोगस्स के पाठ पर ध्यान किया जाता है। श्वासोच्छ्वास में लक्ष्य संभवतः श्वास के आने या जाने को तटस्थता से देखने का रहा होगा । किन्तु कालान्तर में यह विधि छूट गई । कायोत्सर्ग खड़े होकर, बैठकर और लेटकर भी किया जा सकता है। लेकिन श्रेष्ठ विधि खड़े रहकर कायोत्सर्ग करना है, क्योंकि इसमें निद्रा आदि दोष की संभावना कम रहती है। अनुयोगद्वारसूत्र में इस आवश्यक को 'व्रणचिकित्सा' नाम दिया गया है। 'व्रण' का अर्थ होता है- 'घाव' । संयम या व्रतों की आराधना में प्रमादवश लगने वाले अतिचार या दोष व्रण हैं, उनकी चिकित्सा इस 'कायोत्सर्ग' आवश्यक के माध्यम से की जाती है । कायोत्सर्ग एक प्रकार की औषध है, मरहम है जिससे आत्मिक घाव ठीक होते हैं।
छठे 'प्रत्याख्यान' आवश्यक का नाम 'गुणधारणा' भी है । व्रण चिकित्सा होने के पश्चात् श्रावक एवं साधु आत्मसाधना में योग्य गुणों को धारण करते हैं। साधक अपनी वृत्तियों को नियन्त्रित करने के लिए तप की आराधना करता है। इस आवश्यक का लक्ष्य होता है आत्म-दोषों का निराकरण कर उन्हें पुनः न करने का संकल्प तथा ज्ञानादि सद्गुणों की प्राप्ति । प्रत्याख्यान के माध्यम से ही क्रोधादि कषायों पर विजय पायी जाती है। कोई भी प्रत्याख्यान है, वह ज्ञानपूर्वक करने पर