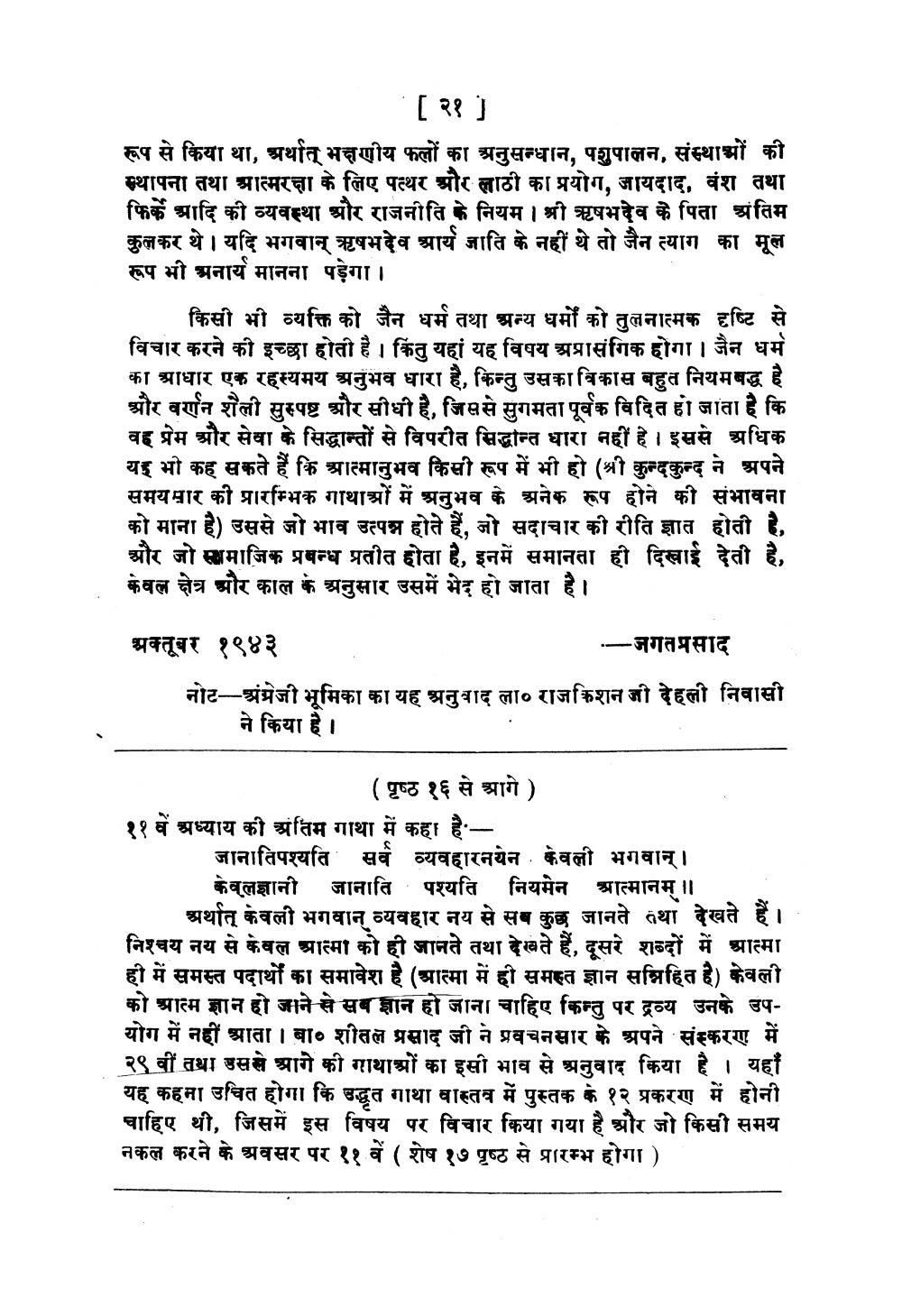________________
[ २१ । रूप से किया था, अर्थात् भक्षणीय फलों का अनुसन्धान, पशुपालन, संस्थाओं की स्थापना तथा आत्मरक्षा के लिए पत्थर और लाठी का प्रयोग, जायदाद, वंश तथा फिर्के आदि की व्यवस्था और राजनीति के नियम । श्री ऋषभदेव के पिता अंतिम कुलकर थे। यदि भगवान् ऋषभदेव आर्य जाति के नहीं थे तो जैन त्याग का मूल रूप भी अनार्य मानना पड़ेगा।
किसी भी व्यक्ति को जैन धर्म तथा अन्य धर्मों को तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने की इच्छा होती है। किंतु यहां यह विषय अप्रासंगिक होगा। जैन धर्म का आधार एक रहस्यमय अनुभव धारा है, किन्तु उसका विकास बहुत नियमबद्ध है और वर्णन शैली सुस्पष्ट और सीधी है, जिससे सुगमता पूर्वक विदित हो जाता है कि वह प्रेम और सेवा के सिद्धान्तों से विपरीत सिद्धान्त धारा नहीं है। इससे अधिक यह भी कह सकते हैं कि आत्मानुभव किसी रूप में भी हो (श्री कुन्दकुन्द ने अपने समयमार की प्रारम्भिक गाथाओं में अनुभव के अनेक रूप होने की संभावना को माना है) उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो सदाचार की रीति ज्ञात होती है, और जो सामाजिक प्रबन्ध प्रतीत होता है, इनमें समानता ही दिखाई देती है, केवल क्षेत्र और काल के अनुसार उसमें भेद हो जाता है।
अक्तूबर १९४३
.-जगतप्रसाद नोट-अंग्रेजी भूमिका का यह अनुवाद ला० राजकिशन जी देहली निवासी
ने किया है।
(पृष्ठ १६ से आगे) ११वें अध्याय की अंतिम गाथा में कहा है -
जानातिपश्यति सर्व व्यवहारनयेन . केवली भगवान् । केवलज्ञानी जानाति · पश्यति नियमेन आत्मानम् ॥
अथात् केवली भगवान व्यवहार नय से सब कुछ जानते तथा देखते हैं। निश्चय नय से केवल आत्मा को ही जानते तथा देखते हैं, दूसरे शब्दों में आत्मा ही में समस्त पदार्थों का समावेश है (आत्मा में ही समस्त ज्ञान सन्निहित है) केवली को आत्म ज्ञान हो जाने से सब ज्ञान हो जाना चाहिए किन्तु पर द्रव्य उनके उपयोग में नहीं आता। बा० शीतल प्रसाद जी ने प्रवचनसार के अपने संस्करण में २९ वीं तथा उससे आगे की गाथाओं का इसी भाव से अनुवाद किया है । यहाँ यह कहना उचित होगा कि उद्धृत गाथा वास्तव में पुस्तक के १२ प्रकरण में होनी चाहिए थी, जिसमें इस विषय पर विचार किया गया है और जो किसी समय नकल करने के अवसर पर ११ वें ( शेष १७ पृष्ठ से प्रारम्भ होगा)