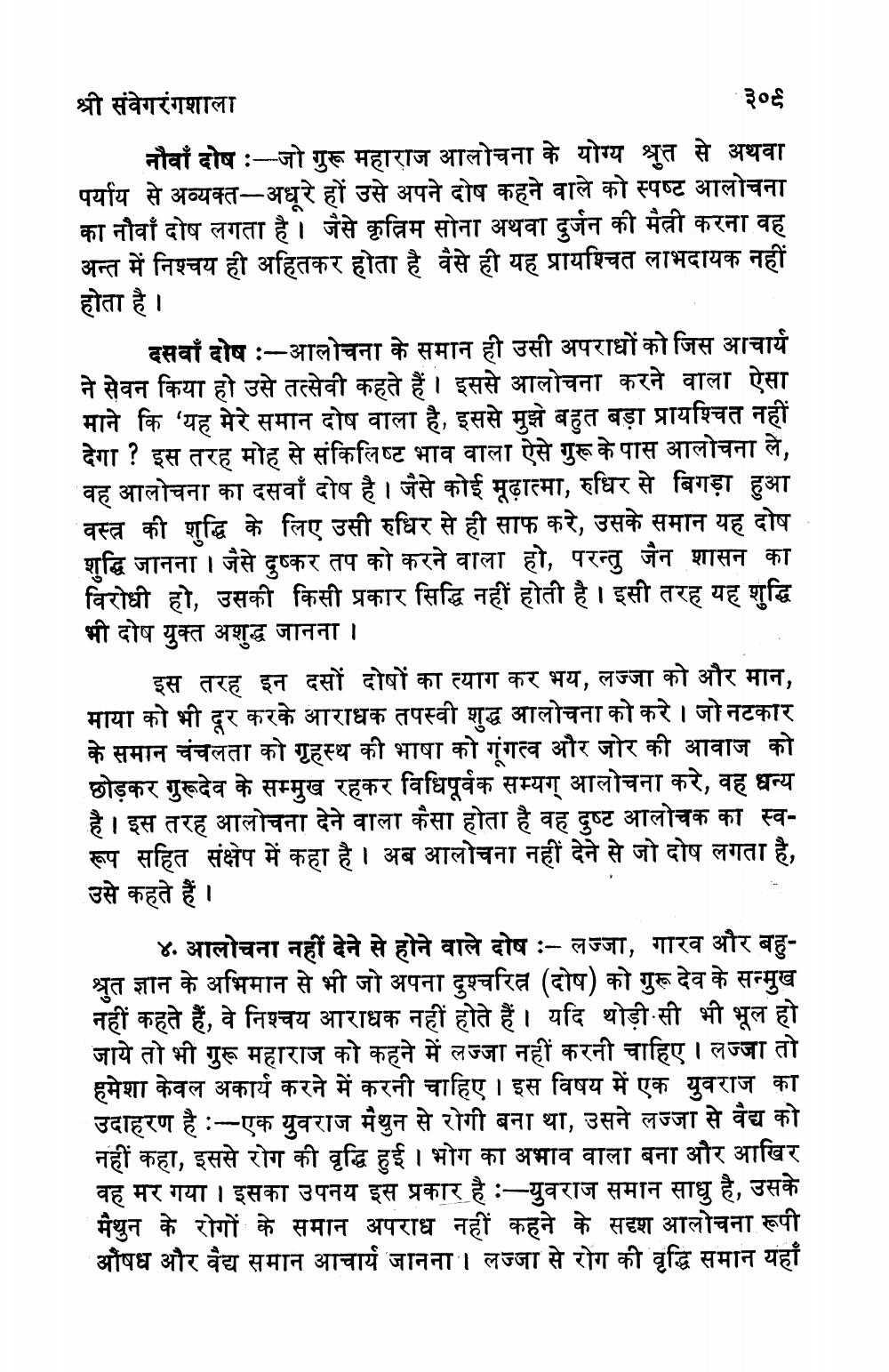________________
श्री संवेगरंगशाला
३०६ नौवाँ दोष :-जो गुरू महाराज आलोचना के योग्य श्रुत से अथवा पर्याय से अव्यक्त-अधूरे हों उसे अपने दोष कहने वाले को स्पष्ट आलोचना का नौवाँ दोष लगता है। जैसे कृत्रिम सोना अथवा दुर्जन की मैत्री करना वह अन्त में निश्चय ही अहितकर होता है वैसे ही यह प्रायश्चित लाभदायक नहीं होता है।
__दसवाँ दोष :-आलोचना के समान ही उसी अपराधों को जिस आचार्य ने सेवन किया हो उसे तत्सेवी कहते हैं। इससे आलोचना करने वाला ऐसा माने कि 'यह मेरे समान दोष वाला है, इससे मुझे बहुत बड़ा प्रायश्चित नहीं देगा ? इस तरह मोह से संकिलिष्ट भाव वाला ऐसे गुरू के पास आलोचना ले, वह आलोचना का दसवाँ दोष है। जैसे कोई मूढ़ात्मा, रुधिर से बिगड़ा हुआ वस्त्र की शुद्धि के लिए उसी रुधिर से ही साफ करे, उसके समान यह दोष शुद्धि जानना । जैसे दुष्कर तप को करने वाला हो, परन्तु जैन शासन का विरोधी हो, उसकी किसी प्रकार सिद्धि नहीं होती है। इसी तरह यह शुद्धि भी दोष युक्त अशुद्ध जानना ।
इस तरह इन दसों दोषों का त्याग कर भय, लज्जा को और मान, माया को भी दूर करके आराधक तपस्वी शुद्ध आलोचना को करे । जो नटकार के समान चंचलता को गृहस्थ की भाषा को गूंगत्व और जोर की आवाज को छोड़कर गुरूदेव के सम्मुख रहकर विधिपूर्वक सम्यग् आलोचना करे, वह धन्य है। इस तरह आलोचना देने वाला कैसा होता है वह दुष्ट आलोचक का स्वरूप सहित संक्षेप में कहा है। अब आलोचना नहीं देने से जो दोष लगता है, उसे कहते हैं।
४. आलोचना नहीं देने से होने वाले दोष :- लज्जा, गारव और बहुश्रुत ज्ञान के अभिमान से भी जो अपना दुश्चरित्र (दोष) को गुरू देव के सन्मुख नहीं कहते हैं, वे निश्चय आराधक नहीं होते हैं। यदि थोड़ी सी भी भूल हो जाये तो भी गुरू महाराज को कहने में लज्जा नहीं करनी चाहिए । लज्जा तो हमेशा केवल अकार्य करने में करनी चाहिए । इस विषय में एक युवराज का उदाहरण है :-एक युवराज मैथुन से रोगी बना था, उसने लज्जा से वैद्य को नहीं कहा, इससे रोग की वृद्धि हुई । भोग का अभाव वाला बना और आखिर वह मर गया। इसका उपनय इस प्रकार है :-युवराज समान साधु है, उसके मैथुन के रोगों के समान अपराध नहीं कहने के सदृश आलोचना रूपी औषध और वैद्य समान आचार्य जानना । लज्जा से रोग की वृद्धि समान यहाँ