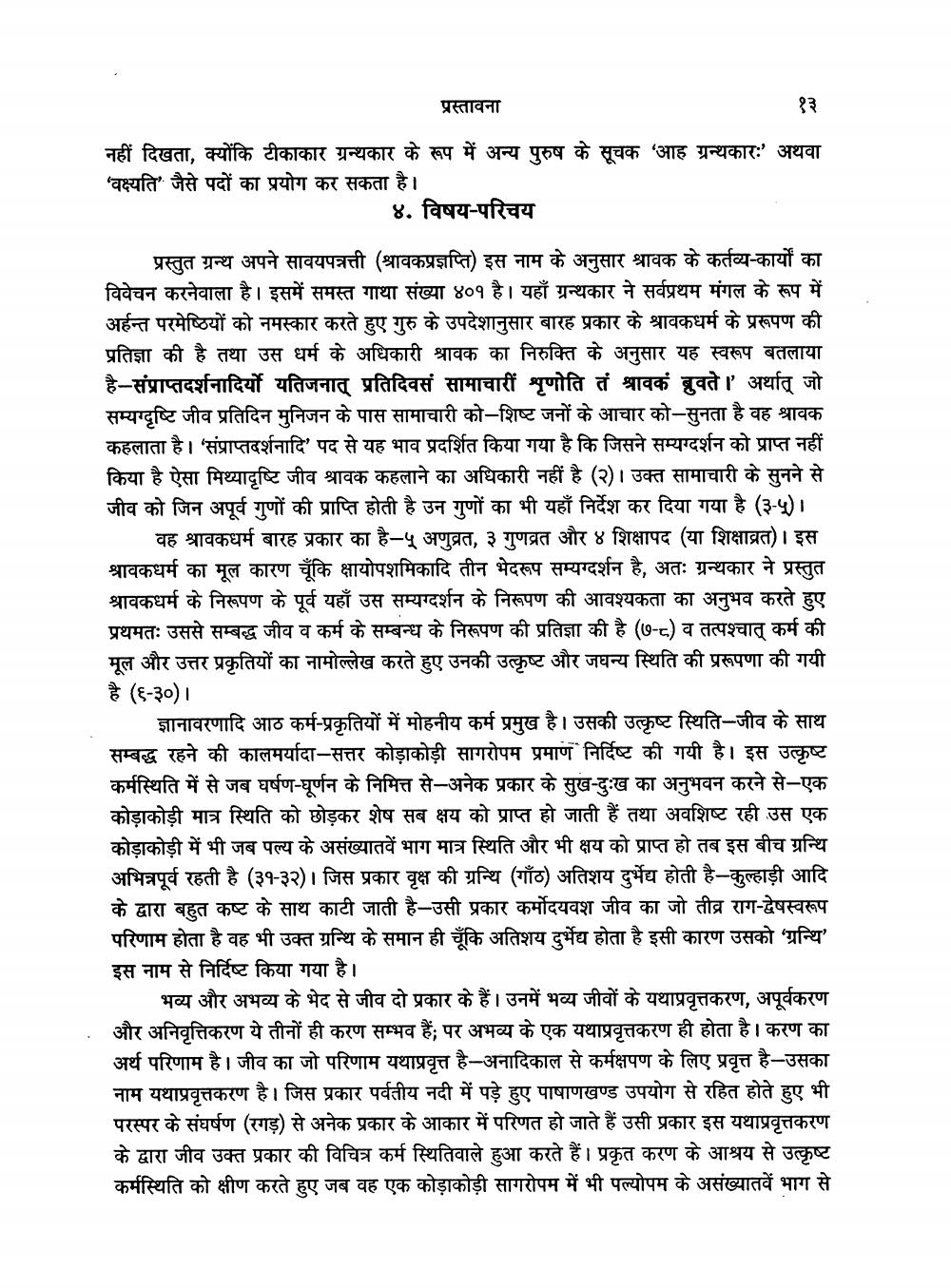________________
प्रस्तावना
१३
नहीं दिखता, क्योंकि टीकाकार ग्रन्थकार के रूप में अन्य पुरुष के सूचक 'आह ग्रन्थकारः' अथवा 'वक्ष्यति' जैसे पदों का प्रयोग कर सकता है ।
४. विषय - परिचय
प्रस्तुत ग्रन्थ अपने सावयपन्नत्ती (श्रावकप्रज्ञप्ति) इस नाम के अनुसार श्रावक के कर्तव्य कार्यों का विवेचन करनेवाला है। इसमें समस्त गाथा संख्या ४०१ है । यहाँ ग्रन्थकार ने सर्वप्रथम मंगल के रूप में अर्हन्त परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए गुरु के उपदेशानुसार बारह प्रकार के श्रावकधर्म के प्ररूपण की प्रतिज्ञा की है तथा उस धर्म के अधिकारी श्रावक का निरुक्ति के अनुसार यह स्वरूप बतलाया है - संप्राप्तदर्शनादिर्यो यतिजनात् प्रतिदिवस सामाचारीं शृणोति तं श्रावकं ब्रुवते ।' अर्थात् जो सम्यग्दृष्टि जीव प्रतिदिन मुनिजन के पास सामाचारी को -शिष्ट जनों के आचार को - सुनता है वह श्रावक कहलाता है । 'संप्राप्तदर्शनादि' पद यह भाव प्रदर्शित किया गया है कि जिसने सम्यग्दर्शन को प्राप्त नहीं किया है ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है (२) । उक्त सामाचारी के सुनने से जीव को जिन अपूर्व गुणों की प्राप्ति होती है उन गुणों का भी यहाँ निर्देश कर दिया गया है (३-५)।
वह श्रावकधर्म बारह प्रकार का है - ५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत और ४ शिक्षापद (या शिक्षाव्रत ) । इस श्रावकधर्म का मूल कारण चूँकि क्षायोपशमिकादि तीन भेदरूप सम्यग्दर्शन है, अतः ग्रन्थकार ने प्रस्तुत श्रावकधर्म के निरूपण के पूर्व यहाँ उस सम्यग्दर्शन के निरूपण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए प्रथमतः उससे सम्बद्ध जीव व कर्म के सम्बन्ध के निरूपण की प्रतिज्ञा की है (७-८) व तत्पश्चात् कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियों का नामोल्लेख करते हुए उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति की प्ररूपणा की गयी
(६-३०) ।
ज्ञानावरणादि आठ कर्म-प्रकृतियों में मोहनीय कर्म प्रमुख है । उसकी उत्कृष्ट स्थिति - जीव के साथ सम्बद्ध रहने की कालमर्यादा -सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण निर्दिष्ट की गयी है। इस उत्कृष्ट कर्मस्थिति में से जब घर्षण - घूर्णन के निमित्त से - अनेक प्रकार के सुख-दुःख का अनुभवन करने से - एक कोड़ाकोड़ी मात्र स्थिति को छोड़कर शेष सब क्षय को प्राप्त हो जाती हैं तथा अवशिष्ट रही उस एक कोड़ाकोड़ी में भी जब पल्य के असंख्यातवें भाग मात्र स्थिति और भी क्षय को प्राप्त हो तब इस बीच ग्रन्थि अभिपूर्व रहती है (३१-३२) । जिस प्रकार वृक्ष की ग्रन्थि (गाँठ ) अतिशय दुर्भेद्य होती है- कुल्हाड़ी आदि के द्वारा बहुत कष्ट के साथ काटी जाती है-उसी प्रकार कर्मोदयवश जीव का जो तीव्र राग-द्वेषस्वरूप परिणाम होता है वह भी उक्त ग्रन्थि के समान ही चूँकि अतिशय दुर्भेद्य होता है इसी कारण उसको 'ग्रन्थि ' इस नाम से निर्दिष्ट किया गया है ।
भव्य और अभव्य के भेद से जीव दो प्रकार के हैं । उनमें भव्य जीवों के यथाप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये तीनों ही करण सम्भव हैं; पर अभव्य के एक यथाप्रवृत्तकरण ही होता है। अर्थ परिणाम है। जीव का जो परिणाम यथाप्रवृत्त है - अनादिकाल से कर्मक्षपण के लिए प्रवृत्त है - उसका नाम यथाप्रवृत्तकरण है। जिस प्रकार पर्वतीय नदी में पड़े हुए पाषाणखण्ड उपयोग से रहित होते हुए भी परस्पर के संघर्षण (रगड़) से अनेक प्रकार के आकार में परिणत हो जाते हैं उसी प्रकार इस यथाप्रवृत्तकरण के द्वारा जीव उक्त प्रकार की विचित्र कर्म स्थितिवाले हुआ करते हैं । प्रकृत करण के आश्रय से उत्कृष्ट कर्मस्थिति को क्षीण करते हुए जब वह एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम में भी पल्योपम के असंख्यातवें भाग से