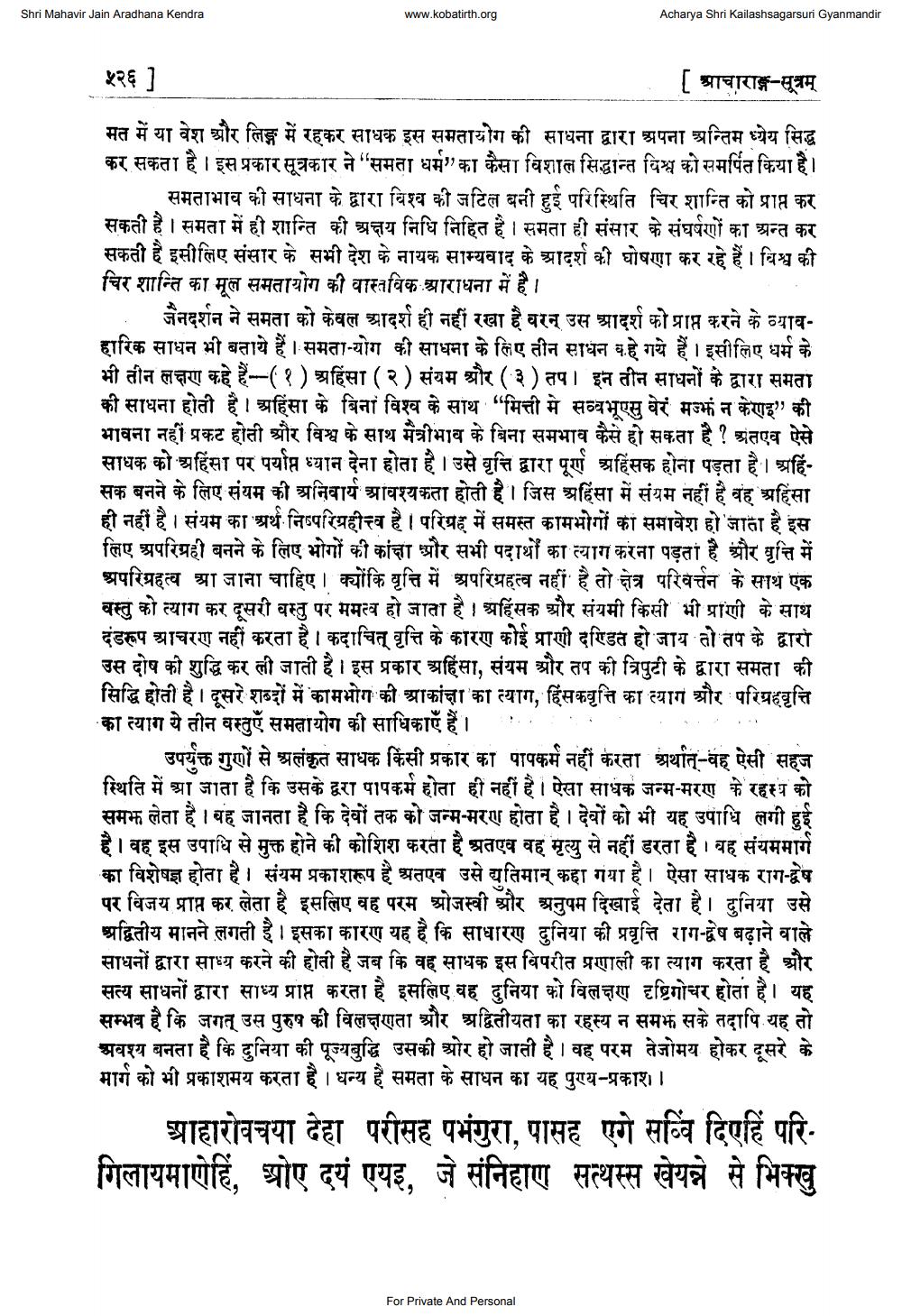________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmandir
५२६ ]
[ आचाराङ्ग-सूत्रम्
मत में या वेश और लिङ्ग में रहकर साधक इस समतायोग की साधना द्वारा अपना अन्तिम ध्येय सिद्ध कर सकता है । इस प्रकार सूत्रकार ने "समता धर्म" का कैसा विशाल सिद्धान्त विश्व को समर्पित किया है।
समताभाव की साधना के द्वारा विश्व की जटिल बनी हुई परिस्थिति चिर शान्ति को प्राप्त कर सकती है । समता में ही शान्ति की अक्षय निधि निहित है। समता ही संसार के संघर्षणों का अन्त कर सकती है इसीलिए संसार के सभी देश के नायक साम्यवाद के आदर्श की घोषणा कर रहे हैं। विश्व की चिर शान्ति का मूल समतायोग की वास्तविक आराधना में है ।
जैनदर्शन ने समता को केवल आदर्श ही नहीं रखा है वरन् उस आदर्श को प्राप्त करने के व्याव हारिक साधन भी बताये हैं । समता-योग की साधना के लिए तीन साधन कहे गये हैं । इसीलिए धर्म के भी तीन लक्षण कहे हैं -- ( १ ) हिंसा ( २ ) संयम और ( ३ ) तप । इन तीन साधनों के द्वारा समता की साधना होती है । अहिंसा के बिना विश्व के साथ "मित्ती मे सव्वभूएस वेरं मज्भं न केाइ" की भावना नहीं प्रकट होती और विश्व के साथ मैत्रीभाव के बिना समभाव कैसे हो सकता है ? अतएव ऐसे साधक को हिंसा पर पर्याप्त ध्यान देना होता है । उसे वृत्ति द्वारा पूर्ण अहिंसक होना पड़ता है। हिंसक बनने के लिए संयम की अनिवार्य आवश्यकता होती है। जिस हिंसा में संयम नहीं है वह अहिंसा
नहीं है । संयम का अर्थ निष्परिग्रहीत्त्व है । परिग्रह में समस्त कामभोगों का समावेश हो जाता है इस लिए अपरिग्रही बनने के लिए भोगों की कांक्षा और सभी पदार्थों का त्याग करना पड़ता है और वृत्ति में अपरिग्रहत्व आ जाना चाहिए। क्योंकि वृत्ति में अपरिग्रहत्व नहीं है तो क्षेत्र परिवर्तन के साथ एक वस्तु को त्याग कर दूसरी वस्तु पर ममत्व हो जाता है। अहिंसक और संयमी किसी भी प्राणी के साथ isरूप चरण नहीं करता है । कदाचित् वृत्ति के कारण कोई प्राणी दण्डित हो जाय तो तप के द्वारो उस दोष की शुद्धि कर ली जाती है। इस प्रकार अहिंसा, संयम और तप की त्रिपुटी के द्वारा समता की सिद्धि होती है। दूसरे शब्दों में कामभोग की आकांक्षा का त्याग, हिंसकवृत्ति का त्याग और परिग्रहवृत्ति - का त्याग ये तीन वस्तुएँ समतायोग की साधिकाएँ हैं ।
उपर्युक्त गुणों से अलंकृत साधक किसी प्रकार का पापकर्म नहीं करता अर्थात् वह ऐसी सहज स्थिति में आ जाता है कि उसके द्वरा पापकर्म होता हीं नहीं है। ऐसा साधक जन्म-मरण के रहस्य को समझ लेता है । वह जानता है कि देवों तक को जन्म-मरण होता है। देवों को भी यह उपाधि लगी हुई है । वह इस उपाधि से मुक्त होने की कोशिश करता है श्रतएव वह मृत्यु से नहीं डरता है । वह संयममार्ग का विशेषज्ञ होता है । संयम प्रकाशरूप है अतएव उसे द्युतिमान् कहा गया है। ऐसा साधक राग-द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेता है इसलिए वह परम प्रोजस्वी और अनुपम दिखाई देता है । दुनिया उसे
द्वितीय मानने लगती है । इसका कारण यह है कि साधारण दुनिया की प्रवृत्ति राग-द्वेष बढ़ाने वाले साधनों द्वारा साध्य करने की होती है जब कि वह साधक इस विपरीत प्रणाली का त्याग करता है और सत्य साधनों द्वारा साध्य प्राप्त करता है इसलिए वह दुनिया को विलक्षण दृष्टिगोचर होता है । यह सम्भव है कि जगत् उस पुरुष की विलक्षणता और अद्वितीयता का रहस्य न समझ सके तदापि यह तो अवश्य बनता है कि दुनिया की पूज्यबुद्धि उसकी ओर हो जाती है । वह परम तेजोमय होकर दूसरे के मार्ग को भी प्रकाशमय करता है । धन्य है समता के साधन का यह पुण्य - प्रकाशः ।
श्राहारोवच्या देहा परीसह पभंगुरा, पासह एगे सव्विं दिएहिं परिगिलायमाणेहिं श्रोए दयं एयर, जे संनिहाण सत्यस्स खेयन्ने से भिक्खु
For Private And Personal