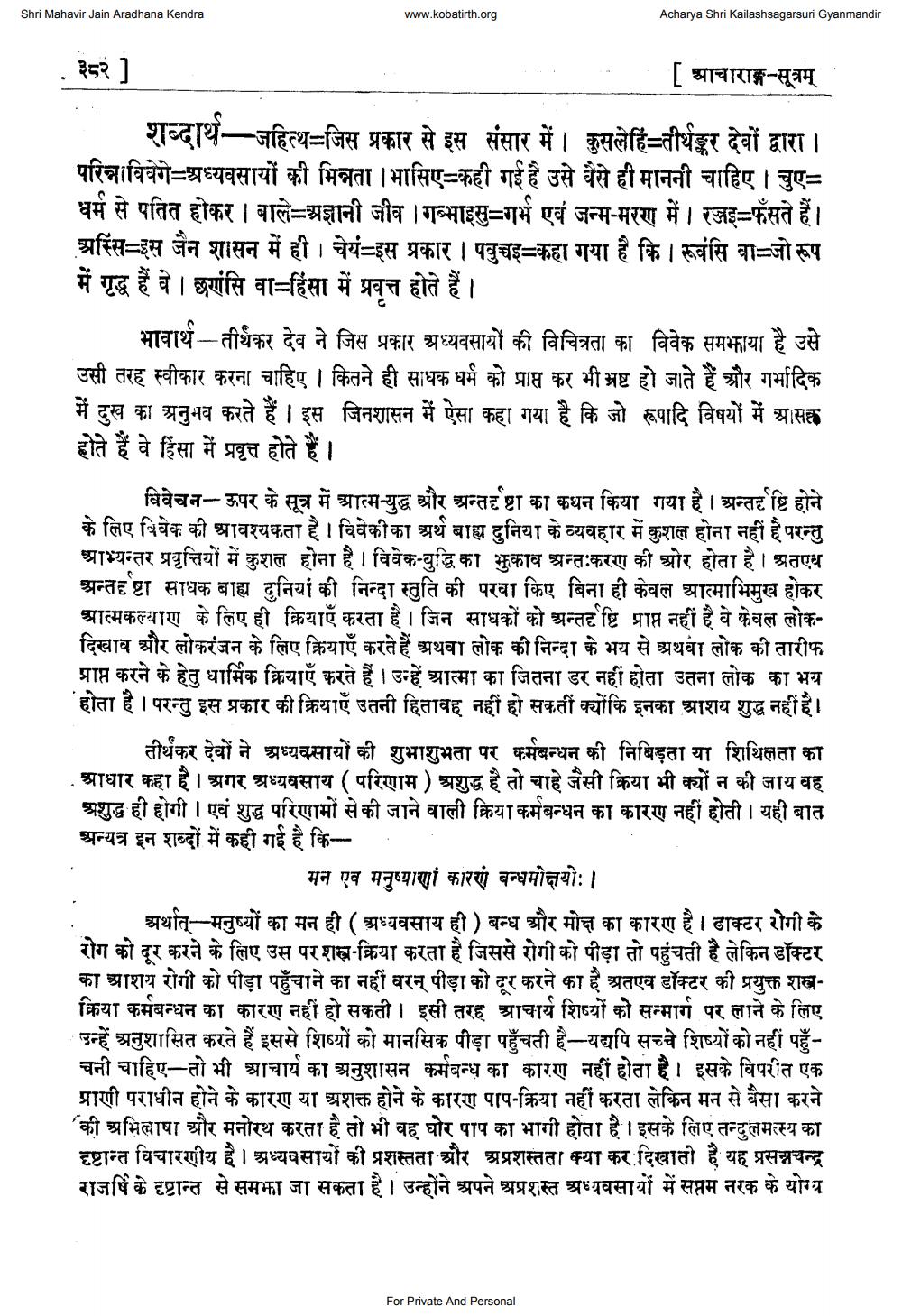________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailashsagarsuri Gyanmandir
. ३८२ ]
[आचाराङ्ग-सूत्रम्
शब्दार्थ-जहित्थ-जिस प्रकार से इस संसार में। कुसलेहि तीर्थङ्कर देवों द्वारा । परिन्नाविवेगे अध्यवसायों की भिन्नता । भासिए कही गई है उसे वैसे ही माननी चाहिए । चुए= धर्म से पतित होकर । बाले अज्ञानी जीव । गब्भाइसु-गर्भ एवं जन्म-मरण में । रजइ फँसते हैं। अस्सि-इस जैन शासन में ही। चेयं इस प्रकार । पवुच्चइ कहा गया है कि । रूवंसि वा जो रूप में गृद्ध हैं वे । छणंसि वा=हिंसा में प्रवृत्त होते हैं ।
भावार्थ-तीर्थकर देव ने जिस प्रकार अध्यवसायों की विचित्रता का विवेक समझाया है उसे उसी तरह स्वीकार करना चाहिए । कितने ही साधक धर्म को प्राप्त कर भी भ्रष्ट हो जाते हैं और गर्भादिक में दुख का अनुभव करते हैं । इस जिनशासन में ऐसा कहा गया है कि जो रूपादि विषयों में प्रासत होते हैं वे हिंसा में प्रवृत्त होते हैं।
विवेचन- ऊपर के सूत्र में आत्म-युद्ध और अन्तर्दृष्टा का कथन किया गया है। अन्तष्टि होने के लिए विवेक की आवश्यकता है । विवेकी का अर्थ बाह्य दुनिया के व्यवहार में कुशल होना नहीं है परन्तु आभ्यन्तर प्रवृत्तियों में कुशल होना है। विवेक-बुद्धि का भुकाव अन्तःकरण की ओर होता है। अतएव अन्तष्टा साधक बाह्य दुनियां की निन्दा स्तुति की परवा किए बिना ही केवल आत्माभिमुख होकर
आत्मकल्याण के लिए ही क्रियाएँ करता है । जिन साधकों को अन्तर्दृष्टि प्राप्त नहीं है वे केवल लोकदिखाव और लोकरंजन के लिए क्रियाएँ करते हैं अथवा लोक की निन्दा के भय से अथवा लोक की तारीफ प्राप्त करने के हेतु धार्मिक क्रियाएँ करते हैं । उन्हें आत्मा का जितना डर नहीं होता उतना लोक का भय होता है । परन्तु इस प्रकार की क्रियाएँ उतनी हितावह नहीं हो सकती क्योंकि इनका आशय शुद्ध नहीं है।
तीर्थंकर देवों ने अध्यक्सायों की शुभाशुभता पर कर्मबन्धन की निबिड़ता या शिथिलता का आधार कहा है। अगर अध्यवसाय ( परिणाम ) अशुद्ध है तो चाहे जैसी क्रिया भी क्यों न की जाय वह अशुद्ध ही होगी । एवं शुद्ध परिणामों से की जाने वाली क्रिया कर्मबन्धन का कारण नहीं होती। यही बात अन्यत्र इन शब्दों में कही गई है कि
__ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । . अर्थात्-मनुष्यों का मन ही (अध्यवसाय ही ) बन्ध और मोक्ष का कारण है । डाक्टर रोगी के रोग को दूर करने के लिए उस पर शस्त्रक्रिया करता है जिससे रोगी को पीड़ा तो पहुंचती है लेकिन डॉक्टर का आशय रोगी को पीड़ा पहुँचाने का नहीं वरन् पीड़ा को दूर करने का है अतएव डॉक्टर की प्रयुक्त शस्त्रक्रिया कर्मबन्धन का कारण नहीं हो सकती। इसी तरह प्राचार्य शिष्यों को सन्मार्ग पर लाने के लिए उन्हें अनुशासित करते हैं इससे शिष्यों को मानसिक पीड़ा पहुँचती है-यद्यपि सच्चे शिष्यों को नहीं पहुँचनी चाहिए तो भी आचार्य का अनुशासन कर्मबन्ध का कारण नहीं होता है। इसके विपरीत एक प्राणी पराधीन होने के कारण या अशक्त होने के कारण पाप-क्रिया नहीं करता लेकिन मन से वैसा करने 'की अभिलाषा और मनोरथ करता है तो भी वह घोर पाप का भागी होता है । इसके लिए तन्दुलमत्स्य का दृष्टान्त विचारणीय है। अध्यवसायों की प्रशस्तता और अप्रशस्तता क्या कर दिखाती है यह प्रसन्नचन्द्र राजर्षि के दृष्टान्त से समझा जा सकता है। उन्होंने अपने प्रशस्त अध्यवसायों में सप्तम नरक के योग्य
For Private And Personal