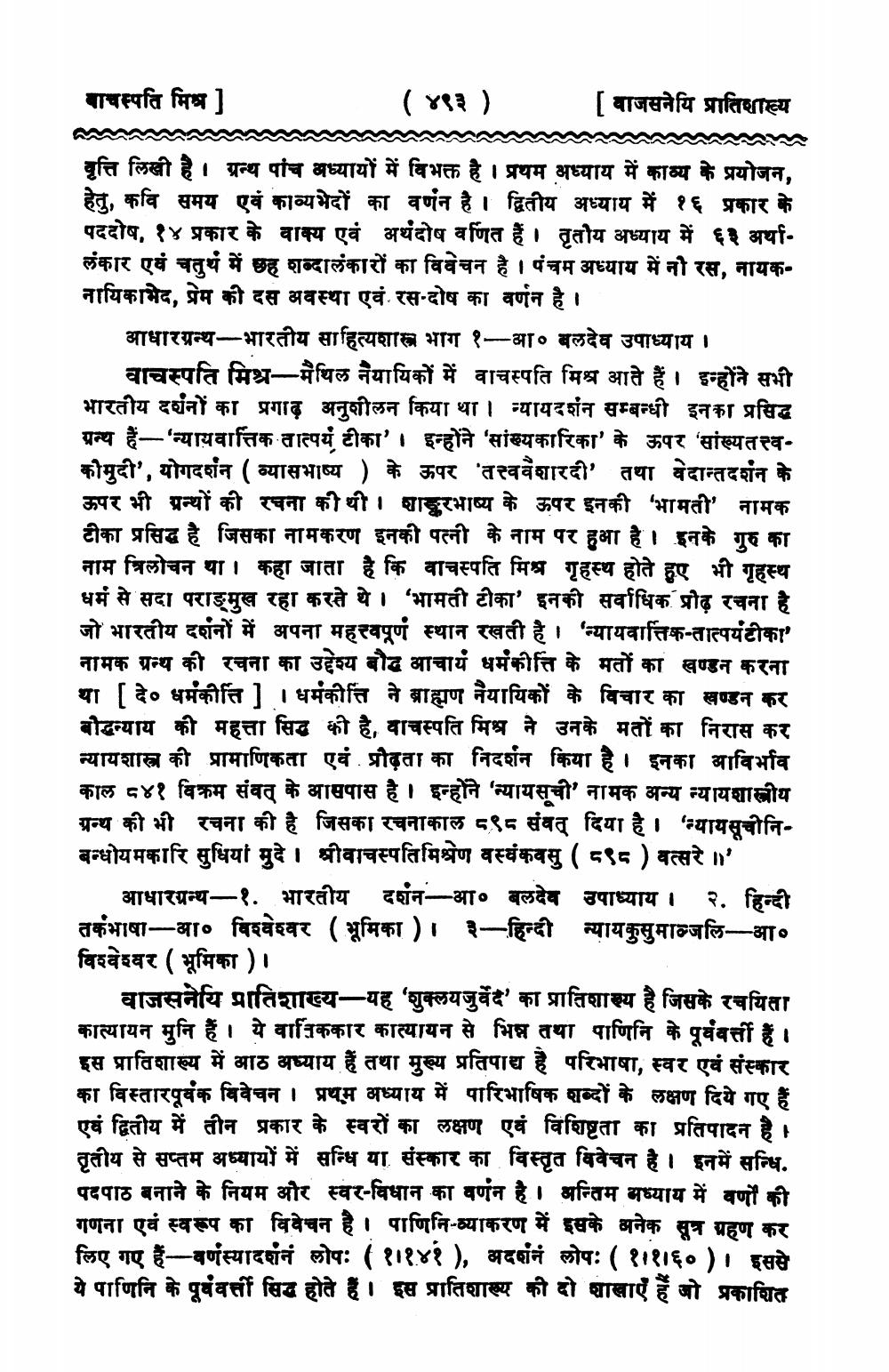________________
वाचस्पति मिश्र]
( ४९३ )
[वाजसनेयि प्रातिशाख्य
वृत्ति लिखी है। ग्रन्थ पांच अध्यायों में विभक्त है । प्रथम अध्याय में काव्य के प्रयोजन, हेतु, कवि समय एवं काव्यभेदों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में १६ प्रकार के पददोष, १४ प्रकार के वाक्य एवं अर्थदोष वर्णित हैं। तृतीय अध्याय में ६३ अर्थालंकार एवं चतुर्थ में छह शब्दालंकारों का विवेचन है । पंचम अध्याय में नो रस, नायकनायिकाभेद, प्रेम की दस अवस्था एवं रस-दोष का वर्णन है।
आधारग्रन्थ-भारतीय साहित्यशास्त्र भाग १-आ० बलदेव उपाध्याय ।
वाचस्पति मिश्र-मैथिल नैयायिकों में वाचस्पति मिश्र आते हैं। इन्होंने सभी भारतीय दर्शनों का प्रगाढ़ अनुशीलन किया था। न्यायदर्शन सम्बन्धी इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं- 'न्यायवात्तिक तात्पर्य टीका'। इन्होंने 'सांख्यकारिका' के ऊपर 'सांख्यतत्व. कौमुदी', योगदर्शन ( व्यासभाष्य ) के ऊपर 'तत्त्ववैशारदी' तथा वेदान्तदर्शन के ऊपर भी ग्रन्थों की रचना की थी। शाङ्करभाष्य के ऊपर इनकी 'भामती' नामक टीका प्रसिद्ध है जिसका नामकरण इनकी पत्नी के नाम पर हुआ है। इनके गुरु का नाम त्रिलोचन था। कहा जाता है कि वाचस्पति मिश्र गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ धर्म से सदा पराङ्मुख रहा करते थे। 'भामती टीका' इनकी सर्वाधिक प्रौढ़ रचना है जो भारतीय दर्शनों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । 'न्यायवात्तिक-तात्पर्यटीका' नामक ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य बौद आचार्य धर्मकीति के मतों का खण्डन करना था [ दे० धर्मकीति] । धर्मकीति ने ब्राह्मण नैयायिकों के विचार का खण्डन कर बौद्धन्याय की महत्ता सिद्ध की है, वाचस्पति मिश्र ने उनके मतों का निरास कर न्यायशास्त्र की प्रामाणिकता एवं प्रौढ़ता का निदर्शन किया है। इनका आविर्भाव काल ८४१ विक्रम संवत् के आसपास है। इन्होंने 'न्यायसूची' नामक अन्य न्यायशास्त्रीय ग्रन्थ की भी रचना की है जिसका रचनाकाल ८९८ संवत् दिया है। न्यायसूचीनिबन्धोयमकारि सुधियां मुदे । श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वंकवसु ( ८९८) वत्सरे॥'
आधारग्रन्थ-१. भारतीय दर्शन-आ. बलदेव उपाध्याय । २. हिन्दी तर्कभाषा-आ. विश्वेश्वर (भूमिका)। ३-हिन्दी न्यायकुसुमान्जलि-आ० विश्वेश्वर ( भूमिका )।
वाजसनेयि प्रातिशाख्य-यह 'शुक्लयजुर्वेद' का प्रातिशाख्य है जिसके रचयिता कात्यायन मुनि हैं। ये वार्तिककार कात्यायन से भिन्न तथा पाणिनि के पूर्ववर्ती हैं। इस प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं तथा मुख्य प्रतिपाद्य है परिभाषा, स्वर एवं संस्कार का विस्तारपूर्वक विवेचन । प्रथम अध्याय में पारिभाषिक शब्दों के लक्षण दिये गए हैं एवं द्वितीय में तीन प्रकार के स्वरों का लक्षण एवं विशिष्टता का प्रतिपादन है। तृतीय से सप्तम अध्यायों में सन्धि या संस्कार का विस्तृत विवेचन है। इनमें सन्धि. पदपाठ बनाने के नियम और स्वर-विधान का वर्णन है। अन्तिम अध्याय में वर्णों की गणना एवं स्वरूप का विवेचन है। पाणिनि-व्याकरण में इसके अनेक सूत्र ग्रहण कर लिए गए हैं-वर्णस्यादर्शनं लोपः (१।१४१), अदर्शनं लोपः ( १११६६०)। इससे ये पाणिनि के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। इस प्रातिशाख्य की दो शाखाएं हैं जो प्रकाशित