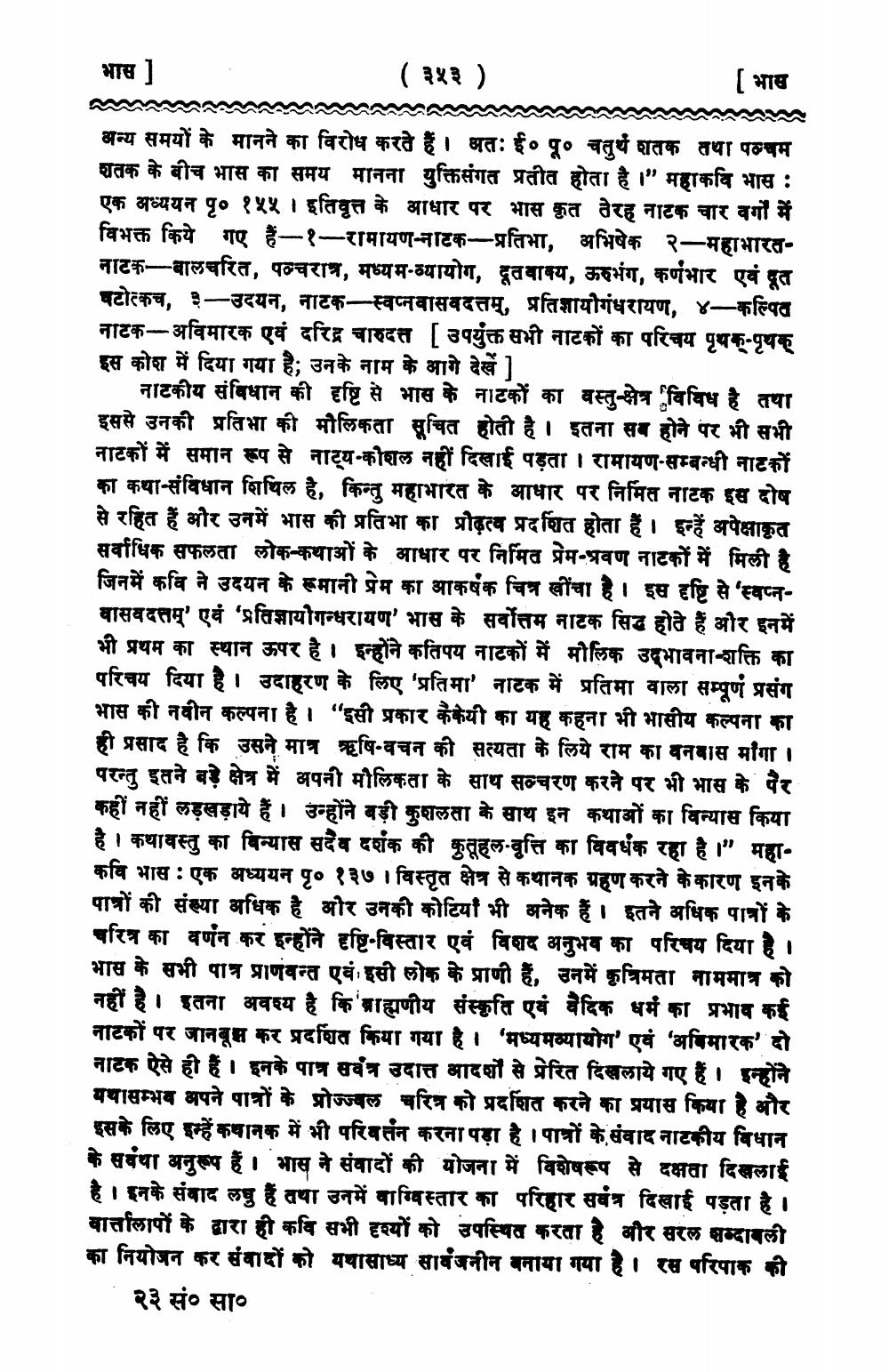________________
भास]
( ३५३ )
[भास
अन्य समयों के मानने का विरोध करते हैं। अतः ई० पू० चतुर्थ शतक तथा पञ्चम शतक के बीच भास का समय मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।" महाकवि भास : एक अध्ययन पृ० १५५ । इतिवृत्त के आधार पर भास कृत तेरह नाटक चार वर्गों में विभक्त किये गए हैं-१-रामायण-नाटक-प्रतिभा, अभिषेक २-महाभारतनाटक-बालचरित, पन्चरात्र, मध्यम-व्यायोग, दूतवाक्य, ऊरुभंग, कर्णभार एवं दूत घटोत्कच, ३-उदयन, नाटक-स्वप्नवासवदत्तम्, प्रतिज्ञायोगंधरायण, ४-कल्पित नाटक-अविमारक एवं दरिद्र चारुदत्त [ उपर्युक्त सभी नाटकों का परिचय पृथक्-पृथक् इस कोश में दिया गया है; उनके नाम के आगे देखें ] ___ नाटकीय संविधान की दृष्टि से भास के नाटकों का वस्तु-क्षेत्र विविध है तथा इससे उनकी प्रतिभा की मौलिकता सूचित होती है। इतना सब होने पर भी सभी नाटकों में समान रूप से नाट्य-कौशल नहीं दिखाई पड़ता । रामायण-सम्बन्धी नाटकों का कथा-संविधान शिथिल है, किन्तु महाभारत के आधार पर निर्मित नाटक इस दोष से रहित हैं और उनमें भास की प्रतिभा का प्रौढत्व प्रदर्शित होता हैं। इन्हें अपेक्षाकृत सर्वाधिक सफलता लोक-कथाओं के आधार पर निर्मित प्रेम-प्रवण नाटकों में मिली है जिनमें कवि ने उदयन के रूमानी प्रेम का आकर्षक चित्र खींचा है। इस दृष्टि से 'स्वप्नवासवदत्तम्' एवं 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' भास के सर्वोत्तम नाटक सिद्ध होते हैं और इनमें भी प्रथम का स्थान ऊपर है। इन्होंने कतिपय नाटकों में मौलिक उद्भावना-शक्ति का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए 'प्रतिमा' नाटक में प्रतिमा वाला सम्पूर्ण प्रसंग भास की नवीन कल्पना है। "इसी प्रकार कैकेयी का यह कहना भी भासीय कल्पना का ही प्रसाद है कि उसने मात्र ऋषि-वचन की सत्यता के लिये राम का वनवास मांगा। परन्तु इतने बड़े क्षेत्र में अपनी मौलिकता के साथ सन्चरण करने पर भी भास के पैर कहीं नहीं लड़खड़ाये हैं। उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ इन कथाओं का विन्यास किया है । कथावस्तु का विन्यास सदैव दर्शक की कुतूहल-वृत्ति का विवर्धक रहा है।" महा. कवि भास : एक अध्ययन पृ० १३७ । विस्तृत क्षेत्र से कथानक ग्रहण करने के कारण इनके पात्रों की संख्या अधिक है और उनकी कोटियां भी अनेक हैं। इतने अधिक पात्रों के चरित्र का वर्णन कर इन्होंने दृष्टि विस्तार एवं विशद अनुभव का परिचय दिया है। भास के सभी पात्र प्राणवन्त एवं इसी लोक के प्राणी हैं, उनमें कृत्रिमता नाममात्र को नहीं है। इतना अवश्य है कि ब्राह्मणीय संस्कृति एवं वैदिक धर्म का प्रभाव कई नाटकों पर जानबूझ कर प्रदर्शित किया गया है। 'मध्यमव्यायोग' एवं 'अविमारक' दो नाटक ऐसे ही हैं। इनके पात्र सर्वत्र उदात्त आदशों से प्रेरित दिखलाये गए हैं। इन्होंने यथासम्भव अपने पात्रों के प्रोज्ज्वल चरित्र को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है और इसके लिए इन्हें कथानक में भी परिवर्तन करना पड़ा है । पात्रों के संवाद नाटकीय विधान के सर्वथा अनुरूप हैं। भास ने संवादों की योजना में विशेषरूप से दक्षता दिखलाई है। इनके संवाद लघु हैं तथा उनमें वाग्विस्तार का परिहार सर्वत्र दिखाई पड़ता है। वार्तालापों के द्वारा ही कवि सभी दृश्यों को उपस्थित करता है और सरल शब्दावली का नियोजन कर संवादों को यथासाध्य सार्वजनीन बनाया गया है। रस परिपाक की
२३ सं० सा०