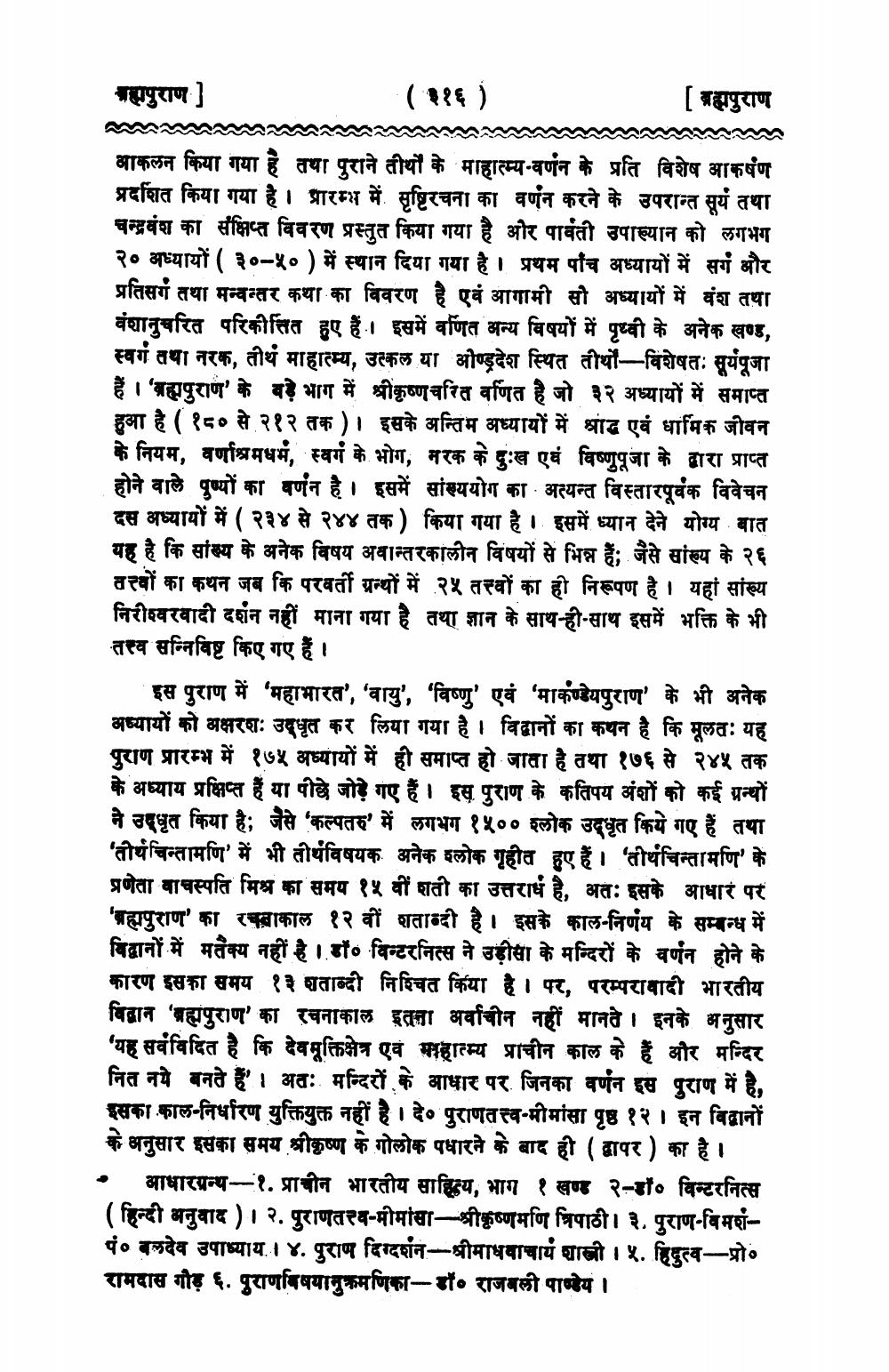________________
ब्रह्मपुराण]
( ३१६ )
[ब्रह्मपुराण
अाकलन किया गया है तथा पुराने तीर्थों के माहात्म्य-वर्णन के प्रति विशेष आकर्षण प्रदर्शित किया गया है। प्रारम्भ में सृष्टिरचना का वर्णन करने के उपरान्त सूर्य तथा चन्द्रवंश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है और पार्वती उपाख्यान को लगभग २० अध्यायों ( ३०-५० ) में स्थान दिया गया है। प्रथम पांच अध्यायों में सर्ग और प्रतिसगं तथा मन्वन्तर कथा का विवरण है एवं आगामी सो अध्यायों में वंश तथा वंशानुचरित परिकीतित हुए हैं। इसमें वर्णित अन्य विषयों में पृथ्वी के अनेक खण्ड, स्वर्ग तथा नरक, तीथ माहात्म्य, उत्कल या ओण्डदेश स्थित तीर्थो-विशेषतः सूर्यपूजा हैं । 'ब्रह्मपुराण' के बड़े भाग में श्रीकृष्णचरित वणित है जो ३२ अध्यायों में समाप्त हुआ है ( १८० से २१२ तक)। इसके अन्तिम अध्यायों में श्राद्ध एवं धार्मिक जीवन के नियम, वर्णाश्रमधर्म, स्वर्ग के भोग, नरक के दुःख एवं विष्णुपूजा के द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्यों का वर्णन है। इसमें सांख्ययोग का - अत्यन्त विस्तारपूर्वक विवेचन दस अध्यायों में ( २३४ से २४४ तक) किया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि सांख्य के अनेक विषय अवान्तरकालीन विषयों से भिन्न हैं; जैसे सांख्य के २६ तत्त्वों का कथन जब कि परवर्ती ग्रन्थों में २५ तत्वों का ही निरूपण है। यहां सांख्य निरीश्वरवादी दर्शन नहीं माना गया है तथा ज्ञान के साथ-ही-साथ इसमें भक्ति के भी तत्व सन्निविष्ट किए गए हैं।
इस पुराण में 'महाभारत', 'वायु', 'विष्णु' एवं 'मार्कण्डेयपुराण' के भी अनेक अध्यायों को अक्षरशः उद्धृत कर लिया गया है । विद्वानों का कथन है कि मूलतः यह पुराण प्रारम्भ में १७५ अध्यायों में ही समाप्त हो जाता है तथा १७६ से २४५ तक के अध्याय प्रक्षिप्त हैं या पीछे जोड़े गए हैं। इस पुराण के कतिपय अंशों को कई ग्रन्थों ने उद्धृत किया है; जैसे 'कल्पतरु' में लगभग १५०० श्लोक उद्धृत किये गए हैं तथा 'तीर्थचिन्तामणि' में भी तीर्थविषयक अनेक श्लोक गृहीत हुए हैं। 'तीर्थचिन्तामणि' के प्रणेता वाचस्पति मिश्र का समय १५ वीं शती का उत्तरार्ध है, अतः इसके आधार पर 'ब्रह्मपुराण' का रचनाकाल १२ वीं शताब्दी है। इसके काल-निर्णय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है । डॉ० विन्टरनित्स ने उड़ीसा के मन्दिरों के वर्णन होने के कारण इसका समय १३ शताब्दी निश्चित किया है। पर, परम्परावादी भारतीय विद्वान 'ब्रह्मपुराण' का रचनाकाल इतना अर्वाचीन नहीं मानते। इनके अनुसार 'यह सर्वविदित है कि देवमूक्तिक्षेत्र एवं माहात्म्य प्राचीन काल के हैं और मन्दिर नित नये बनते हैं। अतः मन्दिरों के आधार पर जिनका वर्णन इस पुराण में है, इसका काल-निर्धारण युक्तियुक्त नहीं है । दे. पुराणतत्त्व-मीमांसा पृष्ठ १२ । इन विद्वानों के अनुसार इसका समय श्रीकृष्ण के गोलोक पधारने के बाद ही ( द्वापर ) का है। • आधारग्रन्थ-१. प्राचीन भारतीय साहित्य, भाग १ खण्ड २-डॉ. विन्टरनित्स (हिन्दी अनुवाद ) । २. पुराणतरव-मीमांसा-श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी। ३. पुराण-विमर्शपं. बलदेव उपाध्याय.। ४. पुराण दिग्दर्शन-श्रीमाधवाचार्य शास्त्री । ५. हिदुत्व-प्रो. रामदास गौड़ ६. पुराणविषयानुक्रमणिका-डॉ. राजबली पाण्डेय ।