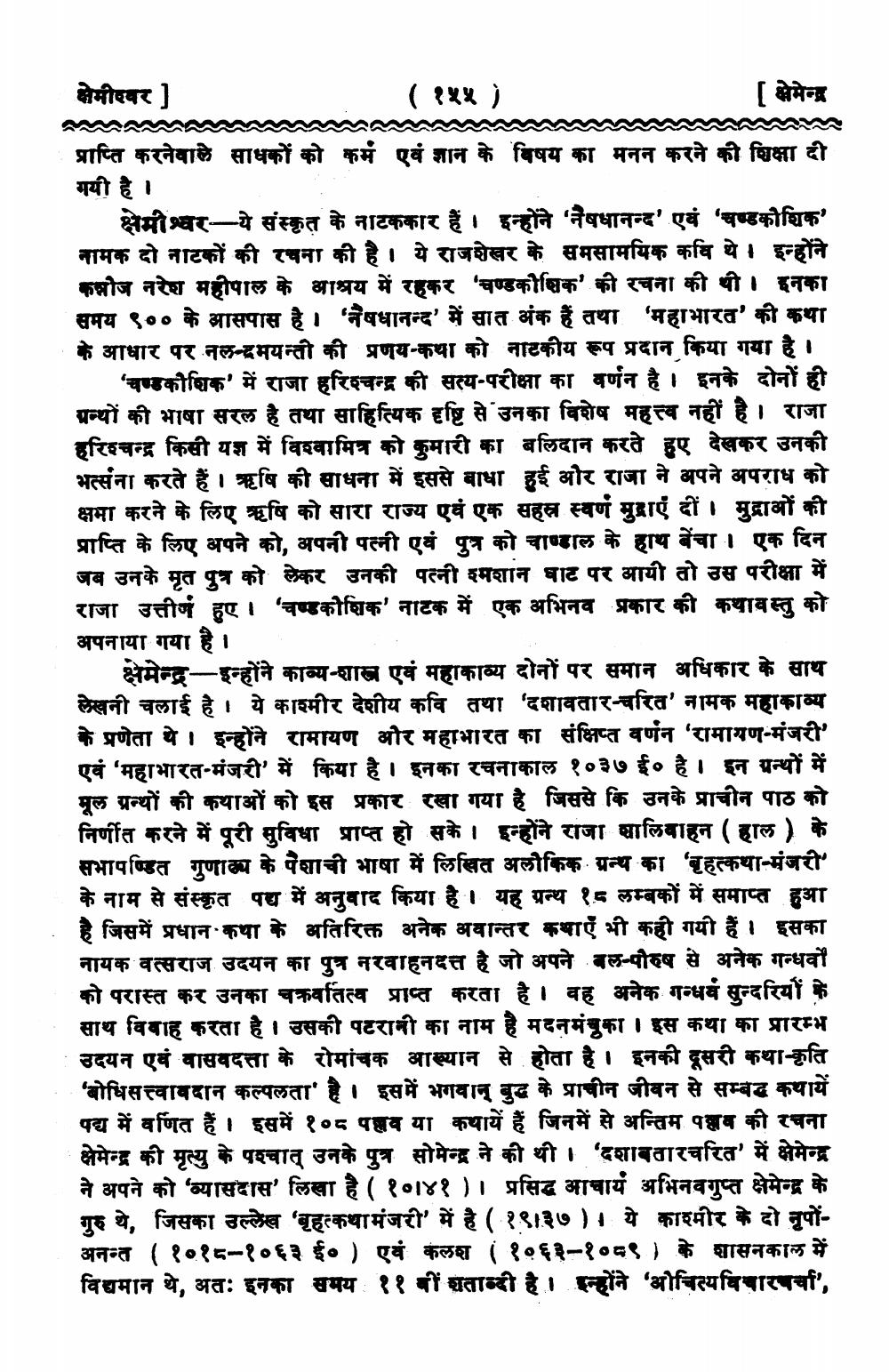________________
क्षेमीश्वर]
( १५५)
[क्षेमेन्द्र
प्राप्ति करनेवाले साधकों को कम एवं ज्ञान के विषय का मनन करने की शिक्षा दी गयी है।
क्षेमीश्वर-ये संस्कृत के नाटककार हैं। इन्होंने 'नैषधानन्द' एवं 'चण्डकौशिक' नामक दो नाटकों की रचना की है। ये राजशेखर के समसामयिक कवि थे। इन्होंने कन्नौज नरेश महीपाल के आश्रय में रहकर 'चण्डकौशिक' की रचना की थी। इनका समय ९०० के आसपास है। 'नैषधानन्द' में सात अंक हैं तथा 'महाभारत' की कथा के आधार पर नल-दमयन्ती की प्रणय-कथा को नाटकीय रूप प्रदान किया गया है। ___ 'चण्डकोशिक' में राजा हरिश्चन्द्र की सत्य-परीक्षा का वर्णन है। इनके दोनों ही अन्यों की भाषा सरल है तथा साहित्यिक दृष्टि से उनका विशेष महत्त्व नहीं है। राजा हरिश्चन्द्र किसी यज्ञ में विश्वामित्र को कुमारी का बलिदान करते हुए देखकर उनकी भत्सना करते हैं। ऋषि की साधना में इससे बाधा हुई और राजा ने अपने अपराध को क्षमा करने के लिए ऋषि को सारा राज्य एवं एक सहस्र स्वर्ण मुद्राएं दीं। मुद्राओं की प्राप्ति के लिए अपने को, अपनी पत्नी एवं पुत्र को चाण्डाल के हाथ बेंचा। एक दिन जब उनके मृत पुत्र को लेकर उनकी पत्नी श्मशान घाट पर आयी तो उस परीक्षा में राजा उत्तीर्ण हुए। 'चण्डकोशिक' नाटक में एक अभिनव प्रकार की कथावस्तु को अपनाया गया है।
क्षेमेन्द्र-इन्होंने काव्य-शास्त्र एवं महाकाव्य दोनों पर समान अधिकार के साथ लेखनी चलाई है। ये काश्मीर देशीय कवि तथा 'दशावतार-चरित' नामक महाकाव्य के प्रणेता थे। इन्होंने रामायण और महाभारत का संक्षिप्त वर्णन 'रामायण-मंजरी' एवं 'महाभारत-मंजरी' में किया है। इनका रचनाकाल १०३७ ई० है। इन ग्रन्थों में मूल ग्रन्थों की कथाओं को इस प्रकार रखा गया है जिससे कि उनके प्राचीन पाठ को निर्णीत करने में पूरी सुविधा प्राप्त हो सके। इन्होंने राजा शालिवाहन (हाल) के सभापण्डित गुणाढ्य के पैशाची भाषा में लिखित अलौकिक ग्रन्थ का 'बृहत्कथा-मंजरी' के नाम से संस्कृत पद्य में अनुवाद किया है। यह ग्रन्थ १८ लम्बकों में समाप्त हुआ है जिसमें प्रधान कथा के अतिरिक्त अनेक अवान्तर कथाएँ भी कही गयी हैं। इसका नायक वत्सराज उदयन का पुत्र नरवाहनदत्त है जो अपने बल-पौरुष से अनेक गन्धों को परास्त कर उनका चक्रवर्तित्व प्राप्त करता है। वह अनेक गन्धर्व सुन्दरियों के साथ विवाह करता है । उसकी पटरानी का नाम है मदनमंचुका । इस कथा का प्रारम्भ उदयन एवं वासवदत्ता के रोमांचक आख्यान से होता है। इनकी दूसरी कथा-कृति 'बोधिसत्त्वावदान कल्पलता' है। इसमें भगवान बुद्ध के प्राचीन जीवन से सम्बद्ध कथायें पद्य में वर्णित हैं। इसमें १०८ पल्लव या कथायें हैं जिनमें से अन्तिम पहब की रचना क्षेमेन्द्र की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र सोमेन्द्र ने की थी। 'दशावतारचरित' में क्षेमेन्द्र ने अपने को 'व्यासदास' लिखा है ( १०॥४१ )। प्रसिद्ध आचार्य अभिनवगुप्त क्षेमेन्द्र के गुरु थे, जिसका उल्लेख 'बृहत्कथामंजरी' में है ( १९:३७ )। ये काश्मीर के दो नृपोंअनन्त ( १०१८-१०६३ ई.) एवं कलश । १०६३-१०८९) के शासनकाल में विद्यमान थे, अतः इनका समय ११ वीं शताब्दी है। इन्होंने 'औचित्यविचारपर्चा',