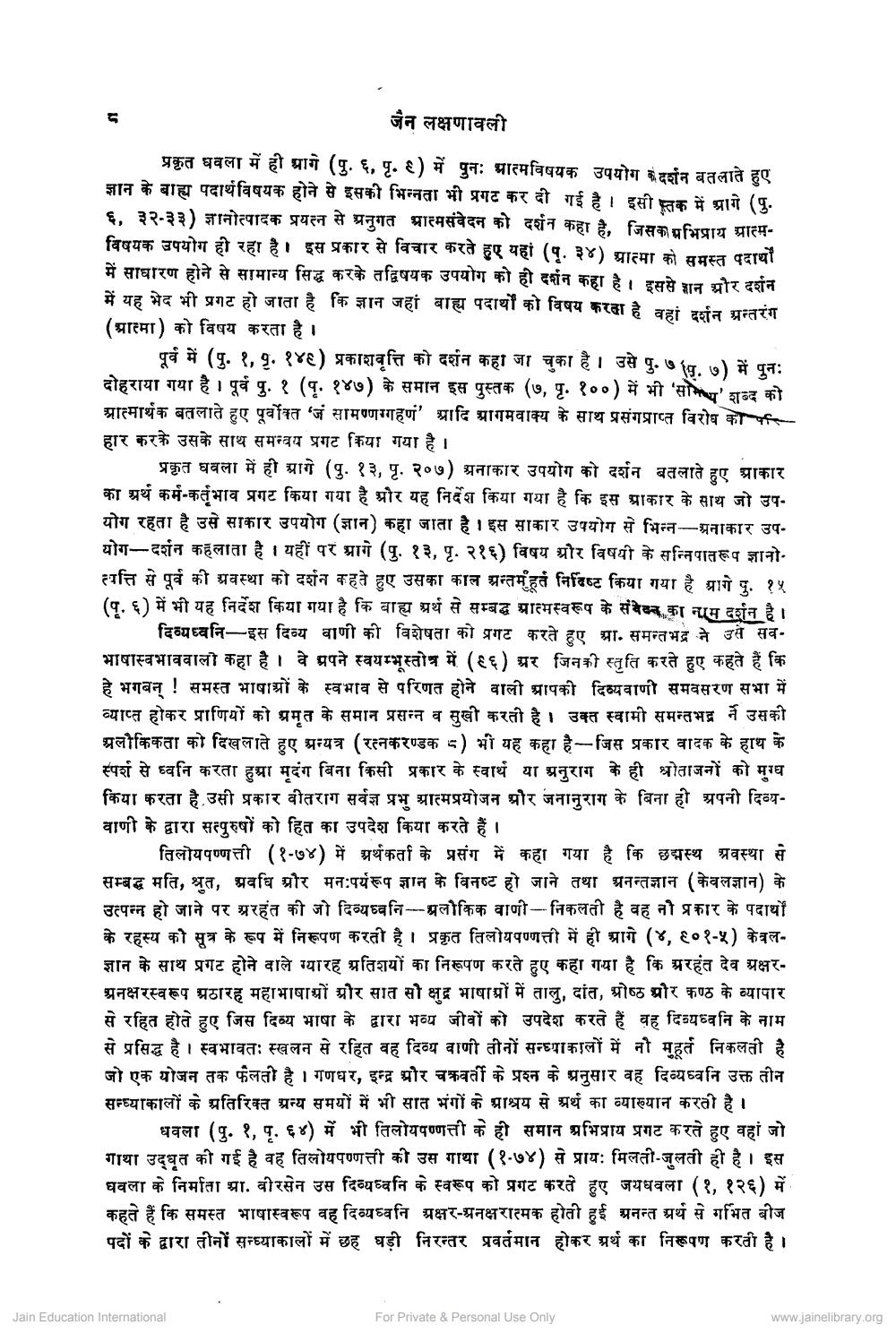________________
जैन लक्षणावली प्रकृत धवला में ही प्रागे (पु. ६, पृ. ६) में पुनः प्रात्मविषयक उपयोग के दर्शन बतलाते हुए ज्ञान के बाह्य पदार्थविषयक होने से इसकी भिन्नता भी प्रगट कर दी गई है। इसी तक में प्रागे (पु. ६, ३२-३३) ज्ञानोत्पादक प्रयत्न से अनुगत प्रात्मसंवेदन को दर्शन कहा है, जिसका अभिप्राय प्रात्मविषयक उपयोग ही रहा है। इस प्रकार से विचार करते हुए यहां (पृ. ३४) प्रात्मा को सस्त पदार्थों में साधारण होने से सामान्य सिद्ध करके तद्विषयक उपयोग को ही दर्शन कहा है। इससे जान और दर्शन में यह भेद भी प्रगट हो जाता है कि ज्ञान जहां बाह्य पदार्थों को विषय करता है वहां दर्शन अन्तरंग (आत्मा) को विषय करता है।
पूर्व में (पु. १, पृ. १४६) प्रकाशवृत्ति को दर्शन कहा जा चुका है। उसे पु. ७. ७) में पुनः दोहराया गया है। पूर्व पु. १ (पृ. १४७) के समान इस पुस्तक (७, पृ. १००) में भी 'साय' शब्द को आत्मार्थक बतलाते हुए पूर्वोक्त 'जं सामण्णग्गहणं' आदि आगमवाक्य के साथ प्रसंगप्राप्त विरोध का परिहार करके उसके साथ समन्वय प्रगट किया गया है।
प्रकृत धवला में ही आगे (पु. १३, पृ. २०७) अनाकार उपयोग को दर्शन बतलाते हए प्राकार का अर्थ कर्म-कर्तृभाव प्रगट किया गया है और यह निर्देश किया गया है कि इस प्रकार के साथ जो उपयोग रहता है उसे साकार उपयोग (ज्ञान) कहा जाता है। इस साकार उपयोग से भिन्न-अनाकार उपयोग-दर्शन कहलाता है । यहीं पर प्रागे (पु. १३, पृ. २१६) विषय और विषयी के सन्निपातरूप ज्ञानो. त्पत्ति से पूर्व की अवस्था को दर्शन कहते हुए उसका काल अन्तर्मुहूर्त निर्दिष्ट किया गया है प्रागे पु. १५ (प. ६) में भी यह निर्देश किया गया है कि बाह्य अर्थ से सम्बद्ध प्रात्मस्वरूप के संवेदन का नाम दर्शन है।
दिव्यध्वनि-इस दिव्य वाणी की विशेषता को प्रगट करते हुए प्रा. समन्तभद्र ने उसे सवभाषास्वभाववालो कहा है। वे अपने स्वयम्भूस्तोत्र में (६६) पर जिनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवन् ! समस्त भाषाओं के स्वभाव से परिणत होने वाली प्रापकी दिव्यवाणी समवसरण सभा में व्याप्त होकर प्राणियों को अमृत के समान प्रसन्न व सूखी करती है। उक्त स्वामी समन्तभद्र ने उसकी अलौकिकता को दिखलाते हुए अन्यत्र (रत्नकरण्डक ८) भी यह कहा है-जिस प्रकार वादक के हाथ के स्पर्श से ध्वनि करता हुआ मृदंग बिना किसी प्रकार के स्वार्थ या अनुराग के ही श्रोताजनों को मुग्ध किया करता है उसी प्रकार वीतराग सर्वज्ञ प्रभु आत्मप्रयोजन और जनानुराग के बिना ही अपनी दिव्यवाणी के द्वारा सत्पुरुषों को हित का उपदेश किया करते हैं।
तिलोयपण्णत्ती (१-७४) में अर्थकर्ता के प्रसंग में कहा गया है कि छद्मस्थ अवस्था से सम्बद्ध मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यरूप ज्ञान के विनष्ट हो जाने तथा अनन्तज्ञान (केवलज्ञान) के उत्पन्न हो जाने पर अरहंत की जो दिव्यध्वनि--अलौकिक वाणी-निकलती है वह नौ प्रकार के पदार्थों के रहस्य को सूत्र के रूप में निरूपण करती है। प्रकृत तिलोयपण्णत्ती में ही आगे (४,६०१-५) केवलज्ञान के साथ प्रगट होने वाले ग्यारह अतिशयों का निरूपण करते हुए कहा गया है कि अरहंत देव अक्षरअनक्षरस्वरूप अठारह महाभाषाओं और सात सौ क्षुद्र भाषाओं में तालु, दांत, प्रोष्ठ और कण्ठ के व्यापार से रहित होते हुए जिस दिव्य भाषा के द्वारा भव्य जीवों को उपदेश करते हैं वह दिव्यध्वनि के नाम से प्रसिद्ध है। स्वभावतः स्खलन से रहित वह दिव्य वाणी तीनों सन्ध्याकालों में नौ मुहूर्त निकलती है जो एक योजन तक फैलती है । गणधर, इन्द्र और चक्रवर्ती के प्रश्न के अनुसार वह दिव्यध्वनि उक्त तीन सन्ध्याकालों के अतिरिक्त अन्य समयों में भी सात भंगों के प्राश्रय से अर्थ का व्याख्यान करती है।
धवला (पु. १, पृ. ६४) में भी तिलोयपण्णत्ती के ही समान अभिप्राय प्रगट करते हुए वहां जो गाथा उद्धत की गई है वह तिलोयपण्णत्ती की उस गाथा (१.७४) से प्रायः मिलती-जुलती ही है। इस धवला के निर्माता प्रा. वीरसेन उस दिव्यध्वनि के स्वरूप को प्रगट करते हुए जयधवला (१, १२६) में कहते हैं कि समस्त भाषास्वरूप वह दिव्यध्वनि अक्षर-अनक्षरात्मक होती हुई अनन्त अर्थ से गभित बीज पदों के द्वारा तीनों सन्ध्याकालों में छह घड़ी निरन्तर प्रवर्तमान होकर अर्थ का निरूपण करती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org