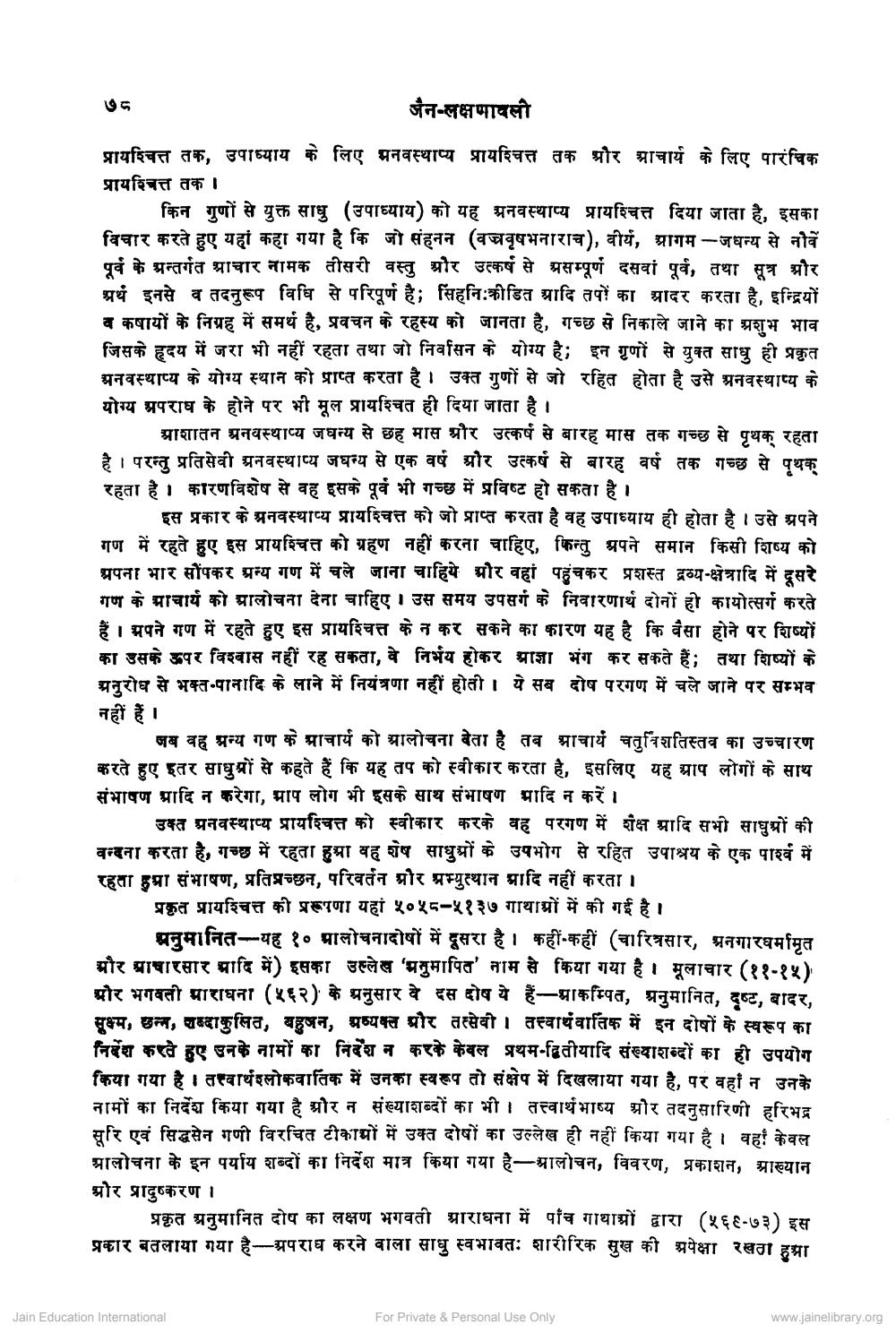________________
जैन - लक्षणावली
प्रायश्चित्त तक, उपाध्याय के लिए अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त तक और आचार्य के लिए पारंचिक प्रायश्चित्त तक |
किन गुणों से युक्त साधु ( उपाध्याय) को यह अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त दिया जाता है, इसका विचार करते हुए यहां कहा गया है कि जो संहनन ( वज्रवृषभनाराच), वीर्य, श्रागम – जघन्य से नौवें पूर्व के अन्तर्गत श्राचार नामक तीसरी वस्तु और उत्कर्ष से असम्पूर्ण दसवां पूर्व, तथा सूत्र और अर्थं इनसे व तदनुरूप विधि से परिपूर्ण है; सिंहनिःक्रीडित श्रादि तपों का आदर करता है, इन्द्रियों व कषायों के निग्रह में समर्थ है, प्रवचन के रहस्य को जानता है, गच्छ से निकाले जाने का अशुभ भाव जिसके हृदय में जरा भी नहीं रहता तथा जो निर्वासन के योग्य है; इन गुणों से युक्त साधु ही प्रकृत अनवस्थाप्य के योग्य स्थान को प्राप्त करता है । उक्त गुणों से जो रहित होता है उसे अनवस्थाप्य के योग्य अपराध के होने पर भी मूल प्रायश्चित ही दिया जाता है । आशातन अनवस्थाप्य जघन्य से छह मास और उत्कर्ष से बारह मास तक गच्छ से पृथक् रहता
७८
है । परन्तु प्रतिसेवी अनवस्थाप्य जघन्य से एक वर्ष और उत्कर्ष से बारह वर्ष तक गच्छ से पृथक् रहता है । कारणविशेष से वह इसके पूर्व भी गच्छ में प्रविष्ट हो सकता है ।
इस प्रकार के अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त को जो प्राप्त करता है वह उपाध्याय ही होता है । उसे अपने गण में रहते हुए इस प्रायश्चित्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किन्तु अपने समान किसी शिष्य को अपना भार सौंपकर अन्य गण में चले जाना चाहिये और वहां पहुंचकर प्रशस्त द्रव्य क्षेत्रादि में दूसरे गण के प्राचार्य को आलोचना देना चाहिए। उस समय उपसर्ग के निवारणार्थ दोनों ही कायोत्सर्ग करते हैं | अपने गण में रहते हुए इस प्रायश्चित्त के न कर सकने का कारण यह है कि वैसा होने पर शिष्यों का उसके ऊपर विश्वास नहीं रह सकता, वे निर्भय होकर आज्ञा भंग कर सकते हैं; तथा शिष्यों के अनुरोध से भक्त पानादि के लाने में नियंत्रणा नहीं होती । ये सब दोष परगण में चले जाने पर सम्भव नहीं हैं।
जब वह अन्य गण के प्राचार्य को आलोचना देता है तब श्राचार्यं चतुत्रिंशतिस्तव का उच्चारण करते हुए इतर साधुत्रों से कहते हैं कि यह तप को स्वीकार करता है, इसलिए यह आप लोगों के साथ संभाषण प्रादि न करेगा, भाप लोग भी इसके साथ संभाषण आदि न करें ।
उक्त अवस्थाप्य प्रायश्चित्त को स्वीकार करके वह परगण में शैक्ष आदि सभी साधुत्रों की वन्दना करता है, गच्छ में रहता हुआ वह शेष साधुत्रों के उपभोग से रहित उपाश्रय के एक पार्श्व में रहता हुआ संभाषण, प्रतिप्रच्छन, परिवर्तन और प्रभ्युत्थान प्रादि नहीं करता ।
प्रकृत प्रायश्चित्त की प्ररूपणा यहां ५०५८-५१३७ गाथाओं में की गई है ।
अनुमानित - यह १० प्रालोचनादोषों में दूसरा है । कहीं-कहीं ( चारित्रसार, अनगारधर्मामृत और प्रचारसार प्रादि में) इसका उल्लेख 'मनुमापित' नाम से किया गया है । मूलाचार (११-१५) और भगवती प्राराधना ( ५६२ ) के अनुसार वे दस दोष ये हैं- प्राकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी । तत्त्वार्थवार्तिक में इन दोषों के स्वरूप का निर्देश करते हुए उनके नामों का निर्देशन करके केवल प्रथम-द्वितीयादि संख्याशब्दों का ही उपयोग किया गया है । तस्वार्थश्लोकवार्तिक में उनका स्वरूप तो संक्षेप में दिखलाया गया है, पर वहाँ न उनके नामों का निर्देश किया गया है और न संख्याशब्दों का भी । तत्त्वार्थभाष्य और तदनुसारिणी हरिभद्र सूरि एवं सिद्धसेन गणी विरचित टीकामों में उक्त दोषों का उल्लेख ही नहीं किया गया है । वहाँ केवल श्रालोचना के इन पर्याय शब्दों का निर्देश मात्र किया गया है— आलोचन, विवरण, प्रकाशन, आख्यान और प्रादुष्करण |
प्रकृत अनुमानित दोष का लक्षण भगवती आराधना में पाँच गाथाओं द्वारा (५६६-७३) इस प्रकार बतलाया गया है- अपराध करने वाला साधु स्वभावतः शारीरिक सुख की अपेक्षा रखता हुआ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org