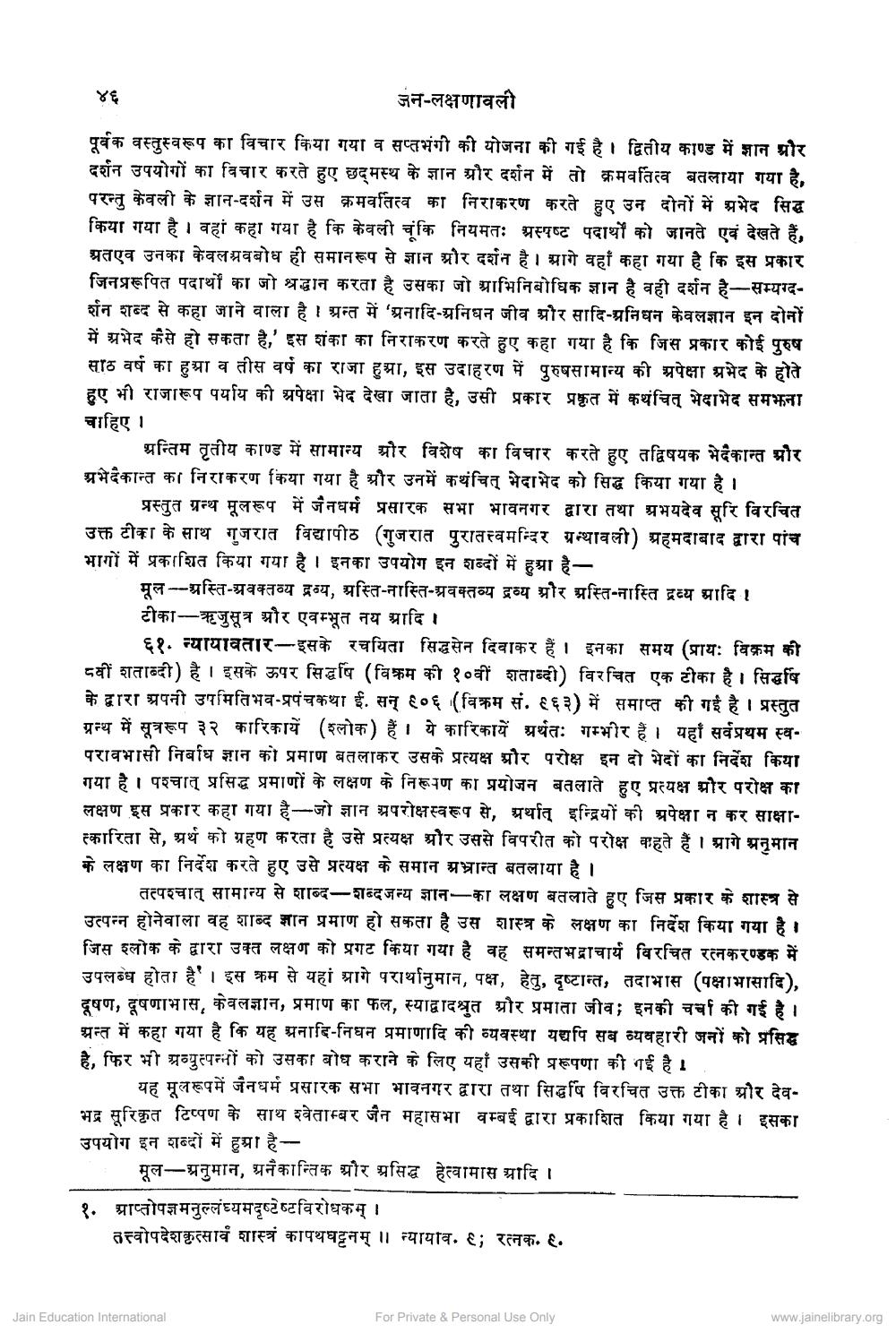________________
जन-लक्षणावली
पूर्वक वस्तुस्वरूप का विचार किया गया व सप्तभंगी की योजना की गई है। द्वितीय काण्ड में ज्ञान और दर्शन उपयोगों का विचार करते हुए छमस्थ के ज्ञान और दर्शन में तो क्रमवर्तित्व बतलाया गया है, परन्तु केवली के ज्ञान-दर्शन में उस क्रमवर्तित्व का निराकरण करते हुए उन दोनों में अभेद सिद्ध किया गया है। वहां कहा गया है कि केवली चूंकि नियमतः अस्पष्ट पदार्थों को जानते एवं देखते हैं, अतएव उनका केवलप्रवबोध ही समानरूप से ज्ञान और दर्शन है। आगे वहाँ कहा गया है कि इस प्रकार जिनप्ररूपित पदार्थों का जो श्रद्धान करता है उसका जो आभिनिबोधिक ज्ञान है वही दर्शन है-सम्यग्दर्शन शब्द से कहा जाने वाला है। अन्त में 'अनादि-अनिधन जीव और सादि-अनिधन केवलज्ञान इन दोनों में अभेद कैसे हो सकता है, इस शंका का निराकरण करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष साठ वर्ष का हुआ व तीस वर्ष का राजा हुआ, इस उदाहरण में पुरुषसामान्य की अपेक्षा अभेद के होते हए भी राजारूप पर्याय की अपेक्षा भेद देखा जाता है, उसी प्रकार प्रकृत में कथंचित् भेदाभेद समझना चाहिए।
अन्तिम ततीय काण्ड में सामान्य और विशेष का विचार करते हए तद्विषयक भेदकान्त और अभेदैकान्त का निराकरण किया गया है और उनमें कथंचित् भेदाभेद को सिद्ध किया गया है।।
प्रस्तुत ग्रन्थ मूलरूप में जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा अभयदेव सूरि विरचित उक्त टीका के साथ गुजरात विद्यापीठ (गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर ग्रन्थावली) अहमदाबाद द्वारा पांच भागों में प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन शब्दों में हुआ है
मूल --अस्ति-प्रवक्तव्य द्रव्य, अस्ति-नास्ति-प्रवक्तव्य द्रव्य और अस्ति-नास्ति द्रव्य आदि । टीका-ऋजुसूत्र और एवम्भूत नय आदि ।
६१. न्यायावतार-इसके रचयिता सिद्धसेन दिवाकर हैं। इनका समय (प्रायः विक्रम की ८वीं शताब्दी) है । इसके ऊपर सिद्धषि (विक्रम की १०वीं शताब्दी) विरचित एक टीका है। सिद्धर्षि के द्वारा अपनी उपमितिभव-प्रपंचकथा ई. सन् ६०६ (विक्रम सं. ६६३) में समाप्त की गई है । प्रस्तुत ग्रन्थ में सूत्ररूप ३२ कारिकायें (श्लोक) हैं। ये कारिकायें अर्थतः गम्भीर हैं। यहाँ सर्वप्रथम स्वपरावभासी निधि ज्ञान को प्रमाण बतलाकर उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदों का निर्देश किया गया है। पश्चात् प्रसिद्ध प्रमाणों के लक्षण के निरूपण का प्रयोजन बतलाते हए प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण इस प्रकार कहा गया है-जो ज्ञान अपरोक्षस्वरूप से, अर्थात् इन्द्रियों की अपेक्षा न कर साक्षास्कारिता से, अर्थ को ग्रहण करता है उसे प्रत्यक्ष और उससे विपरीत को परोक्ष कहते हैं । आगे अनुमान के लक्षण का निर्देश करते हुए उसे प्रत्यक्ष के समान अभ्रान्त बतलाया है।
तत्पश्चात् सामान्य से शाब्द-शब्दजन्य ज्ञान का लक्षण बतलाते हए जिस प्रकार के शास्त्र से उत्पन्न होनेवाला वह शाब्द ज्ञान प्रमाण हो सकता है उस शास्त्र के लक्षण का निर्देश किया गया है। जिस श्लोक के द्वारा उक्त लक्षण को प्रगट किया गया है वह समन्तभद्राचार्य विरचित रत्नकरण्डक में उपलब्ध होता है। इस क्रम से यहां आगे परार्थानुमान, पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, तदाभास (पक्षाभासादि), दृषण, दूषणाभास, केवलज्ञान, प्रमाण का फल, स्याद्वादश्रुत और प्रमाता जीव; इनकी चर्चा की गई है। अन्त में कहा गया है कि यह अनादि-निधन प्रमाणादि की व्यवस्था यद्यपि सब व्यवहारी जनों को प्रसिद्ध है. फिर भी अव्युत्पन्नों को उसका बोध कराने के लिए यहाँ उसकी प्ररूपणा की गई है।
यह मूलरूपमें जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा सिद्धर्षि विरचित उक्त टीका और देवभद्र सरिकृत टिप्पण के साथ श्वेताम्बर जैन महासभा वम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुअा है
___ मूल-अनुमान, अनैकान्तिक और प्रसिद्ध हेत्वामास प्रादि । १. प्राप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।
तत्त्वोपदेशकृत्सा शास्त्रं कापथघट्टनम् ।। न्यायाव. रत्नक. ६.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org