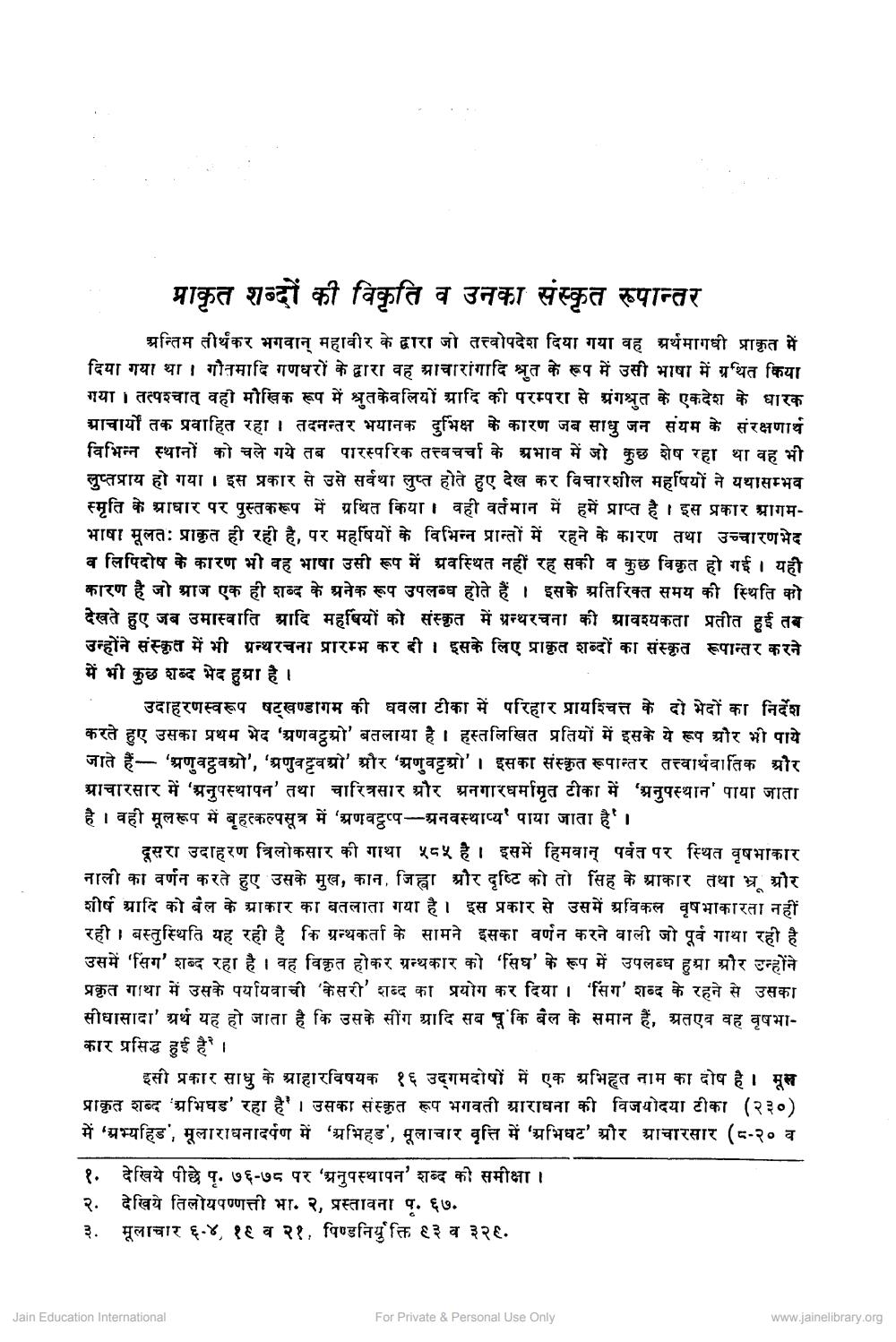________________
प्राकृत शब्दों की विकृति व उनका संस्कृत रूपान्तर
अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के द्वारा जो तत्त्वोपदेश दिया गया वह अर्थमागधी प्राकृत में दिया गया था । गौतमादि गणधरों के द्वारा वह आचारांगादि श्रुत के रूप में उसी भाषा में ग्रथित किया गया । तत्पश्चात् वही मौखिक रूप में श्रुतकेवलियों आदि की परम्परा से अंगश्रुत के एकदेश के धारक आचार्यों तक प्रवाहित रहा । तदनन्तर भयानक दुर्भिक्ष के कारण जब साधु जन संयम के संरक्षणार्थ विभिन्न स्थानों को चले गये तब पारस्परिक तत्त्वचर्चा के प्रभाव में जो कुछ शेष रहा था वह भी लुप्तप्राय हो गया । इस प्रकार से उसे सर्वथा लुप्त होते हुए देख कर विचारशील महर्षियों ने यथासम्भव स्मृति के आधार पर पुस्तकरूप में ग्रथित किया । वही वर्तमान में हमें प्राप्त । इस प्रकार श्रागमभाषा मूलत: प्राकृत ही रही है, पर महर्षियों के विभिन्न प्रान्तों में रहने के कारण तथा उच्चारणभेद व लिपिदोष के कारण भी वह भाषा उसी रूप में अवस्थित नहीं रह सकी व कुछ विकृत हो गई । यही कारण है जो आज एक ही शब्द के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं । इसके अतिरिक्त समय की स्थिति को देखते हुए जब उमास्वाति आदि महर्षियों को संस्कृत में ग्रन्थरचना की आवश्यकता प्रतीत हुई तब उन्होंने संस्कृत में भी ग्रन्थरचना प्रारम्भ कर दी । इसके लिए प्राकृत शब्दों का संस्कृत रूपान्तर करने में भी कुछ शब्द भेद हुग्रा है ।
उदाहरणस्वरूप षट्खण्डागम की घवला टीका में परिहार प्रायश्चित्त के दो भेदों का निर्देश करते हुए उसका प्रथम भेद 'अणवटु' बतलाया है । हस्तलिखित प्रतियों में इसके ये रूप और भी पाये जाते हैं- 'अणुवटुवनो', 'अणुवट्टवओो' और 'अणुवट्टो' । इसका संस्कृत रूपान्तर तत्त्वार्थवार्तिक और प्रचारसार में 'अनुपस्थापन' तथा चारित्रसार और अनगारधर्मामृत टीका में 'अनुपस्थान' पाया जाता है । वही मूलरूप में बृहत्कल्पसूत्र में 'अणवटुप्प - श्रनवस्थाप्य' पाया जाता है ।
दूसरा उदाहरण त्रिलोकसार की गाथा ५८५ है । इसमें हिमवान् पर्वत पर स्थित वृषभाकार नाली का वर्णन करते हुए उसके मुख, कान, जिह्वा और दृष्टि को तो सिंह के आकार तथा भ्रू और शीर्ष आदि को बैल के आकार का बतलाता गया है। इस प्रकार से उसमें अविकल वृषभाकारता नहीं रही । बस्तुस्थिति यह रही है कि ग्रन्थकर्ता के सामने इसका वर्णन करने वाली जो पूर्व गाथा रही है उसमें 'सिंग' शब्द रहा है। वह विकृत होकर ग्रन्थकार को 'सिंघ' के रूप में उपलब्ध हुआ और उन्होंने प्रकृत गाथा में उसके पर्यायवाची 'केसरी' शब्द का प्रयोग कर दिया। 'सिंग' शब्द के रहने से उसका सीधासादा' अर्थ यह हो जाता है कि उसके सींग आदि सब चूंकि बैल के समान हैं, अतएव वह वृषभाकार प्रसिद्ध हुई है ।
इसी प्रकार साधु के प्राहारविषयक १६ उद्गमदोषों में एक अभिहृत नाम का दोष है । मूल प्राकृत शब्द 'अभिघड' रहा है । उसका संस्कृत रूप भगवती आराधना की विजयोदया टीका ( २३० ) 'ह', मूलाराधनादर्पण में 'अभिहड', मूलाचार वृत्ति में 'अभिघट' और प्रचारसार ( ८-२० व
१. देखिये पीछे पृ. ७६-७८ पर 'अनुपस्थापन' शब्द की समीक्षा |
२.
देखिये तिलोय पण्णत्ती भा. २, प्रस्तावना पू. ६७.
३. मूलाचार ६-४, १६ व २१, पिण्डनिर्युक्ति ९३ व ३२६.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org