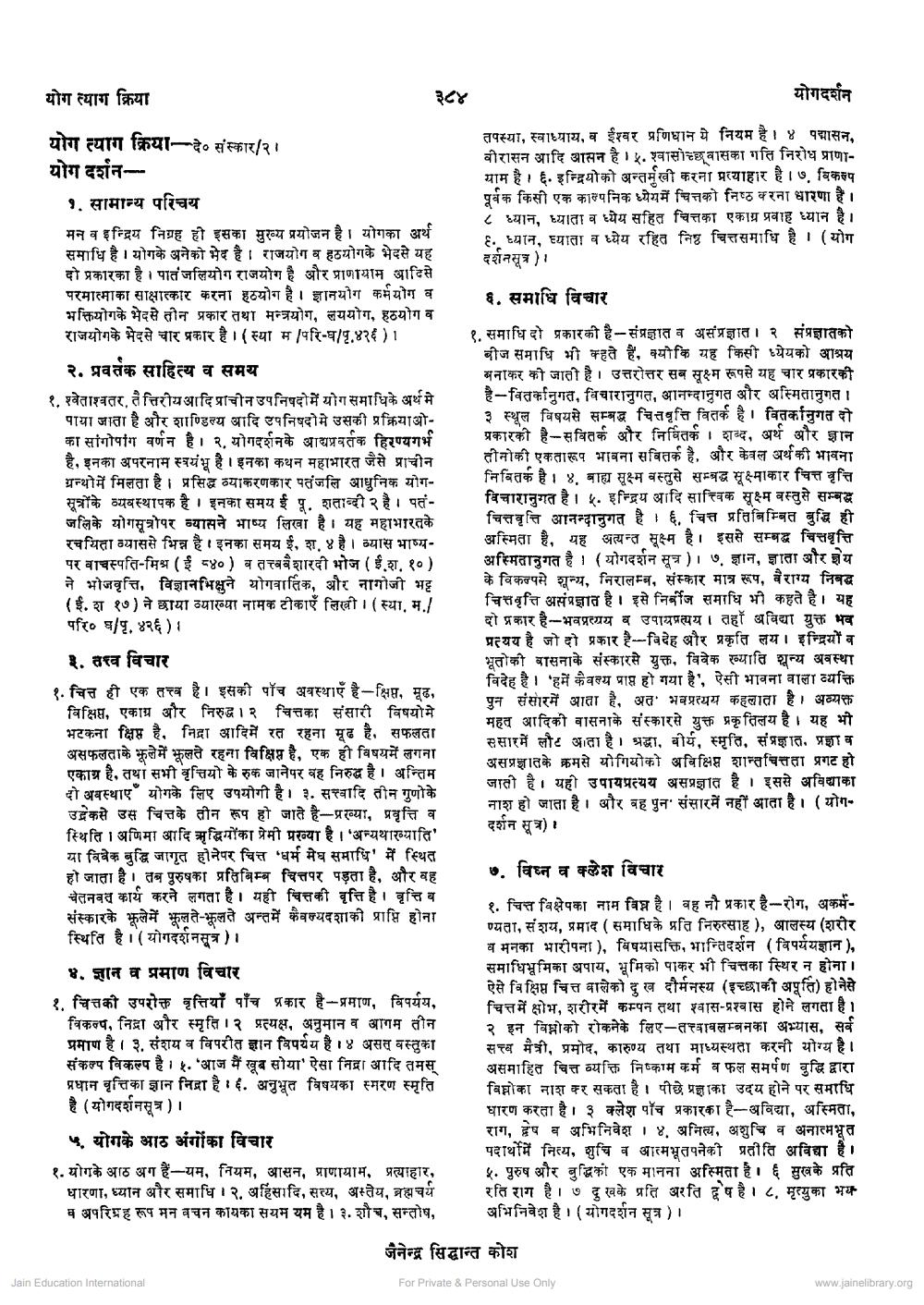________________
योग त्याग क्रिया
३८४
योगदर्शन
तपस्या, स्वाध्याय, व ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। ४ पद्मासन, वीरासन आदि आसन है। ५. श्वासोच्छवासका गति निरोध प्राणायाम है। ६. इन्द्रियोको अन्तर्मुखी करना प्रत्याहार है । ७. विकल्प पूर्वक किसी एक काल्पनिक ध्येयमें चित्तको निष्ठ करना धारणा है । ८ ध्यान, ध्याता व ध्येय सहित चित्तका एकाग्र प्रवाह ध्यान है। १. ध्यान, ध्याता व ध्येय रहित निष्ठ चित्तसमाधि है । (योग दर्शनसूत्र )।
योग त्याग क्रिया-दे० संस्कार/२। योग दर्शन
१. सामान्य परिचय मन व इन्द्रिय निग्रह ही इसका मुख्य प्रयोजन है। योगका अर्थ समाधि है । योगके अनेको भेद है। राजयोग व हठयोगके भेदसे यह दो प्रकारका है । पातंजलियोग राजयोग है और प्राणायाम आदिसे परमात्माका साक्षात्कार करना हठयोग है। ज्ञानयोग कर्म योग व भक्तियोगके भेदसे तीन प्रकार तथा मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग व राजयोगके भेदसे चार प्रकार है। (स्या म /परि-ध/पृ.४२६) ।
२. प्रवर्तक साहित्य व समय १. श्वेताश्वतर, तैत्तिरीय आदि प्राचीन उपनिषदोमें योग समाधिके अर्थ मे पाया जाता है और शाण्डित्य आदि उपनिषदोमे उसकी प्रक्रियाओका सांगोपांग वर्णन है। २. योगदर्शनके आद्यप्रवर्तक हिरण्यगर्भ है, इनका अपरनाम स्वयंभू है । इनका कथन महाभारत जैसे प्राचीन ग्रन्थोमें मिलता है। प्रसिद्ध व्याकरणकार पतंजलि आधुनिक योगसूत्रोंके व्यवस्थापक है । इनका समय ई पू. शताब्दी २ है। पतंजलिके योगसूत्रोपर व्यासने भाष्य लिखा है। यह महाभारतके रचयिता व्याससे भिन्न है। इनका समय ई, श.४ है। व्यास भाष्यपर वाचस्पति-मिश्र (ई ८४०) व तत्त्ववैशारदी भोज (ई.श. १०) ने भोजवृत्ति, विज्ञानभिक्षुने योगवार्तिक, और नागोजी भट्ट (ई. श १७) ने छाया व्याख्या नामक टीकाएँ लिखी। (स्या. म./ परि० घ/पृ. ४२६)
३. तत्व विचार १. चित्त ही एक तत्त्व है। इसकी पॉच अवस्थाएँ है-क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । २ चित्तका संसारी विषयोमे भटकना क्षिप्त है, निद्रा आदिमें रत रहना मूढ है, सफलता असफलताके झूले में झूलते रहना विक्षिप्त है, एक ही विषयमें लगना एकाग्र है, तथा सभी वृत्तियो के रुक जानेपर वह निरुद्ध है। अन्तिम दो अवस्थाए योगके लिए उपयोगी है। ३. सत्त्वादि तीन गुणोके उद्रेकसे उस चित्त के तीन रूप हो जाते है-प्रख्या, प्रवृत्ति व स्थिति । अणिमा आदि ऋद्धियोंका प्रेमी प्ररव्या है । अन्यथाख्याति' या विवेक बुद्धि जागृत होनेपर चित्त 'धर्म मेघ समाधि' में स्थित हो जाता है। तब पुरुषका प्रतिबिम्ब चित्तपर पड़ता है, और वह चेतनबत कार्य करने लगता है। यही चित्तकी वृत्ति है। वृत्ति व संस्कारके झूलेमें झूलते-झूलते अन्त में कैवल्यदशाकी प्राप्ति होना स्थिति है । ( योगदर्शनसूत्र )।
४. ज्ञान व प्रमाण विचार १. चित्तको उपरोक्त वृत्तियाँ पाँच प्रकार है-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । २ प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम तीन प्रमाण है। ३. संशय व विपरीत ज्ञान विपर्यय है। ४ असत वस्तुका संकल्प विकल्प है। १. 'आज मैं खूब सोया' ऐसा निद्रा आदि तमस् प्रधान वृत्तिका ज्ञान निद्रा है । ६. अनुभूत विषयका स्मरण स्मृति है (योगदर्शनसूत्र )।
५. योगके आठ अंगोंका विचार १. योगके आठ अग हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । २. अहिंसादि, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य घ अपरिग्रह रूप मन वचन कायका सयम यम है। ३. शौच, सन्तोष,
६. समाधि विचार १. समाधि दो प्रकार की है-संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात। २ संप्रज्ञातको बीज समाधि भी कहते हैं, क्योकि यह किसी ध्येयको आश्रय मनाकर की जाती है। उत्तरोत्तर सब सूक्ष्म रूपसे यह चार प्रकारकी है-वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत । ३ स्थूल विषयसे सम्बद्ध चित्तवृत्ति वितर्क है। वितर्कानगत दो प्रकारकी है-सवितर्क और निर्वितर्क । शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनोकी एकतारूप भावना सवितर्क है, और केवल अर्थ की भावना निवितक है। ४. बाह्य सूक्ष्म वस्तुसे सम्बद्ध सूक्ष्माकार चित्त वृत्ति विचारानुगत है। १. इन्द्रिय आदि सात्त्विक सूक्ष्म वस्तुसे सम्बद्ध चित्तवृत्ति आनन्दानुगत है । ६. चित्त प्रतिबिम्बित बुद्धि ही अस्मिता है, यह अत्यन्त सूक्ष्म है। इससे सम्बद्ध चित्तवृत्ति अस्मितानुगत है । ( योगदर्शन सूत्र )। ७. ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के विकल्पसे शून्य, निरालम्ब, संस्कार मात्र रूप, वैराग्य निबद्ध चित्तवृत्ति असंप्रज्ञात है। इसे निर्बीज समाधि भी कहते है। यह दो प्रकार है-भवप्रत्यय व उपायप्रत्यय । तहाँ अविद्या युक्त भव प्रत्यय है जो दो प्रकार है--विदेह और प्रकृति लय। इन्द्रियों व भूतोकी बासनाके संस्कारसे युक्त, विवेक ख्याति शून्य अवस्था विदेह है। हमें कैवल्य प्राप्त हो गया है', ऐसी भावना वाला व्यक्ति पुन संसारमें आता है, अत' भवप्रत्यय कहलाता है। अव्यक्त महत आदिकी वासनाके संस्कारसे युक्त प्रकृतिलय है। यह भी ससारमें लौट आता है। श्रद्धा, बीर्य, स्मृति, संप्रज्ञात, प्रज्ञा व असप्रज्ञातके क्रमसे योगियोको अविक्षिप्त शान्तचित्तता प्रगट हो जाती है। यही उपायप्रत्यय असप्रज्ञात है । इससे अविद्याका नाश हो जाता है। और वह पुन संसारमें नहीं आता है। ( योगदर्शन सूत्र)।
७. विघ्न व क्लेश विचार १. चित्त विक्षेपका नाम विघ्न है। वह नौ प्रकार है-रोग, अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद ( समाधिके प्रति निरुत्साह ), आलस्य (शरीर व मनका भारीपना), विषयासक्ति, भान्तिदर्शन (विपर्ययज्ञान), समाधिभूमिका अपाय, भूमिको पाकर भी चित्तका स्थिर न होना। ऐसे विक्षिप्त चित्त बालेको दुख दौर्मनस्य (इच्छाकी अपूर्ति) होनेसे चित्त में क्षोभ, शरीरमें कम्पन तथा श्वास-प्रश्वास होने लगता है। २ इन विघ्नोको रोकनेके लिए-तत्त्वावलम्बनका अभ्यास, सर्व सत्त्व मैत्री, प्रमोद, कारुण्य तथा माध्यस्थता करनी योग्य है। असमाहित चित्त व्यक्ति निष्काम कर्म व फल समर्पण वुद्धि द्वारा विनोका नाश कर सकता है। पीछे प्रज्ञाका उदय होने पर समाधि धारण करता है। ३ क्लेश पॉच प्रकारका है-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश । ४. अनित्य, अशुचि व अनात्मभूत पदार्थोमें नित्य, शुचि व आत्मभूतपनेकी प्रतीति अविद्या है। ५. पुरुष और बुद्धिको एक मानना अस्मिता है। ६ सुखके प्रति रति राग है। ७ दुखके प्रति अरति द्वेष है। ८. मृत्युका भय अभिनिवेश है। (योगदर्शन सूत्र ) ।
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org