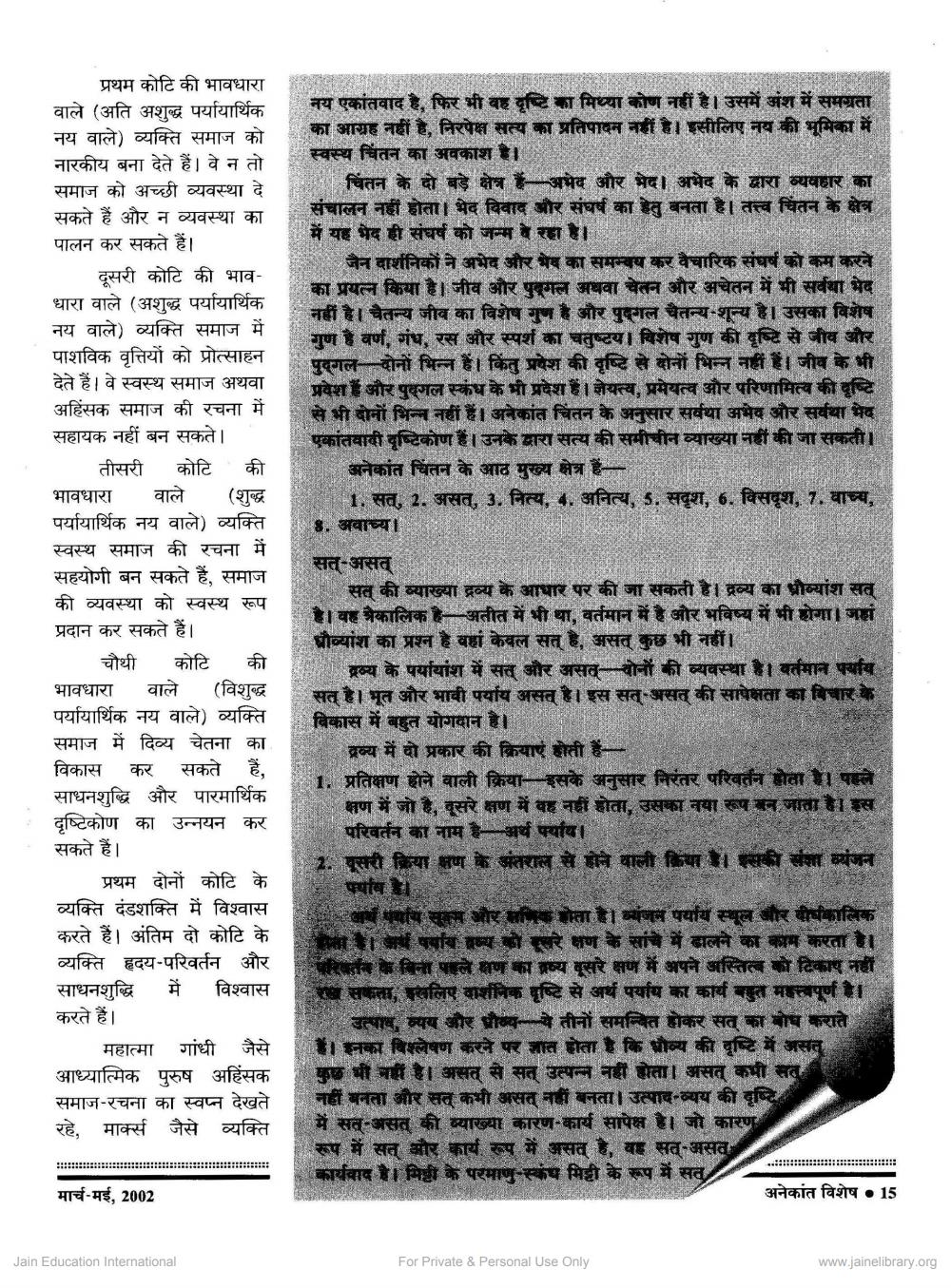________________
प्रथम कोटि की भावधारा वाले (अति अशुद्ध पर्यायार्थिक नय वाले) व्यक्ति समाज को नारकीय बना देते हैं। वे न तो समाज को अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं और न व्यवस्था का पालन कर सकते हैं।
दूसरी कोटि की भावधारा वाले (अशुद्ध पर्यायार्थिक नय वाले) व्यक्ति समाज में पाशविक वृत्तियों को प्रोत्साहन देते हैं। वे स्वस्थ समाज अथवा अहिंसक समाज की रचना में सहायक नहीं बन सकते।
तीसरी कोटि की भावधारा वाले (शुद्ध पर्यायार्थिक नय वाले) व्यक्ति स्वस्थ समाज की रचना में सहयोगी बन सकते हैं, समाज की व्यवस्था को स्वस्थ रूप प्रदान कर सकते हैं।
चौथी कोटि की भावधारा वाले (विशुद्ध पर्यायार्थिक नय वाले) व्यक्ति समाज में दिव्य चेतना का विकास कर सकते हैं, साधनशुद्धि और पारमार्थिक दृष्टिकोण का उन्नयन कर सकते हैं।
प्रथम दोनों कोटि के व्यक्ति दंडशक्ति में विश्वास करते हैं। अंतिम दो कोटि के व्यक्ति हृदय-परिवर्तन और साधनशुद्धि में विश्वास करते हैं।
महात्मा गांधी जैसे आध्यात्मिक पुरुष अहिंसक समाज-रचना का स्वप्न देखते रहे, मार्क्स जैसे व्यक्ति
Here नय एकांतवाद है, फिर भी वह दृष्टि का मिथ्या कोण नहीं है। उसमें अंश में समग्रता का आग्रह नहीं है, निरपेक्ष सत्य का प्रतिपादन नहीं है। इसीलिए नय की भूमिका में । स्वस्थ चिंतन का अवकाश है। ON चिंतन के दो बड़े क्षेत्र है-अभेद और भेद। अभेद के द्वारा व्यवहार का
संचालन नहीं होता। भेद विवाद और संघर्ष का हेतु बनता है। तत्त्व चिंतन के क्षेत्र में यह भेद ही संघर्ष को जन्म दे रहा है।
जैन दार्शनिकों ने अभेद और मेव का समन्वय कर वैचारिक संघर्ष को कम करने का प्रयत्न किया है। जीव और पबगल अथवा चेतन और अचेतन में भी सर्वथा भेद नहीं है। चैतन्य जीव का विशेष गुण है और पुद्गल चैतन्य-शून्य है। उसका विशेष गुण है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का चतुष्टया विशेष गुण की दृष्टि से जीव और पुद्गल-दोनों भिन्न है। किंतु प्रवेश की दृष्टि से दोनों भिन्न नहीं है। जीव के भी प्रदेश और पुग़ल स्कंध के भी प्रदेश है। जेयत्य, प्रमेयत्व और परिणामित्व की दृष्टि से भी दोनों भिन्न नहीं हैं। अनेकांत चितन के अनुसार सर्वथा अभेद और सर्वथा मेव एकांतवावी दृष्टिकोण हैं। उनके द्वारा सत्य की समीचीन व्याख्या नहीं की जा सकती।
अनेकांत चिंतन के आठ मुख्य क्षेत्र है1. सत, 2. असत्, 3. नित्य, 4. अनित्य, 5. सदृश, 6. विसदृश, 7. वाच्य, अवाच्या न-असत्
सत् की व्याख्या द्रव्य के आधार पर की जा सकती है। द्रव्य का प्रौव्यांश सत् है। वह अकालिक है-अतीत में भी था, वर्तमान में है और भविष्य में भी होगा। जहां प्रौव्यांश का प्रश्न है वहां केवल सत् है, असत् कुछ भी नहीं।
द्रव्य के पर्यायांश में सत् और असत् दोनों की व्यवस्था है। वर्तमान पर्याय सत है। भूत और भावी पर्याय असत है। इस सत्-असत् की सापेक्षता का विचार के । विकास में बहुत योगदान है।
द्रव्य में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैप्रतिक्षण होने वाली क्रिया इसके अनुसार निरंतर परिवर्तन होता है। क्षण में जो है, दूसरे क्षण में वह नहीं होता, उसका नया रूप बन जाता है। इस
परिवर्तन का नाम है- अर्थ पाय। 2. दूसरी किया क्षण के अंतराल से होने वाली किया गसकी संमा व्यंजन
कवि सकस और मषिोता है। व्यंजन पर्याय स्कूल और दीर्घकालिक ना।। जय पर्याय वज्य को रखरे क्षण के सांचे में डालने का काम करता है। परिवर्तन के बिना पहले सण का तव्य बसरे क्षण में अपने अस्तित्व को टिकाए नहीं
सकता, इसलिए वार्शनिक दृष्टि से अर्थ पर्याय का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।
उत्पाव, व्यय और प्रौव्यये तीनों समन्वित होकर सत् का बोध कराते । इनका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि धौव्य की दृष्टि में असत
भी नहीं है। असत से सत् उत्पन्न नहीं होता। असत् कभी सत ही बनता और सत् कभी असत नहीं बनता। उत्पाद-व्यय की दृष्टि में सत-असत की व्याख्या कारण-कार्य सापेक्ष है। जो कारण रूप में सत् और कार्य रूप में असत् है, वह सत्-असत कार्यवाद है। मिट्टी के परमाण-स्कंध मिट्टी के रूप में सता
अनेकांत विशेष.15
मार्च-मई, 2002
Hd SAMAND
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org