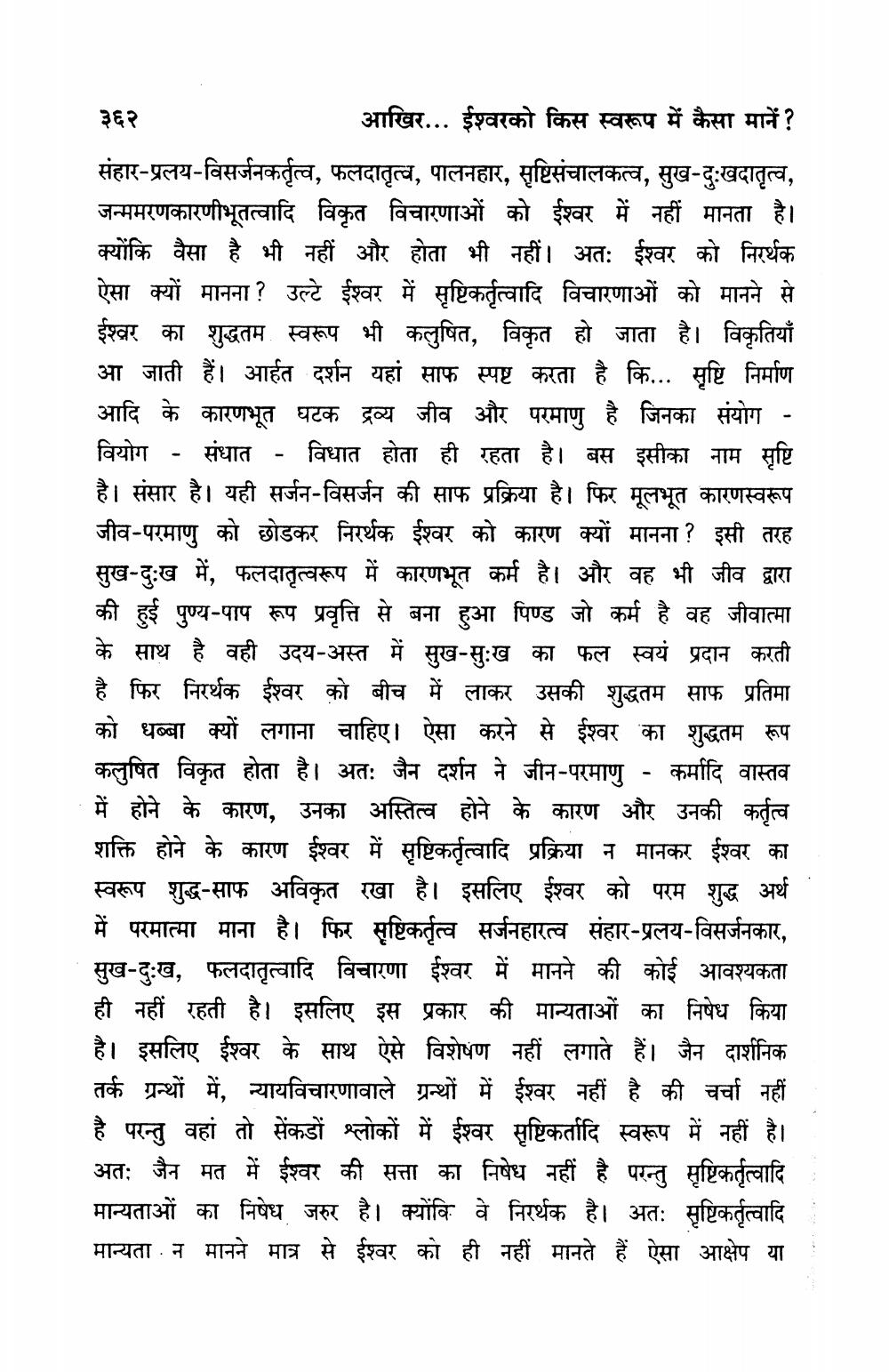________________ 362 आखिर... ईश्वरको किस स्वरूप में कैसा माने? संहार-प्रलय-विसर्जनकर्तृत्व, फलदातृत्व, पालनहार, सृष्टिसंचालकत्व, सुख-दुःखदातृत्व, जन्ममरणकारणीभूतत्वादि विकृत विचारणाओं को ईश्वर में नहीं मानता है। ऐसा क्यों मानना? उल्टे ईश्वर में सृष्टिकर्तृत्वादि विचारणाओं को मानने से ईश्वर का शुद्धतम स्वरूप भी कलुषित, विकृत हो जाता है। विकृतियाँ आ जाती हैं। आर्हत दर्शन यहां साफ स्पष्ट करता है कि... सृष्टि निर्माण आदि के कारणभूत घटक द्रव्य जीव और परमाणु है जिनका संयोग - वियोग - संधात - विधात होता ही रहता है। बस इसीका नाम सृष्टि है। संसार है। यही सर्जन-विसर्जन की साफ प्रक्रिया है। फिर मूलभूत कारणस्वरूप जीव-परमाणु को छोडकर निरर्थक ईश्वर को कारण क्यों मानना ? इसी तरह सुख-दुःख में, फलदातृत्वरूप में कारणभूत कर्म है। और वह भी जीव द्वारा की हुई पुण्य-पाप रूप प्रवृत्ति से बना हुआ पिण्ड जो कर्म है वह जीवात्मा के साथ है वही उदय-अस्त में सुख-सुःख का फल स्वयं प्रदान करती है फिर निरर्थक ईश्वर को बीच में लाकर उसकी शुद्धतम साफ प्रतिमा को धब्बा क्यों लगाना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर का शुद्धतम रूप कलुषित विकृत होता है। अत: जैन दर्शन ने जीन-परमाणु - कर्मादि वास्तव में होने के कारण, उनका अस्तित्व होने के कारण और उनकी कर्तृत्व शक्ति होने के कारण ईश्वर में सृष्टिकर्तृत्वादि प्रक्रिया न मानकर ईश्वर का स्वरूप शुद्ध-साफ अविकृत रखा है। इसलिए ईश्वर को परम शुद्ध अर्थ में परमात्मा माना है। फिर सृष्टिकर्तृत्व सर्जनहारत्व संहार-प्रलय-विसर्जनकार, सुख-दुःख, फलदातृत्वादि विचारणा ईश्वर में मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसलिए इस प्रकार की मान्यताओं का निषेध किया है। इसलिए ईश्वर के साथ ऐसे विशेषण नहीं लगाते हैं। जैन दार्शनिक तर्क ग्रन्थों में, न्यायविचारणावाले ग्रन्थों में ईश्वर नहीं है की चर्चा नहीं है परन्तु वहां तो सेंकडों श्लोकों में ईश्वर सृष्टिकर्तादि स्वरूप में नहीं है। अत: जैन मत में ईश्वर की सत्ता का निषेध नहीं है परन्तु सृष्टिकर्तृत्वादि मान्यताओं का निषेध जरुर है। क्योंकि वे निरर्थक है। अतः सृष्टिकर्तृत्वादि मान्यता . न मानने मात्र से ईश्वर को ही नहीं मानते हैं ऐसा आक्षेप या