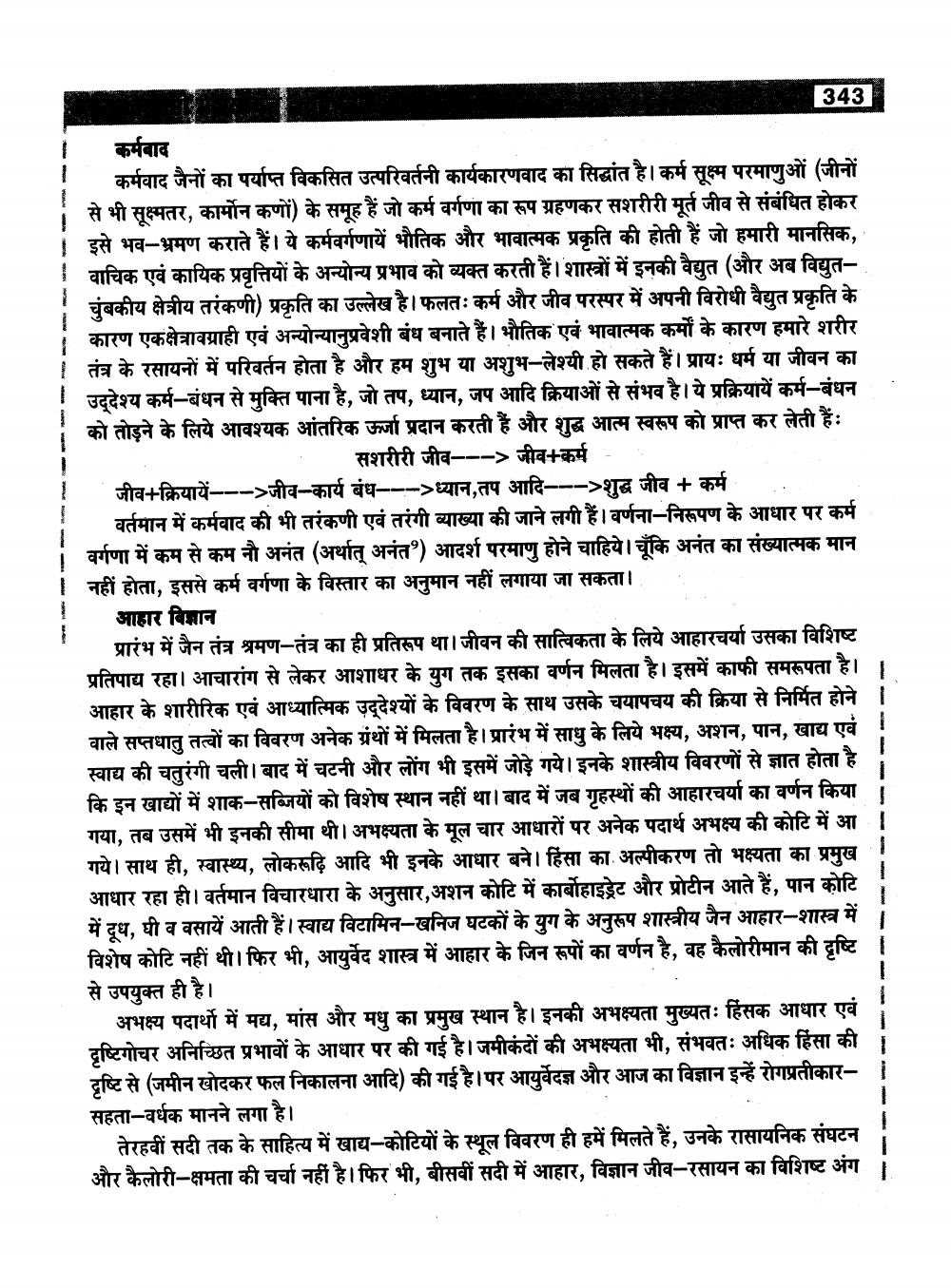________________
3431 । कर्मबाद
कर्मवाद जैनों का पर्याप्त विकसित उत्परिवर्तनी कार्यकारणवाद का सिद्धांत है। कर्म सूक्ष्म परमाणुओं (जीनों से भी सूक्ष्मतर, कार्मोन कणों) के समूह हैं जो कर्म वर्गणा का रूप ग्रहणकर सशरीरी मूर्त जीव से संबंधित होकर इसे भव-भ्रमण कराते हैं। ये कर्मवर्गणायें भौतिक और भावात्मक प्रकृति की होती हैं जो हमारी मानसिक, वाचिक एवं कायिक प्रवृत्तियों के अन्योन्य प्रभाव को व्यक्त करती हैं। शास्त्रों में इनकी वैद्युत (और अब विद्युतचुंबकीय क्षेत्रीय तरंकणी) प्रकृति का उल्लेख है। फलतः कर्म और जीव परस्पर में अपनी विरोधी वैद्युत प्रकृति के
कारण एकक्षेत्रावग्राही एवं अन्योन्यानुप्रवेशी बंध बनाते हैं। भौतिक एवं भावात्मक कर्मों के कारण हमारे शरीर | तंत्र के रसायनों में परिवर्तन होता है और हम शुभ या अशुभ-लेश्यी हो सकते हैं। प्रायः धर्म या जीवन का ! उद्देश्य कर्म-बंधन से मुक्ति पाना है, जो तप, ध्यान, जप आदि क्रियाओं से संभव है। ये प्रक्रियायें कर्म-बंधन को तोड़ने के लिये आवश्यक आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती हैं और शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेती हैं:
सशरीरी जीव---> जीव+कर्म - ___ जीव+क्रियायें--->जीव-कार्य बंध--->ध्यान,तप आदि--->शुद्ध जीव + कर्म .. ___ वर्तमान में कर्मवाद की भी तरंकणी एवं तरंगी व्याख्या की जाने लगी हैं। वर्णना-निरूपण के आधार पर कर्म
वर्गणा में कम से कम नौ अनंत (अर्थात् अनंत) आदर्श परमाणु होने चाहिये। चूँकि अनंत का संख्यात्मक मान | नहीं होता, इससे कर्म वर्गणा के विस्तार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
आहार विज्ञान प्रारंभ में जैन तंत्र श्रमण-तंत्र का ही प्रतिरूप था। जीवन की सात्विकता के लिये आहारचर्या उसका विशिष्ट प्रतिपाय रहा। आचारांग से लेकर आशाधर के युग तक इसका वर्णन मिलता है। इसमें काफी समरूपता है। । आहार के शारीरिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के विवरण के साथ उसके चयापचय की क्रिया से निर्मित होने । वाले सप्तधातु तत्वों का विवरण अनेक ग्रंथों में मिलता है। प्रारंभ में साधु के लिये भक्ष्य, अशन, पान, खाद्य एवं ! स्वाद्य की चतुरंगी चली। बाद में चटनी और लोंग भी इसमें जोड़े गये। इनके शास्त्रीय विवरणों से ज्ञात होता है कि इन खायों में शाक-सब्जियों को विशेष स्थान नहीं था। बाद में जब गृहस्थों की आहारचर्या का वर्णन किया । गया, तब उसमें भी इनकी सीमा थी। अभक्ष्यता के मूल चार आधारों पर अनेक पदार्थ अभक्ष्य की कोटि में आ । गये। साथ ही, स्वास्थ्य, लोकरूढ़ि आदि भी इनके आधार बने। हिंसा का अल्पीकरण तो भक्ष्यता का प्रमुख । आधार रहा ही। वर्तमान विचारधारा के अनुसार,अशन कोटि में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आते हैं, पान कोटि में दूध, घी व वसायें आती हैं। स्वाद्य विटामिन-खनिज घटकों के युग के अनुरूप शास्त्रीय जैन आहार-शास्त्र में विशेष कोटि नहीं थी। फिर भी, आयुर्वेद शास्त्र में आहार के जिन रूपों का वर्णन है, वह कैलोरीमान की दृष्टि से उपयुक्त ही है। __ अभक्ष्य पदार्थो में मद्य, मांस और मधु का प्रमुख स्थान है। इनकी अभक्ष्यता मुख्यतः हिंसक आधार एवं दृष्टिगोचर अनिच्छित प्रभावों के आधार पर की गई है। जमीकंदों की अभक्ष्यता भी, संभवतः अधिक हिंसा की दृष्टि से (जमीन खोदकर फल निकालना आदि) की गई है।पर आयुर्वेदज्ञ और आज का विज्ञान इन्हें रोगप्रतीकार- । सहता-वर्धक मानने लगा है।
तेरहवीं सदी तक के साहित्य में खाद्य-कोटियों के स्थूल विवरण ही हमें मिलते हैं, उनके रासायनिक संघटन और कैलोरी-क्षमता की चर्चा नहीं है। फिर भी, बीसवीं सदी में आहार, विज्ञान जीव-रसायन का विशिष्ट अंग ।