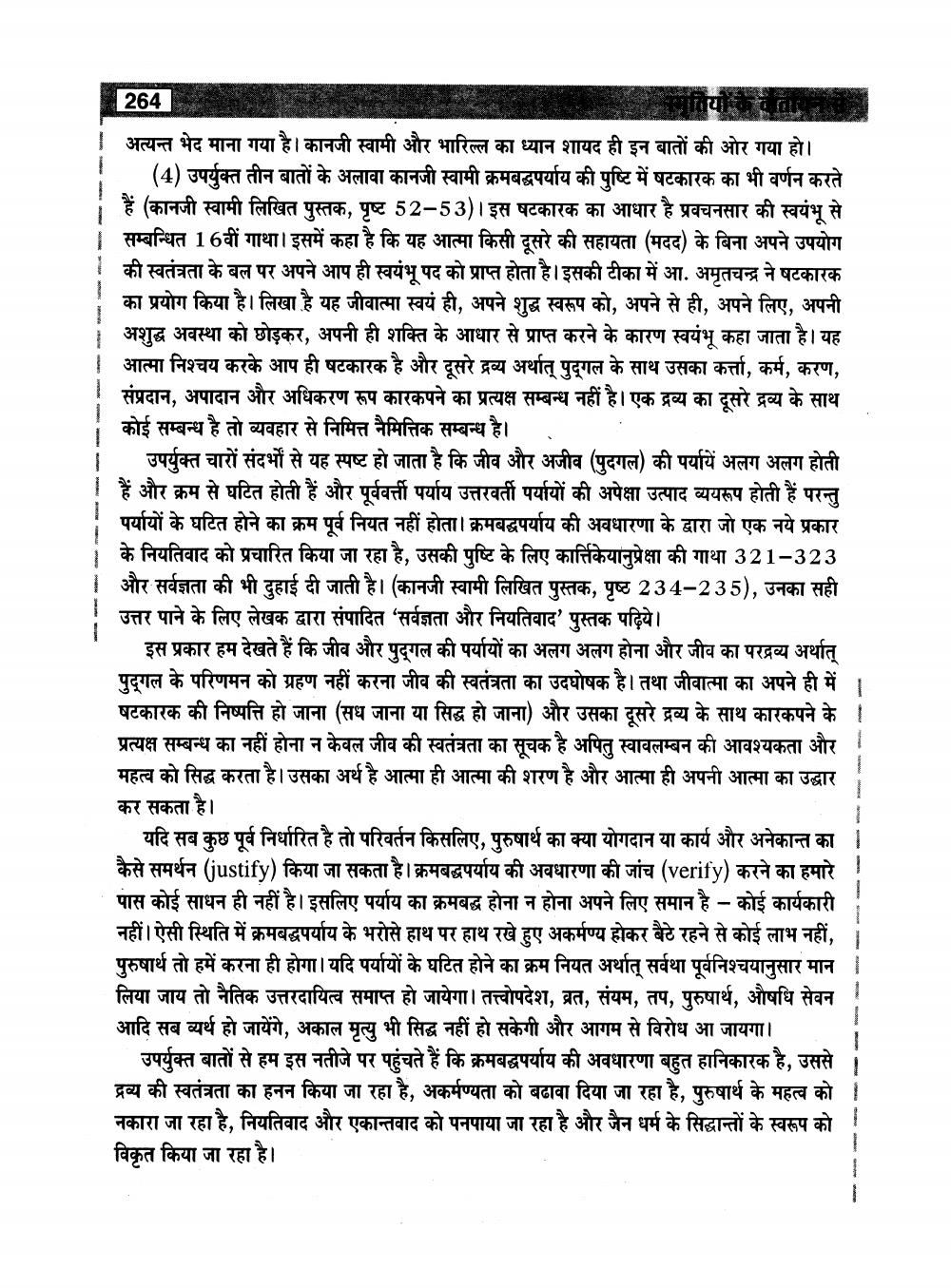________________
264
अत्यन्त भेद माना गया है। कानजी स्वामी और भारिल्ल का ध्यान शायद ही इन बातों की ओर गया हो ।
(4) उपर्युक्त तीन बातों के अलावा कानजी स्वामी क्रमबद्धपर्याय की पुष्टि में षटकारक का भी वर्णन करते हैं ( कानजी स्वामी लिखित पुस्तक, पृष्ट 52-53 ) । इस षटकारक का आधार है प्रवचनसार की स्वयंभू से सम्बन्धित 16वीं गाथा | इसमें कहा है कि यह आत्मा किसी दूसरे की सहायता ( मदद) के बिना अपने उपयोग की स्वतंत्रता के बल पर अपने आप ही स्वयंभू पद को प्राप्त होता है। इसकी टीका में आ. अमृतचन्द्र ने षटकारक का प्रयोग किया है। लिखा है यह जीवात्मा स्वयं ही, अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने से ही, अपने लिए, अपनी अशुद्ध अवस्था को छोड़कर, अपनी ही शक्ति के आधार से प्राप्त करने के कारण स्वयंभू कहा जाता है। यह आमा निश्चय करके आप ही षटकारक है और दूसरे द्रव्य अर्थात् पुद्गल के साथ उसका कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण रूप कारकपने का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई सम्बन्ध है तो व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ।
उपर्युक्त चारों संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव और अजीव (पुदगल) की पर्यायें अलग अलग होती हैं और क्रम से घटित होती हैं और पूर्ववर्त्ती पर्याय उत्तरवर्ती पर्यायों की अपेक्षा उत्पाद व्ययरूप होती हैं परन्तु पर्यायों के घटित होने का क्रम पूर्व नियत नहीं होता । क्रमबद्धपर्याय की अवधारणा के द्वारा जो एक नये प्रकार के नियतिवाद को प्रचारित किया जा रहा है, उसकी पुष्टि के लिए कार्त्तिकेयानुप्रेक्षा की गाथा 321-323 1 और सर्वज्ञता की भी दुहाई दी जाती है। (कानजी स्वामी लिखित पुस्तक, पृष्ठ 234 - 235), उनका सही उत्तर पाने के लिए लेखक द्वारा संपादित 'सर्वज्ञता और नियतिवाद' पुस्तक पढ़िये ।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव और पुद्गल की पर्यायों का अलग अलग होना और जीव का परद्रव्य अर्थात् पुद्गल के परिणमन को ग्रहण नहीं करना जीव की स्वतंत्रता का उदघोषक है। तथा जीवात्मा का अपने ही में षटकारक की निष्पत्ति हो जाना (सध जाना या सिद्ध हो जाना) और उसका दूसरे द्रव्य के साथ कारकपने के प्रत्यक्ष सम्बन्ध का नहीं होना न केवल जीव की स्वतंत्रता का सूचक है अपितु स्वावलम्बन की आवश्यकता और महत्व को सिद्ध करता है। उसका अर्थ है आत्मा ही आत्मा की शरण है और आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है।
1
1
यदि सब कुछ निर्धारित है तो परिवर्तन किसलिए, पुरुषार्थ का क्या योगदान या कार्य और अनेकान्त का कैसे समर्थन (justify) किया जा सकता है। क्रमबद्धपर्याय की अवधारणा की जांच (verify) करने का हमारे पास कोई साधन ही नहीं है। इसलिए पर्याय का क्रमबद्ध होना न होना अपने लिए समान है – कोई कार्यकारी नहीं । ऐसी स्थिति में क्रमबद्धपर्याय के भरोसे हाथ पर हाथ रखे हुए अकर्मण्य होकर बैठे रहने से कोई लाभ नहीं, पुरुषार्थ तो हमें करना ही होगा । यदि पर्यायों के घटित होने का क्रम नियत अर्थात् सर्वथा पूर्वनिश्चयानुसार मान ! लिया जाय तो नैतिक उत्तरदायित्व समाप्त हो जायेगा । तत्त्वोपदेश, व्रत, संयम, तप, पुरुषार्थ, औषधि सेवन आदि सब व्यर्थ हो जायेंगे, अकाल मृत्यु भी सिद्ध नहीं हो सकेगी और आगम से विरोध आ जायगा।
उपर्युक्त बातों से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि क्रमबद्धपर्याय की अवधारणा बहुत हानिकारक है, उससे द्रव्य की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, अकर्मण्यता को बढावा दिया जा रहा है, पुरुषार्थ के महत्व को 1 नकारा जा रहा है, नियतिवाद और एकान्तवाद को पनपाया जा रहा है और जैन धर्म के सिद्धान्तों के स्वरूप को विकृत किया जा रहा है।