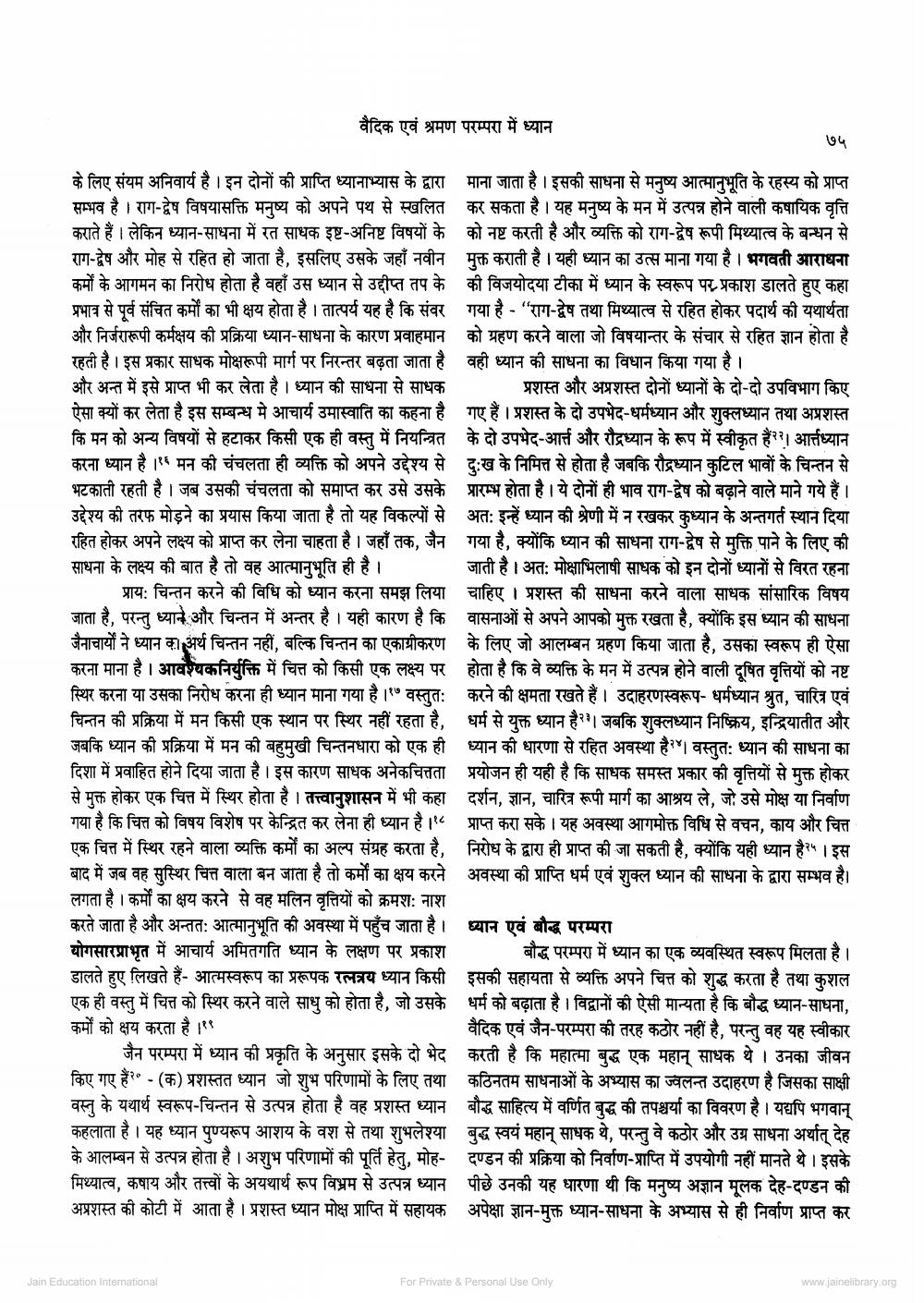________________
वैदिक एवं श्रमण परम्परा में ध्यान
७५
के लिए संयम अनिवार्य है। इन दोनों की प्राप्ति ध्यानाभ्यास के द्वारा माना जाता है। इसकी साधना से मनुष्य आत्मानुभूति के रहस्य को प्राप्त सम्भव है। राग-द्वेष विषयासक्ति मनुष्य को अपने पथ से स्खलित कर सकता है। यह मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली कषायिक वृत्ति कराते हैं । लेकिन ध्यान-साधना में रत साधक इष्ट-अनिष्ट विषयों के को नष्ट करती है और व्यक्ति को राग-द्वेष रूपी मिथ्यात्व के बन्धन से राग-द्वेष और मोह से रहित हो जाता है, इसलिए उसके जहाँ नवीन मुक्त कराती है । यही ध्यान का उत्स माना गया है । भगवती आराधना कमों के आगमन का निरोध होता है वहाँ उस ध्यान से उद्दीप्त तप के की विजयोदया टीका में ध्यान के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा प्रभाव से पूर्व संचित कर्मों का भी क्षय होता है । तात्पर्य यह है कि संवर गया है - "राग-द्वेष तथा मिथ्यात्व से रहित होकर पदार्थ की यथार्थता
और निर्जरारूपी कर्मक्षय की प्रक्रिया ध्यान-साधना के कारण प्रवाहमान को ग्रहण करने वाला जो विषयान्तर के संचार से रहित ज्ञान होता है रहती है । इस प्रकार साधक मोक्षरूपी मार्ग पर निरन्तर बढ़ता जाता है वही ध्यान की साधना का विधान किया गया है।
और अन्त में इसे प्राप्त भी कर लेता है। ध्यान की साधना से साधक प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों ध्यानों के दो-दो उपविभाग किए ऐसा क्यों कर लेता है इस सम्बन्ध मे आचार्य उमास्वाति का कहना है गए हैं । प्रशस्त के दो उपभेद-धर्मध्यान और शुक्लध्यान तथा अप्रशस्त कि मन को अन्य विषयों से हटाकर किसी एक ही वस्तु में नियन्त्रित के दो उपभेद-आर्त और रौद्रध्यान के रूप में स्वीकृत हैं। आर्तध्यान करना ध्यान है ।१६ मन की चंचलता ही व्यक्ति को अपने उद्देश्य से दु:ख के निमित्त से होता है जबकि रौद्रध्यान कुटिल भावों के चिन्तन से भटकाती रहती है । जब उसकी चंचलता को समाप्त कर उसे उसके प्रारम्भ होता है। ये दोनों ही भाव राग-द्वेष को बढ़ाने वाले माने गये हैं। उद्देश्य की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जाता है तो यह विकल्पों से अत: इन्हें ध्यान की श्रेणी में न रखकर कुध्यान के अन्तगर्त स्थान दिया रहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहता है । जहाँ तक, जैन गया है, क्योंकि ध्यान की साधना राग-द्वेष से मुक्ति पाने के लिए की साधना के लक्ष्य की बात है तो वह आत्मानुभूति ही है। जाती है। अत: मोक्षाभिलाषी साधक को इन दोनों ध्यानों से विरत रहना
प्राय: चिन्तन करने की विधि को ध्यान करना समझ लिया चाहिए । प्रशस्त की साधना करने वाला साधक सांसारिक विषय जाता है, परन्तु ध्याने और चिन्तन में अन्तर है। यही कारण है कि वासनाओं से अपने आपको मुक्त रखता है, क्योंकि इस ध्यान की साधना जैनाचार्यों ने ध्यान का अर्थ चिन्तन नहीं, बल्कि चिन्तन का एकाग्रीकरण के लिए जो आलम्बन ग्रहण किया जाता है, उसका स्वरूप ही ऐसा करना माना है । आवश्यकनियुक्ति में चित्त को किसी एक लक्ष्य पर होता है कि वे व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाली दूषित वृत्तियों को नष्ट स्थिर करना या उसका निरोध करना ही ध्यान माना गया है । वस्तुतः करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरणस्वरूप-धर्मध्यान श्रुत, चारित्र एवं चिन्तन की प्रक्रिया में मन किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, धर्म से युक्त ध्यान है। जबकि शुक्लध्यान निष्क्रिय, इन्द्रियातीत और जबकि ध्यान की प्रक्रिया में मन की बहुमुखी चिन्तनधारा को एक ही ध्यान की धारणा से रहित अवस्था है। वस्तुत: ध्यान की साधना का दिशा में प्रवाहित होने दिया जाता है। इस कारण साधक अनेकचित्तता प्रयोजन ही यही है कि साधक समस्त प्रकार की वृत्तियों से मुक्त होकर से मुक्त होकर एक चित्त में स्थिर होता है । तत्त्वानुशासन में भी कहा दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी मार्ग का आश्रय ले, जो उसे मोक्ष या निर्वाण गया है कि चित्त को विषय विशेष पर केन्द्रित कर लेना ही ध्यान है।८ प्राप्त करा सके । यह अवस्था आगमोक्त विधि से वचन, काय और चित्त एक चित्त में स्थिर रहने वाला व्यक्ति कर्मों का अल्प संग्रह करता है, निरोध के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि यही ध्यान है।५ । इस बाद में जब वह सुस्थिर चित्त वाला बन जाता है तो कर्मों का क्षय करने अवस्था की प्राप्ति धर्म एवं शुक्ल ध्यान की साधना के द्वारा सम्भव है। लगता है । कर्मों का क्षय करने से वह मलिन वृत्तियों को क्रमशः नाश करते जाता है और अन्ततः आत्मानुभूति की अवस्था में पहुँच जाता है। ध्यान एवं बौद्ध परम्परा योगसारप्राभृत में आचार्य अमितगति ध्यान के लक्षण पर प्रकाश बौद्ध परम्परा में ध्यान का एक व्यवस्थित स्वरूप मिलता है। डालते हुए लिखते हैं- आत्मस्वरूप का प्ररूपक रलत्रय ध्यान किसी इसकी सहायता से व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करता है तथा कुशल एक ही वस्तु में चित्त को स्थिर करने वाले साधु को होता है, जो उसके धर्म को बढ़ाता है। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि बौद्ध ध्यान-साधना, कर्मों को क्षय करता है ।१९
वैदिक एवं जैन-परम्परा की तरह कठोर नहीं है, परन्तु वह यह स्वीकार जैन परम्परा में ध्यान की प्रकृति के अनुसार इसके दो भेद करती है कि महात्मा बुद्ध एक महान् साधक थे । उनका जीवन किए गए हैं२० - (क) प्रशस्तत ध्यान जो शुभ परिणामों के लिए तथा कठिनतम साधनाओं के अभ्यास का ज्वलन्त उदाहरण है जिसका साक्षी वस्तु के यथार्थ स्वरूप-चिन्तन से उत्पन्न होता है वह प्रशस्त ध्यान बौद्ध साहित्य में वर्णित बुद्ध की तपश्चर्या का विवरण है। यद्यपि भगवान् कहलाता है। यह ध्यान पुण्यरूप आशय के वश से तथा शुभलेश्या बुद्ध स्वयं महान् साधक थे, परन्तु वे कठोर और उग्र साधना अर्थात् देह के आलम्बन से उत्पन्न होता है । अशुभ परिणामों की पूर्ति हेतु, मोह- दण्डन की प्रक्रिया को निर्वाण-प्राप्ति में उपयोगी नहीं मानते थे। इसके मिथ्यात्व, कषाय और तत्त्वों के अयथार्थ रूप विभ्रम से उत्पन्न ध्यान पीछे उनकी यह धारणा थी कि मनुष्य अज्ञान मूलक देह-दण्डन की अप्रशस्त की कोटी में आता है। प्रशस्त ध्यान मोक्ष प्राप्ति में सहायक अपेक्षा ज्ञान-मुक्त ध्यान-साधना के अभ्यास से ही निर्वाण प्राप्त कर
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org