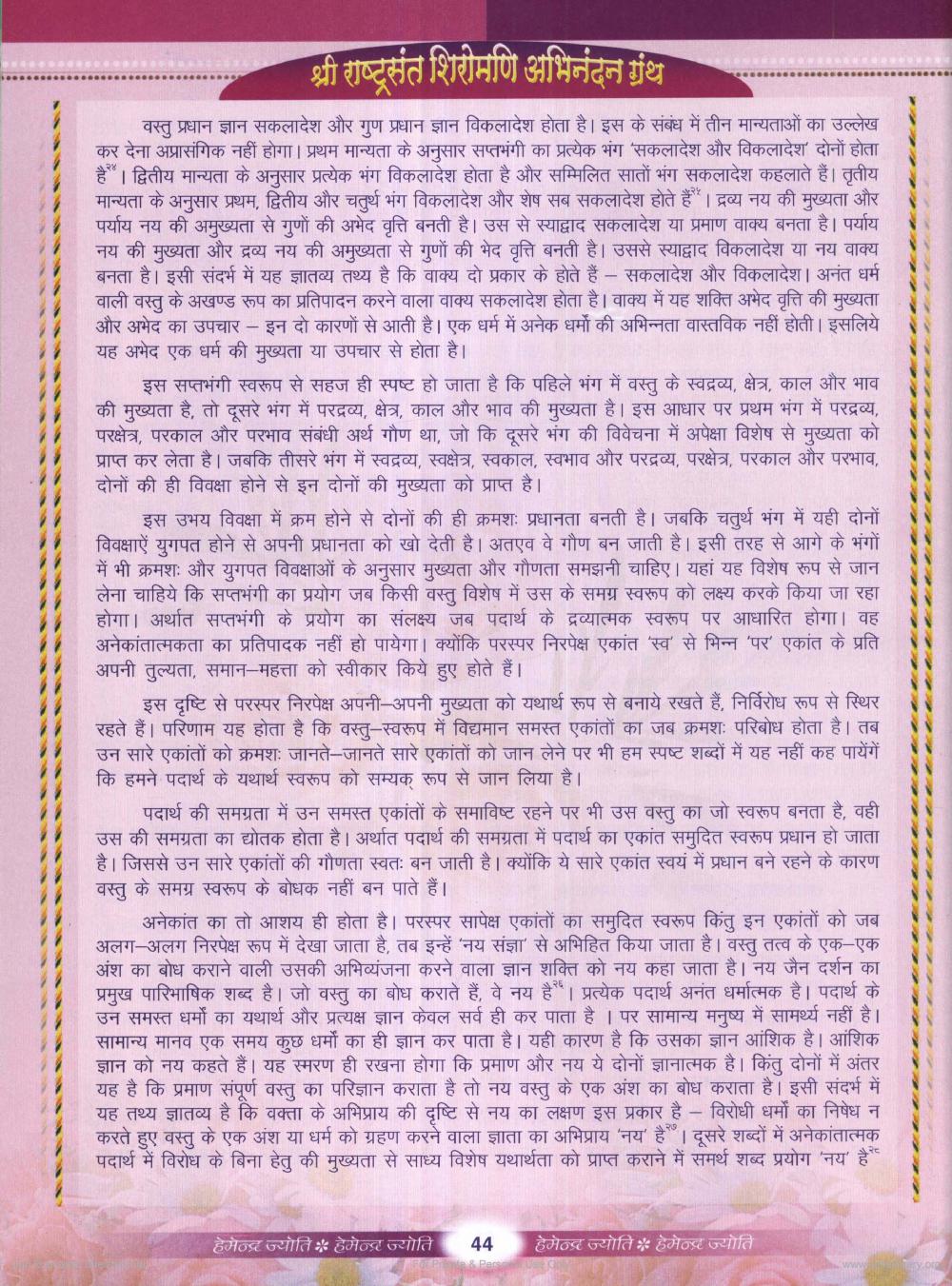________________
श्री राष्ट्रसंत शिरोमणि अभिनंदन ग्रंथ
वस्तु प्रधान ज्ञान सकलादेश और गुण प्रधान ज्ञान विकलादेश होता है। इस के संबंध में तीन मान्यताओं का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा। प्रथम मान्यता के अनुसार सप्तभंगी का प्रत्येक भंग 'सकलादेश और विकलादेश दोनों होता है । द्वितीय मान्यता के अनुसार प्रत्येक भंग विकलादेश होता है और सम्मिलित सातों भंग सकलादेश कहलाते हैं। तृतीय मान्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ भंग विकलादेश और शेष सब सकलादेश होते हैं । द्रव्य नय की मुख्यता और पर्याय नय की अमुख्यता से गुणों की अभेद वृत्ति बनती है। उस से स्याद्वाद सकलादेश या प्रमाण वाक्य बनता है। पर्याय नय की मुख्यता और द्रव्य नय की अमुख्यता से गुणों की भेद वृत्ति बनती है। उससे स्याद्वाद विकलादेश या नय वाक्य बनता है। इसी संदर्भ में यह ज्ञातव्य तथ्य है कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं - सकलादेश और विकलादेश। अनंत धर्म वाली वस्तु के अखण्ड रूप का प्रतिपादन करने वाला वाक्य सकलादेश होता है। वाक्य में यह शक्ति अभेद वृत्ति की मुख्यता
और अभेद का उपचार - इन दो कारणों से आती है। एक धर्म में अनेक धर्मों की अभिन्नता वास्तविक नहीं होती। इसलिये यह अभेद एक धर्म की मुख्यता या उपचार से होता है।
इस सप्तभंगी स्वरूप से सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि पहिले भंग में वस्तु के स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मुख्यता है, तो दूसरे भंग में परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मुख्यता है। इस आधार पर प्रथम भंग में परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव संबंधी अर्थ गौण था, जो कि दूसरे भंग की विवेचना में अपेक्षा विशेष से मुख्यता को प्राप्त कर लेता है। जबकि तीसरे भंग में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव, दोनों की ही विवक्षा होने से इन दोनों की मुख्यता को प्राप्त है।
इस उभय विवक्षा में क्रम होने से दोनों की ही क्रमशः प्रधानता बनती है। जबकि चतुर्थ भंग में यही दोनों विवक्षाएँ युगपत होने से अपनी प्रधानता को खो देती है। अतएव वे गौण बन जाती है। इसी तरह से आगे के भंगों में भी क्रमशः और युगपत विवक्षाओं के अनुसार मुख्यता और गौणता समझनी चाहिए। यहां यह विशेष रूप से जान लेना चाहिये कि सप्तभंगी का प्रयोग जब किसी वस्तु विशेष में उस के समग्र स्वरूप को लक्ष्य करके किया जा रहा होगा। अर्थात सप्तभंगी के प्रयोग का संलक्ष्य जब पदार्थ के द्रव्यात्मक स्वरूप पर आधारित होगा। वह अनेकांतात्मकता का प्रतिपादक नहीं हो पायेगा। क्योंकि परस्पर निरपेक्ष एकांत 'स्व' से भिन्न 'पर' एकांत के प्रति अपनी तुल्यता, समान महत्ता को स्वीकार किये हुए होते हैं।
इस दृष्टि से परस्पर निरपेक्ष अपनी-अपनी मुख्यता को यथार्थ रूप से बनाये रखते हैं, निर्विरोध रूप से स्थिर रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वस्तु-स्वरूप में विद्यमान समस्त एकांतों का जब क्रमशः परिबोध होता है। तब उन सारे एकांतों को क्रमश: जानते-जानते सारे एकांतों को जान लेने पर भी हम स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कह पायेंगें कि हमने पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को सम्यक रूप से जान लिया है।
पदार्थ की समग्रता में उन समस्त एकांतों के समाविष्ट रहने पर भी उस वस्तु का जो स्वरूप बनता है, वही उस की समग्रता का द्योतक होता है। अर्थात पदार्थ की समग्रता में पदार्थ का एकांत समुदित स्वरूप प्रधान हो जाता है। जिससे उन सारे एकांतों की गौणता स्वतः बन जाती है। क्योंकि ये सारे एकांत स्वयं में प्रधान बने रहने के कारण वस्तु के समग्र स्वरूप के बोधक नहीं बन पाते हैं।
अनेकांत का तो आशय ही होता है। परस्पर सापेक्ष एकांतों का समुदित स्वरूप किंतु इन एकांतों को जब अलग-अलग निरपेक्ष रूप में देखा जाता है, तब इन्हें 'नय संज्ञा से अभिहित किया जाता है। वस्तु तत्व के एक-एक अंश का बोध कराने वाली उसकी अभिव्यंजना करने वाला ज्ञान शक्ति को नय कहा जाता है। नय जैन दर्शन का प्रमुख पारिभाषिक शब्द है। जो वस्तु का बोध कराते हैं, वे नय है । प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मात्मक है। पदार्थ के उन समस्त धर्मों का यथार्थ और प्रत्यक्ष ज्ञान केवल सर्व ही कर पाता है । पर सामान्य मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है। सामान्य मानव एक समय कुछ धर्मों का ही ज्ञान कर पाता है। यही कारण है कि उसका ज्ञान आंशिक है। आंशिक ज्ञान को नय कहते हैं। यह स्मरण ही रखना होगा कि प्रमाण और नय ये दोनों ज्ञानात्मक है। किंतु दोनों में अंतर यह है कि प्रमाण संपूर्ण वस्तु का परिज्ञान कराता है तो नय वस्तु के एक अंश का बोध कराता है। इसी संदर्भ में यह तथ्य ज्ञातव्य है कि वक्ता के अभिप्राय की दृष्टि से नय का लक्षण इस प्रकार है - विरोधी धर्मों का निषेध न करते हुए वस्तु के एक अंश या धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय 'नय' है । दूसरे शब्दों में अनेकांतात्मक पदार्थ में विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य विशेष यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ शब्द प्रयोग 'नय' है।
हेमेन्द्र ज्योति * हेमेन्त ज्योति 44 हेमेन्द्र ज्योति* हेमेन्द्र ज्योति
EnKPers