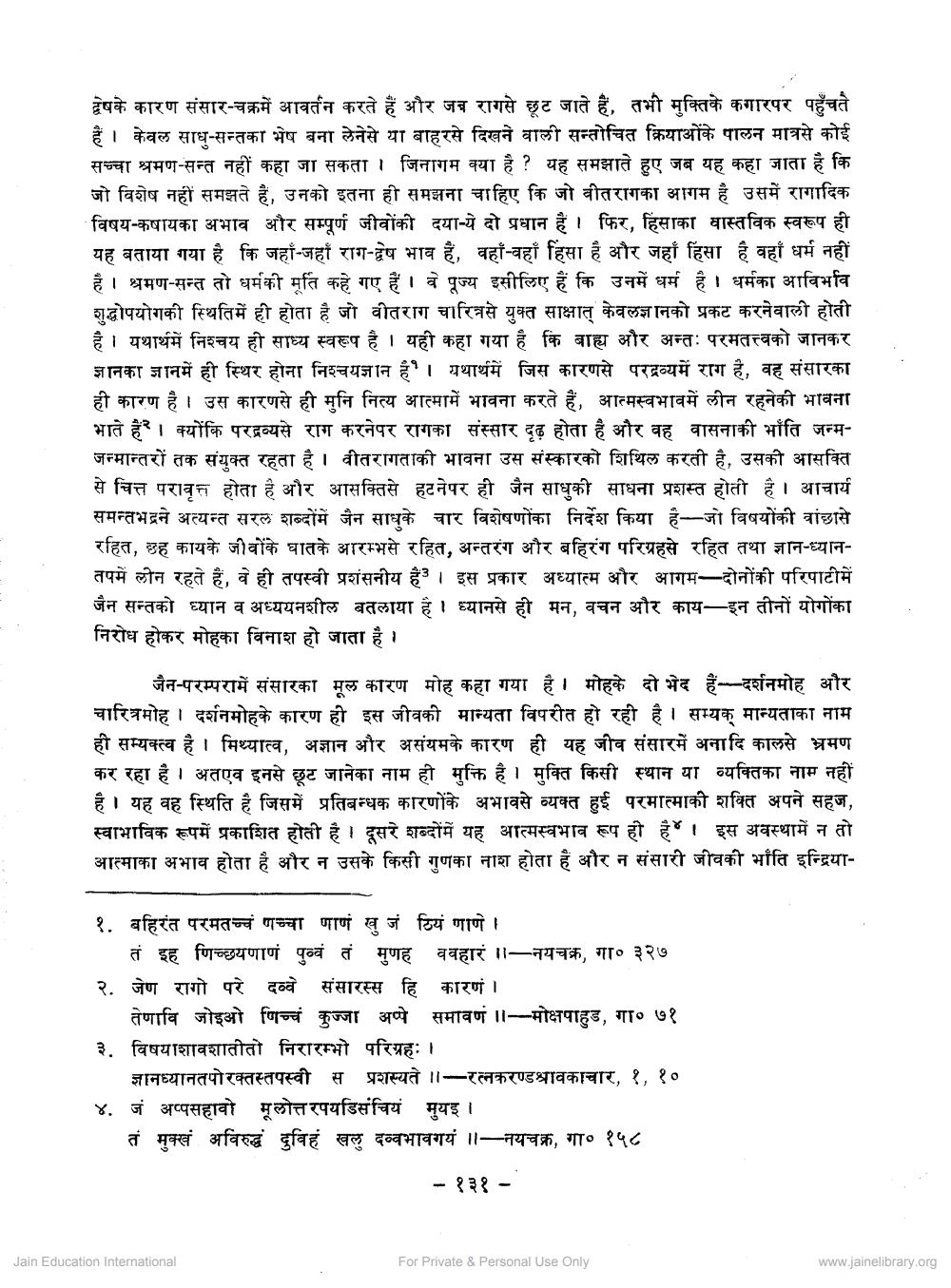________________
द्वेषके कारण संसार-चक्रमें आवर्तन करते हैं और जब रागसे छूट जाते हैं, तभी मुक्तिके कगारपर पहुँचते हैं। केवल साधु-सन्तका भेष बना लेनेसे या बाहरसे दिखने वाली सन्तोचित क्रियाओंके पालन मात्रसे कोई सच्चा श्रमण-सन्त नहीं कहा जा सकता। जिनागम क्या है ? यह समझाते हुए जब यह कहा जाता है कि जो विशेष नहीं समझते हैं, उनको इतना ही समझना चाहिए कि जो वीतरागका आगम है उसमें रागादिक विषय-कषायका अभाव और सम्पूर्ण जीवोंकी दया-ये दो प्रधान है। फिर, हिंसाका वास्तविक स्वरूप ही यह बताया गया है कि जहाँ-जहाँ राग-द्वेष भाव हैं, वहाँ-वहाँ हिसा है और जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। श्रमण-सन्त तो धर्मकी मूर्ति कहे गए हैं। वे पूज्य इसीलिए हैं कि उनमें धर्म है। धर्मका आविर्भाव
की स्थितिमें ही होता है जो वीतराग चारित्रसे यक्त साक्षात केवलज्ञानको प्रकट करनेवाली होती है। यथार्थमें निश्चय ही साध्य स्वरूप है । यही कहा गया है कि बाह्य और अन्तः परमतत्त्वको जानकर ज्ञानका ज्ञानमें ही स्थिर होना निश्चयज्ञान है। यथार्थमें जिस कारणसे परद्रव्यमें राग है, वह संसारका ही कारण है। उस कारणसे ही मुनि नित्य आत्मामें भावना करते हैं, आत्मस्वभावमें लीन रहनेकी भावना भाते हैं। क्योंकि परद्रव्यसे राग करनेपर रागका संस्सार दृढ़ होता है और वह वासनाकी भाँति जन्मजन्मान्तरों तक संयुक्त रहता है। वीतरागताकी भावना उस संस्कारको शिथिल करती है, उसकी आसक्ति से चित्त परावृत्त होता है और आसक्तिसे हटनेपर ही जैन साधुकी साधना प्रशस्त होती है। आचार्य समन्तभद्रने अत्यन्त सरल शब्दोंमें जैन साधके चार विशेषणोंका निर्देश किया है-जो विषयोंकी वांछासे रहित, छह कायके जीवोंके घातके आरम्भसे रहित, अन्तरंग और बहिरंग परिग्रहसे रहित तथा ज्ञान-ध्यानतपमें लीन रहते हैं, वे ही तपस्वी प्रशंसनीय है । इस प्रकार अध्यात्म और आगम-दोनोंकी परिपाटीमें जैन सन्तको ध्यान व अध्ययनशील बतलाया है। ध्यानसे ही मन, वचन और काय-इन तीनों योगोंका निरोध होकर मोहका विनाश हो जाता है ।
___ जैन-परम्परामें संसारका मूल कारण मोह कहा गया है। मोहके दो भेद हैं-दर्शनमोह और चारित्रमोह । दर्शनमोहके कारण ही इस जीवकी मान्यता विपरीत हो रही है । सम्यक् मान्यताका नाम ही सम्यक्त्व है। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयमके कारण ही यह जीव संसारमें अनादि कालसे भ्रमण कर रहा है । अतएव इनसे छूट जानेका नाम ही मुक्ति है। मुक्ति किसी स्थान या व्यक्तिका नाम नहीं है। यह वह स्थिति है जिसमें प्रतिबन्धक कारणोंके अभावसे व्यक्त हुई परमात्माकी शक्ति अपने सहज, स्वाभाविक रूपमें प्रकाशित होती है। दूसरे शब्दोंमें यह आत्मस्वभाव रूप ही है। इस अवस्थामें न तो आत्माका अभाव होता है और न उसके किसी गुणका नाश होता है और न संसारी जीवकी भांति इन्द्रिया
१. बहिरंत परमतच्चं णच्चा णाणं खु जं ठियं णाणे । __ तं इह णिच्छयणाणं पुवं तं मुणह ववहारं ।।-नयचक्र, गा० ३२७ २. जेण रागो परे दव्वे संसारस्स हि कारणं ।
तेणावि जोइओ णिच्चं कुज्जा अप्पे समावणं ।।-मोक्षपाहुड, गा० ७१ ३. विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रहः । ___ ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥-रत्नकरण्डश्रावकाचार, १, १० ४. जं अप्पसहावो मूलोत्तरपयडिसंचियं मुयइ ।
तं मुक्खं अविरुद्धं दुविहं खलु दन्वभावगयं ॥–नयचक्र, गा० १५८
- १३१ -
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org