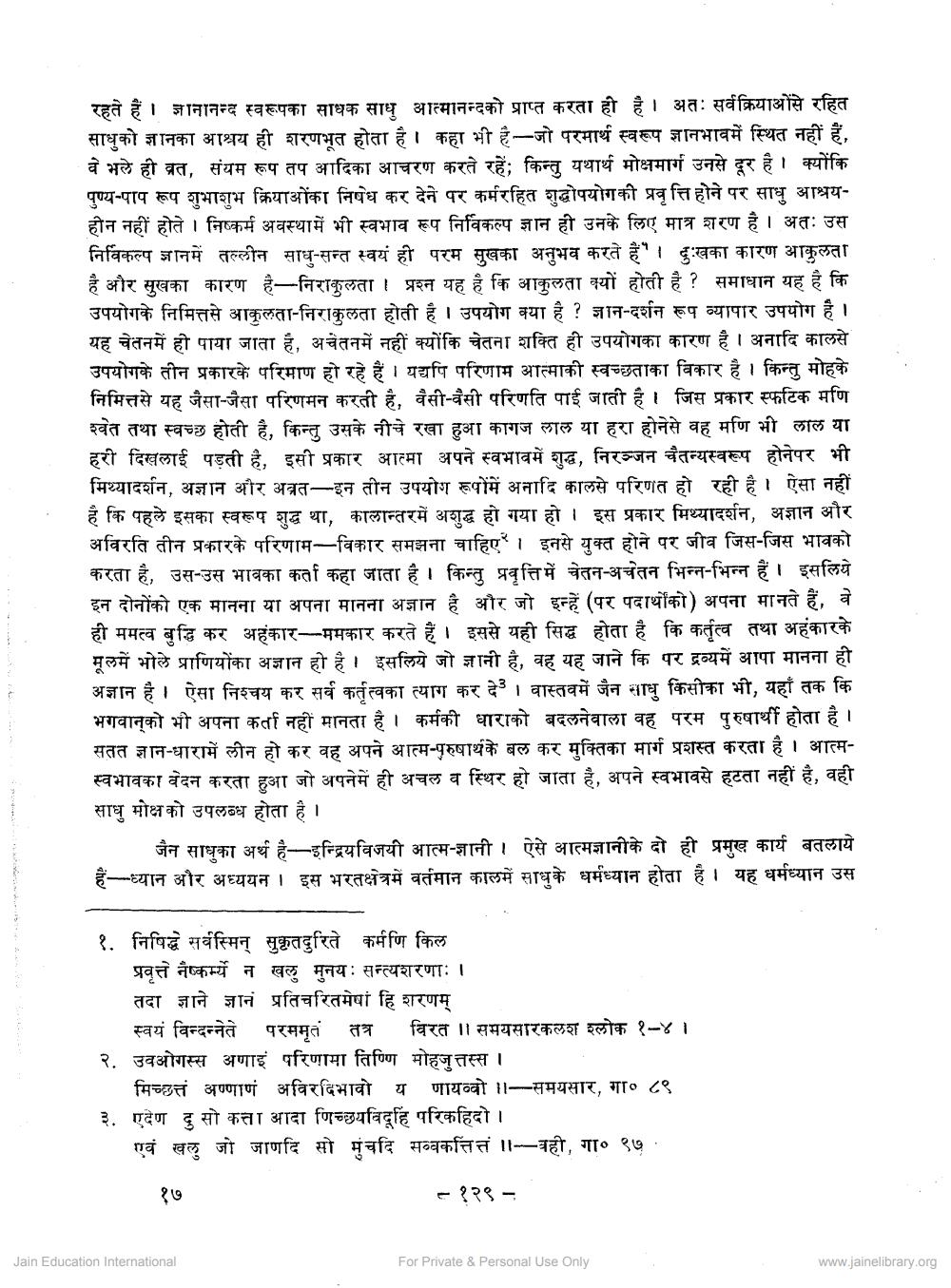________________
रहते हैं। ज्ञानानन्य स्वरूपका साधक साधु आत्मानन्दको प्राप्त करता ही है। अतः सर्वक्रियाओंसे रहित साधुको ज्ञानका आथय ही शरणभूत होता है। कहा भी है जो परमार्थ स्वरूप ज्ञानभाव में स्थित नहीं हैं, वे भले ही व्रत, संयम रूप तप आदिका आचरण करते रहें; किन्तु यथार्थ मोक्षमार्ग उनसे दूर है । क्योंकि पुण्य-पाप रूप शुभाशुभ क्रियाओंका निषेध कर देने पर कर्मरहित शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होने पर साधु आश्रयहोन नहीं होते । निष्कर्म अवस्था में भी स्वभाव रूप निर्विकल्प ज्ञान ही उनके लिए मात्र शरण है। अतः उस निर्विकल्प ज्ञानमें तल्लीन साधु सन्त स्वयं ही परम सुखका अनुभव करते हैं'। दुःखका कारण आकुलता है और सुखका कारण है— निराकुलता । प्रश्न यह है कि आकुलता क्यों होती है ? समाधान यह है कि उपयोगके निमित्तसे आकुलता निराकुलता होती है। उपयोग क्या है ? ज्ञान दर्शन रूप व्यापार उपयोग है। यह चेतनमें ही पाया जाता है, अचेतनमें नहीं क्योंकि चेतना शक्ति ही उपयोगका कारण है । अनादि काल से उपयोगके तीन प्रकारके परिमाण हो रहे हैं। यद्यपि परिणाम आत्माकी स्वच्छताका विकार है। किन्तु मोहके निमित्तसे यह जैसा जैसा परिणमन करती है, वैसी वैसी परिणति पाई जाती है। जिस प्रकार स्फटिक मणि श्वेत तथा स्वच्छ होती है, किन्तु उसके नीचे रखा हुआ कागज लाल या हरा होनेसे वह मणि भी लाल या हरी दिखलाई पड़ती है, इसी प्रकार आत्मा अपने स्वभाव में शुद्ध, निरञ्जन चैतन्यस्वरूप होनेपर भी मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अवत इन तीन उपयोग रूपोंमें अनादि कालसे परिणत हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले इसका स्वरूप शुद्ध था, कालान्तर में अशुद्ध हो गया हो। इस प्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति तीन प्रकारके परिणाम — विकार समझना चाहिए। इनसे युक्त होने पर जीव जिस-जिस भावको करता है, उस उस भावका कर्ता कहा जाता है। किन्तु प्रवृत्ति में चेतन-अचेतन भिन्न-भिन्न । हैं । इसलिये इन दोनोंको एक मानना या अपना मानना अज्ञान है और जो इन्हें ( पर पदार्थों को ) अपना मानते हैं, वे ही ममत्व वृद्धि कर अहंकार - ममकार करते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्तत्व तथा अहंकारके मूलमें भोले प्राणियोंका अज्ञान हो है । इसलिये जो ज्ञानी है, वह यह जाने कि पर द्रव्यमें आपा मानना ही अज्ञान है । ऐसा निश्चय कर सर्व कर्तृत्वका त्याग कर दे । वास्तवमें जैन साधु किसीका भी, यहाँ तक कि भगवान्को भी अपना कर्ता नहीं मानता है। कर्मकी धाराको बदलनेवाला वह परम पुरुषार्थी होता है। सतत ज्ञान-धारामें लीन हो कर वह अपने आत्म-पुरुषार्थ के बल कर मुक्तिका मार्ग प्रशस्त करता स्वभावका वेदन करता हुआ जो अपनेमें ही अचल व स्थिर हो जाता है, अपने स्वभावसे हटता नहीं है, वही साधु मोक्ष को उपलब्ध होता है ।
जैन साधुका अर्थ है - इन्द्रियविजयी आत्म-ज्ञानी । ऐसे आत्मज्ञानीके दो ही प्रमुख कार्य बतलाये है-ध्यान और अध्ययन इस भरतक्षेत्र में वर्तमान कालमें साधुके धर्मध्यान होता है। यह धर्मध्यान उस
१. निषिद्धं सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल
प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यशरणाः । तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणम् स्वयं विन्दग्ने
परममृतं परममृतं तत्र विरत | समयसारकलश श्लोक १-४ ।
२. उवओगस्स अणाई परिणामा तिष्णि मोहजुत्तस्स ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णायव्वो । समयसार, गा० ८९ ३. देश दुसो कता आदा णिच्छयविहि परिकहिदो ।
एवं खलु जो जागदि सो मुंचदि सव्वकलितं । वही गा० ९७
--
१७
- १२९ -
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org