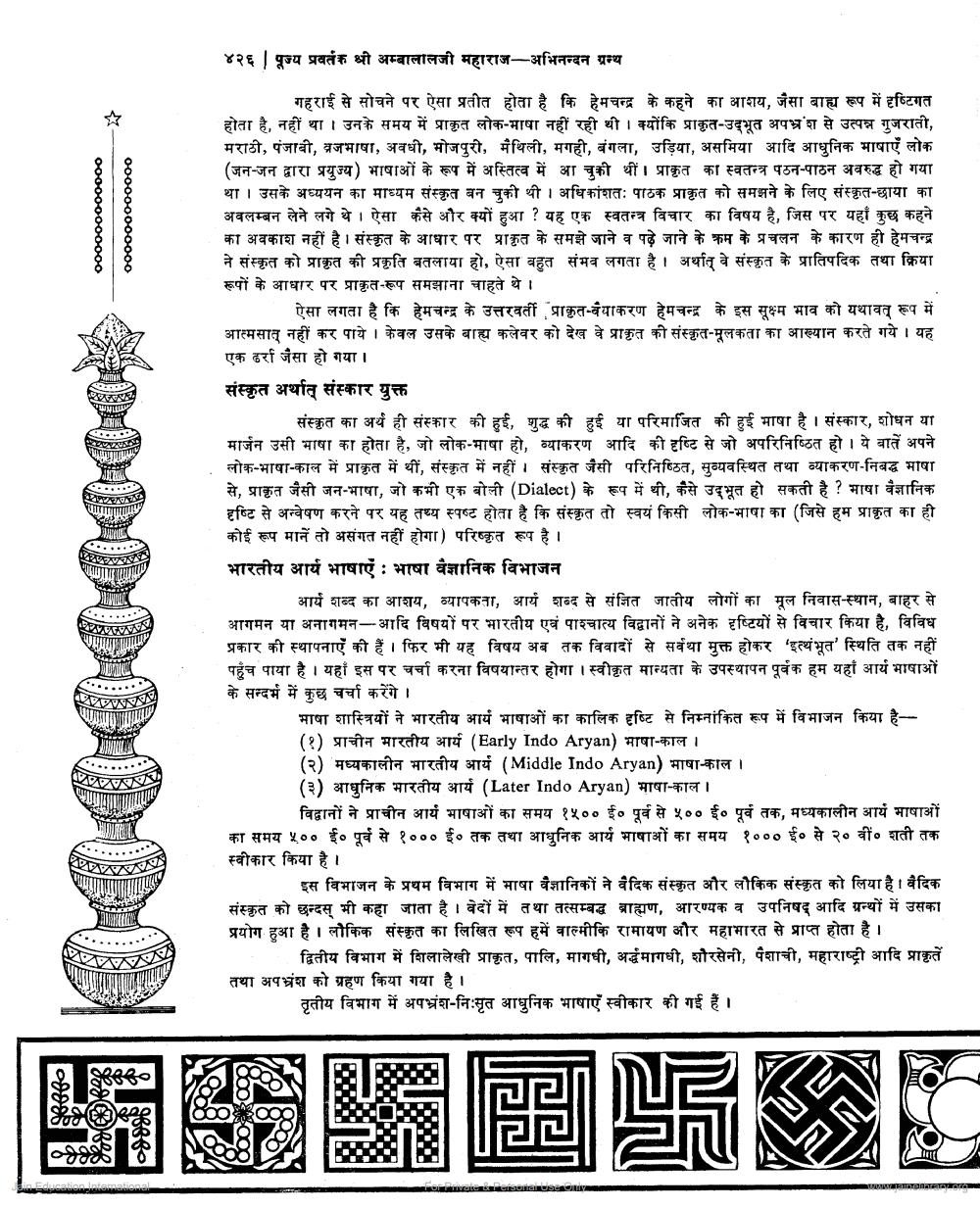________________
४२६ | पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालालजी महाराज-अभिनन्दन ग्रन्थ
000000000000
००००००००००००
Omp>
पूण
C
...
AUTIYA
गहराई से सोचने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हेमचन्द्र के कहने का आशय, जैसा बाह्य रूप में दृष्टिगत होता है, नहीं था। उनके समय में प्राकृत लोक-माषा नहीं रही थी। क्योंकि प्राकृत-उद्भूत अपभ्रंश से उत्पन्न गुजराती, मराठी, पंजाबी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया आदि आधुनिक भाषाएँ लोक (जन-जन द्वारा प्रयुज्य) भाषाओं के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थीं। प्राकृत का स्वतन्त्र पठन-पाठन अवरुद्ध हो गया था। उसके अध्ययन का माध्यम संस्कृत बन चुकी थी । अधिकांशतः पाठक प्राकृत को समझने के लिए संस्कृत-छाया का अवलम्बन लेने लगे थे। ऐसा कैसे और क्यों हुआ? यह एक स्वतन्त्र विचार का विषय है, जिस पर यहाँ कुछ कहने का अवकाश नहीं है । संस्कृत के आधार पर प्राकृत के समझे जाने व पड़े जाने के क्रम के प्रचलन के कारण ही हेमचन्द्र ने संस्कृत को प्राकृत की प्रकृति बतलाया हो, ऐसा बहुत संभव लगता है। अर्थात् वे संस्कृत के प्रातिपदिक तथा क्रिया रूपों के आधार पर प्राकृत-रूप समझाना चाहते थे।
ऐसा लगता है कि हेमचन्द्र के उत्तरवर्ती प्राकृत-वैयाकरण हेमचन्द्र के इस सूक्ष्म भाव को यथावत् रूप में आत्मसात् नहीं कर पाये । केवल उसके बाह्य कलेवर को देख वे प्राकृत की संस्कृत-मूलकता का आख्यान करते गये । यह एक ढर्रा जैसा हो गया। संस्कृत अर्थात् संस्कार युक्त
संस्कृत का अर्थ ही संस्कार को हुई, शुद्ध की हुई या परिमाजित की हुई भाषा है । संस्कार, शोधन या मार्जन उसी भाषा का होता है, जो लोक-भाषा हो, व्याकरण आदि की दृष्टि से जो अपरिनिष्ठित हो। ये बातें अपने लोक-भाषा-काल में प्राकृत में थीं, संस्कृत में नहीं। संस्कृत जैसी परिनिष्ठित, सुव्यवस्थित तथा व्याकरण-निबद्ध भाषा से, प्राकृत जैसी जन-भाषा, जो कभी एक बोली (Dialect) के रूप में थी, कैसे उद्भूत हो सकती है ? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अन्वेषण करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि संस्कृत तो स्वयं किसी लोक-भाषा का (जिसे हम प्राकृत का ही कोई रूप मानें तो असंगत नहीं होगा) परिष्कृत रूप है । भारतीय आर्य भाषाएँ : भाषा वैज्ञानिक विभाजन
आर्य शब्द का आशय, व्यापकता, आर्य शब्द से संजित जातीय लोगों का मूल निवास-स्थान, बाहर से आगमन या अनागमन-आदि विषयों पर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक दृष्टियों से विचार किया है, विविध प्रकार की स्थापनाएं की हैं। फिर भी यह विषय अब तक विवादों से सर्वथा मुक्त होकर 'इत्थंभूत' स्थिति तक नहीं पहुँच पाया है । यहाँ इस पर चर्चा करना विषयान्तर होगा । स्वीकृत मान्यता के उपस्थापन पूर्वक हम यहाँ आर्य भाषाओं के सन्दर्भ में कुछ चर्चा करेंगे।
भाषा शास्त्रियों ने भारतीय आर्य भाषाओं का कालिक दृष्टि से निम्नांकित रूप में विभाजन किया है(१) प्राचीन भारतीय आर्य (Early Indo Aryan) भाषा-काल । (२) मध्यकालीन भारतीय आर्य (Middle Indo Aryan) भाषा-काल । (३) आधुनिक भारतीय आर्य (Later Indo Aryan) भाषा-काल ।
विद्वानों ने प्राचीन आर्य भाषाओं का समय १५०० ई० पूर्व से ५०० ई० पूर्व तक, मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय ५०० ई० पूर्व से १००० ई० तक तथा आधुनिक आर्य भाषाओं का समय १००० ई० से २० वीं शती तक स्वीकार किया है।
इस विभाजन के प्रथम विभाग में भाषा वैज्ञानिकों ने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को लिया है । वैदिक संस्कृत को छन्दस् भी कहा जाता है । वेदों में तथा तत्सम्बद्ध ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद् आदि ग्रन्थों में उसका प्रयोग हुआ है । लौकिक संस्कृत का लिखित रूप हमें वाल्मीकि रामायण और महाभारत से प्राप्त होता है।
द्वितीय विभाग में शिलालेखी प्राकृत, पालि, मागधी, अर्द्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री आदि प्राकृतें तथा अपभ्रंश को ग्रहण किया गया है।
। तृतीय विभाग में अपभ्रंश-निःसृत आधुनिक भाषाएं स्वीकार की गई हैं।
VIE
2000
dodaUK
00000